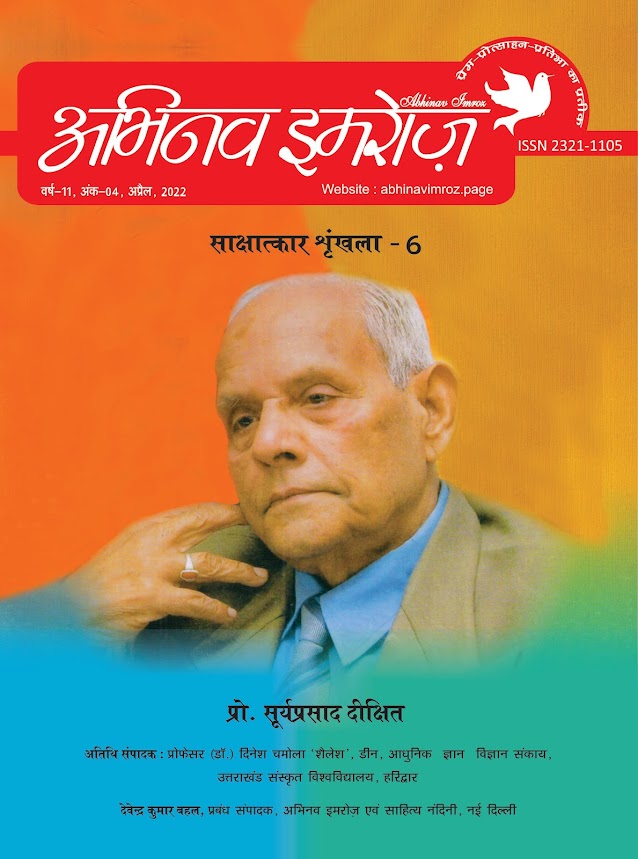अभिनव इमरोज़, अप्रैल 2022
इदं न मम
इन्द्र क्रतुं न आभर, पिता पुत्रेभ्यो यथा
शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि
जीवा ज्योतिरशीमहि।।
-ऋग्वेद
हे परमात्मन
पिता पुत्र को जैसे देवें
ज्ञान युक्त कर्मों का प्रभुवर वर देना
हे बहुस्तुत ईश्वर
इस जीवन पथ में शिक्षित करके
जीवित जागृत पथ आलोकित कर देना
काव्यानुवाद: श्री सत्य प्रकाश उप्पल
मोगा (पंजाब), मो. 98764-28718
___________________________________________________________________________________
पूज्यवर राजनारायण बिसारिया जी को श्रद्धांजलि
पूज्यवर राजनारायण बिसारियाजी का पवित्र स्मरण।
प्रियता और पूज्यता व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति सबके दो पक्ष होते हैं, जिनसे ये स्मृतियों में चिरकाल तक जीवित,सुखद और भास्कर बनें रहते हैं। बिसारियाजी मुझे प्रियतर भी थे, और पूज्यवर भी मान्य थे। उनसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय कभी नहीं हुआ, किंतु बीबीसी, लंदन के ‘‘पत्र मिला ‘‘कार्यक्रम के प्रसारणों में उनकी शैली की जो छाप मुझ पर पड़ी वह शिलालेख के स्वर्णाक्षरों के समान अब भी अंकित है। मैं बहुधा बीबीसी के प्रसारणों के संबंध में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखता था जिसे वे गंभीरता से लेकर पसंद करते और प्रसारणों में जगह भी देते थे। वैसे बीबीसी की ‘‘हिन्दी सेवा ‘‘प्रसारण में एक से एक सुयोग्य उद्घोषक थे, किन्तु बिसारियाजी मुझे सबसे अलग लगते थे। शैली व्यक्तित्व है, यह सटीक है ,और न्यूनाधिक हर व्यक्ति पर लागू होती है,किन्तु फिर भी उनमें अन्तर तो होता ही है। बिसारियाजी मेरी समझ में अपने शब्दप्रयोग, वाक्य विन्यास, के साथ अपनी अभिव्यक्ति की नवीनता के कारण अपनी पूरी टीम में विलक्षण थे। मैं समझता था कि वे अनुकरणीय विश्वविख्यात विरल उद्घोषक हैं। वस्तुतः वाक्य प्रयोग में शब्दों के आरोह अवरोह और उचित विराम का उनका अभ्यास था। वे पूरे नियंत्रण के साथ शब्दों को वाक्य की मालिका में कुशल मालाकार के समान पीरो/गूंथकर अपने श्रोताओं को प्रस्तुत करते थे।
काल प्रवाह में मेरा बीबीसी से संपर्क कम हो गया। बिसारियाजी से कभी व्यक्तिगत पत्राचार भी पहले नहीं हुआ था, आवासीय पता भी नहीं था। किंतु मैं उनको भूला नहीं था, दैवयोग कहा जाय मैं भी उनकी स्मृतियों में कहीं जुगनू की तरह जगमगा रहा था। वर्ष छह के दिसंबर में दिल्ली रहकर मैं यहां अपने घर आया तो एक पत्र देखा, जिसपर प्रेषक की जगह पर बिसारियाजी का नाम पता था। इसे पढ़कर मैं विस्मयविमुग्ध होगया। पत्र के भाव, भाषा और शैली में आत्मीयता थी। वह पत्र आज भी मैंने संजोकर रखा है, जिसे पढ़कर उनके बाहुल्य की सुखद अनुभूतियों में डूब जाता हूं। पावन सुखद अविस्मरणीय स्मृतियों में आज भी ...।
मेरे पुत्र कौस्तुभ जी बताते हैं कि प्रियवर सुहृद्वर बिसारिया जी ने उनका प्रत्यक्ष परिचय आदरणीय देवेन्द्र कुमार बहल, संपादक अभिनव इमरोज और नंदिनी से कराया। बिसारियाजी ने पत्रकारिता के अपने गहन गंभीर ज्ञान के पारस स्पर्श से कौस्तुभजी की पत्रकारीय अभिरुचि शिक्षा प्रशिक्षण को एक कुशल वास्तुशिल्पी की तरह तराशकर नयी नयी ऊंचाइयों का दिग्दर्शन करते रहने का अनथक प्रयास किया, जो एक अज्ञात कुलशील के युवा के लिए प्रवास में अकल्पनीय था। बिसारियाजी ने आपने व्यस्त बहुमूल्य समय का अधिकांश कौस्तुभजी के लिए दिया। उनकी प्रकाशनापेक्षी कृति की पांडुलिपि को अक्षर-अक्षर जांच परखकर प्रकाशन योग्य बनाया। पुस्तक का नाम अपनी पसंद से ‘‘टीवी समाचार की दुनिया‘‘ की भूमिका ‘‘प्रसंग ‘‘लिखी। इसे अपनी मनपसंद भूमिका की तरह उन्होंने लिया और एक विश्वसनीय प्रकाशक ‘‘किताब घर ‘‘से उसके सम्मानसहित प्रकाशन कराने की भी व्यवस्था की। बिसारियाजी स्वभावतः साधक, अनुष्ठान परायण थे। बीबीसी हिंदी सेवा/सर्विस को वे ‘‘हिन्दी अनुष्ठान‘‘ ही कहते थे। जब वे स्टुडियो में आते तो बड़े गौरव से, बीबीसी हिन्दी अनुष्ठान ही कहकर कार्यक्रम को प्रारंभ करते थे। उनके हर शब्द, वाक्य में एक गरिमा प्रतिध्वनित होती थी। वस्तुतः बिसारियाजी बीबीसी, हिन्दी अनुष्ठान की गरिमा ही थे जो स्थान उनकी सेवा निवृति के बाद कोई नहीं ले सका। वे स्वभाव कर्तव्यकर्म से भी स्वयं एक संस्था थे। वे समझते थे कि संस्था केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होती,उसमें नवनिर्माण का वैचारिक मार्दव और कर्मकौशल सौष्ठव प्रतिबिंबित होता है। अपने से छोटे, लघु को शक्ति, स्नेह, और सम्मान देकर नया बनाने का वह एक शिल्प गढ़ रहे थे।
मुझसे उनका कितना गहरा भावनात्मक संबंध था इसका पता एक घटना में मिलता है। बहुत दूर नहीं, पिछले ही वर्षांत दिसंबर में कौस्तुभजी यहां आते थे। इसी बीच एक संध्या उन्हें फोन आया। फोन बिसारियाजी का था। कौस्तुभजी उन्हें बताया कि वे अभी अपने घर/मोतिहारी में है। यह सुनकर उन्होंने तुरंत मेरे बारे में जानकारी ली। कौस्तुभजी ने यह कहते हुए ‘‘वे यहीं हैं, बात कीजिए।‘‘ फोन मुझे दे दिया। दोनों की आत्मीयता भरी बातें होती रहीं। वहीं उनसे मेरी पहली और अन्तिम बातचीत थी। कौन जाने बिसारियाजी मुझे ही खोजते हुए कौस्तुभजी के माध्यम से मेरे घर तक पहुंच गये थे। आत्मीय अंतरंग संबंधों की यह अनंत अकथकथा है।
मेरे आत्मसहचर बिसारियाजी सम्मानित व्यक्ति थे। बीबीसी का कार्यकाल सम्मान व्यतीतकर वे सेवानिवृत्त हुए थे। स्वदेश लौटने पर यहां भी वे भारत सरकार की ‘‘प्रसार भारती‘‘संस्था में रहकर उसे अपने सुदीर्घ अनुभवों से समृद्ध करते रहे। वे बीबीसी से यहां भारत तक जहां भी रहे मेरी मैत्री सुह्द्भाव की रही। पूज्यसुहृद्वर बिसारियाजी आज भी मेरे मनप्राणों को अपनी पवित्र भावनाओं से शक्ति स्फूर्ति देरहें हैं। सच है, वे सच है वे सज्जन सुकृत् पुरुष थे, जिनके लिए कहा गया है ‘‘उन्हें जरा मरण का भय नहीं होता, वे चिरंजीवी होते हैं, सुरतरु की सुरभि के समान उनके कर्तव्य कर्म का शाश्वत सौरभ दिग्दिगन्त को पवित्र करता रहता है।
सच है.. चटक न ताड़ते घटती हुं, सजन नेह गंभीर।
फीकौं पड़ै, न बरू फटै,
रंग्यो चोल रंग चीर। शत शत नमनपुष्प...
सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मोतिहारी (बिहार)
___________________________________________________________________________________
साहित्य समाज ने खोया एक मौन साधक
पूरे देश में बसंत की लहर चल रही थी। सरस्वती देवी के आगे नतमस्तक होते हुए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई-लिखाई में सफलता की प्रार्थना कर रहे थे। साहित्यकार बसंती रचनाओं से अपनी डायरियों के पन्ने रंग रहे थे। ऐसे में एक साहित्यकार अपने बिस्तर पर अनचाहा आराम फरमा रहा था। कभी-कभी बरसात हो जाने से वह काँप सा जाता और सूरज के बादलों से बाहर आने पर धूप का आनंद भी प्राप्त कर लेता था। भविष्य से अनजान चिकित्सक और पारिवारिक सदस्यों के कहने पर दवाई पूरी ईमानदारी से और बिना किसी शोर शराबे के लेते हुए कभी-कभी पुरानी यादों में खो जाता था। जब कोई उसे पुकारता तो वह सुनने वाली मशीन कान में लगी है या नहीं, यह देखने का प्रयास करता था। हरदर्शन सहगल नाम का यह इनसान 10 फरवरी 2022 की शाम अपने निवास स्थान ‘संवाद’ पर सामान्य लेकिन जरूरी भोजन और दवाइयों की खुराक लेकर चुपचाप इस दुनिया से कूच कर गया। ऐसा लगा कि शायद कुछ पलों पश्चात यह प्राणी अचानक उठकर कहेगा, ‘मुझे ठंड सी लग रही है, रजाई ओढ़ा दो।’ लेकिन उसके प्राण पखेरू उड़ चुके थे और वह अब कभी वापस न आने के लिए दूसरी दुनिया में चला गया था।
हरदर्शन सहगल का जन्म 26 फरवरी 1935 को कुंदियाँ, जिला मियांवली, पाकिस्तान में हुआ था। अपनी रेलवे की नौकरी से संतुष्ट बीकानेर स्थानांतरित होकर आने पर यह शहर उन्हें भा गया और उन्होंने इसी शहर में रहना ठीक समझा। बचपन में दस-ग्यारह वर्ष की उम्र में अपनी जन्मभूमि, अपनी मिट्टी, अपना घर, अपनी गलियाँ, अपना खेल का मैदान, अपना स्कूल, अपना शहर छोड़कर आना उन पर एक वज्रपात था। इन्हीं यादों के सहारे अपने जीवन के प्रत्येक कैनवास पर उन्होंने अपनी इच्छा से रंग भरे और उसे फ्रेम किया। एक शब्द, एक वाक्य, एक पैराग्राफ और फिर एक लघुकथा, कहानी, उपन्यास लिखते चले गए। पुरानी यादों को समेटते हुए आत्मकथा भी लिखी। निष्ठुर और अत्याचारी समाज की बुराइयों को व्यंग्य से ललकारा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने सामने अनगिनत पुस्तकों और पत्रिकाओं का ढ़ेर पाया तो बस पढ़ते चले गए और नया रचते चले गए। मित्रों के बीच और समाज के बीच चुपचाप छा जाने का उनके पास कोई हुनर नहीं था, उनके पास कोई दंद-फंद नहीं था फिर भी उनके मित्रों की सूची बहुत लंबी है जिसमें से बहुत से मित्र उनके सामने ही इस दुनिया से चले गए थे।
हरदर्शन सहगल के साहित्य की जो खूबी थी उसके बारे में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जहां किसी से मुलाकात हुई, जहां किसी से छोटी या लंबी बात हुई, जहां साहित्यिक चर्चा हुई, पुस्तक विमोचन हुआ, गोष्ठी हुई, पुस्तक मेले लगे, सभी जगहों पर उन्होंने अपनी रचनाओं का उद्गम पहचान कर, अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को शब्दों में उड़ेला और रचना को आकार दे डाला। उनके द्वारा रचे गए साहित्य की सूची भी लंबी है। जीवन में साथ निभाने वाले साहित्यकारों, परिवार और रिश्तेदारों, दूसरे दोस्तों, मोहल्ले के निवासियों ने उन्हें अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की।
हरदर्शन सहगल के आकस्मिक निधन पर राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला, भारत सरकार के माननीय संसद कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संदेश में परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में शरण देने की प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की। बीकानेर की अनेक संस्थाओं और गणमान्य नागरिक उनके निधन पर शोकमग्न हो गए।
हरदर्शन सहगल के निधन पर भगवान अटलानी, प्रताप सहगल, मुरलीधर वैष्णव, नंद भारद्वाज, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, लक्ष्मीशंकर वाजपेयी, सुकेश साहनी, सीमा अनिल सहगल, गंभीर सिंह पालनी, जय प्रकाश मानस, गिरीश पंकज, प्रेम जनमेजय, अरविंद तिवारी, सुरेश कांत, पंकज त्रिवेदी, सुभाष चंदर, कैलाश मनहर, फारुक अफरीदी, कमलेश भारतीय, पूरन सरमा, रत्न कुमार सांभरिया, कृष्ण कुमार रत्तू, मनहर चव्हाण, संतोष खन्ना, रणी राम गढ़वाली, नीलिमा टिक्कू, ममता वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार झांब, कुँवर प्रदीप सिंह, सैली बलजीत, राजीव श्रीवास्तव, रत्न श्रीवास्तव, सुधीर सक्सेना सुधि, इंदुशेखर तत्पुरुष, सुदर्शन पाण्डेय, सुधा तैलंग, श्याम सिंह राजपुरोहित, अमरीक सिंह खनूजा, अश्विनी कुमार, हीरालाल नागर, आशा पाण्डेय ओझा, चंद्रकांता और बीकानेर के मनोहर लाल चावला, मदन केवलिया, सरल विशारद, राम कुमार घोटड़, दीपचंद सांखला, बुलाकी शर्मा, राजेंद्र पी. जोशी, अजय जोशी, पंकज गोस्वामी, महेंद्र मोदी, राजेश कुमार व्यास, बृज रतन जोशी, राजाराम स्वर्णकार, राजेंद्र स्वर्णकार, आभा शंकरन, नीरज दइया, नवनीत पाण्डे, मंदाकिनी जोशी, प्रकाश खत्री, नासिर अली जैदी, अशफाक कादरी, प्रमिला गंगल, अब्दुल सत्तार कमल, सुधीर केवलिया, नदीम अहमद नदीम, शरद केवलिया, दयानंद शर्मा, संगीता शर्मा, मुक्ता तैलंग, धर्म प्रकाश शर्मा जैसे अनेक साहित्यकारों और पत्रकारों ने अपने-अपने शब्दों में श्रद्धांजलि प्रकट की।
मरुनगरी बीकानेर के दिग्गज और विचारशील साहित्यकारों की जमात में शामिल हरदर्शन सहगल आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन साहित्य क्षेत्र में उनके योगदान को लेखकीय समाज और उनका विशाल पाठक वर्ग अपने हृदय और मस्तिष्क में हमेशा याद रखेगा।
स्वर्गीय हरदर्शन सहगल को विनम्र श्रद्धांजलि और शत-शत नमन।
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
अतिथि संपादकीय
प्रो. दिनेश चमोला ‘शैलेश’
समय अथवा प्रारब्ध, हर उपवननुमा उर्वर मस्तिष्क में सुंदरतम व मूल्यवान फल, पुष्प व अप्राप्य पादपों के दुर्लभ बीजों को जब-तब छितराता रहता है। कोई उन भाव-बीजों के महत्त्व व उपादेयता से अनभिज्ञ हो, उसे नाहक ही नष्ट कर निरुद्देश्य व मृतप्राय होने को विवश कर देता है, जबकि कोई उसकी दुर्लभता व गोपनीयता के रहस्यात्मक चमत्कार को जानते हुए इतनी तल्लीनता से उसके पल्लवन, पुष्पन, संवर्धन व संरक्षण में जुट जाता है कि उसका एक-एक क्षण युग व समाज के लिए उपयोगी व मार्गदर्शी सिद्ध हो जाता है।
उस, प्राप्त भाव-बीज की सोद्देश्यता सुनिश्चित करने के उपक्रम में, वह स्वप्नद्रष्टा माली, प्राकृतिक संगतता के अनुकूल, न केवल उर्वर धरा पर उसके बीजारोपण की आधारभूमि तलाशता है, वरन समय≤ पर सश्रम उसे खर-पतवार व सामयिक झंझावातों से संरक्षित भी करता है। एक दिन, वही भाव-बीज, वृहद ज्ञानवृक्ष के रूप में विकसित होकर न केवल घनी छाया से जीव-जंतुओं व मानव समुदाय को सांसारिक तापों से त्राण देता है, बल्कि पुष्प-फलों से लकदक हो जड़-चेतन को अद्भुत जीवनी-शक्ति, प्रेरणा व ऊर्जा उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है।
फिर, उसी के सहचर्य से विकसित लहलहाते अभयारण्य की सुखद व सुरभित हरीतिमा का अप्रतिम सुख-सहचर्य, समग्र जड़-चेतन को अपनी अद्भुत क्षमता से दीर्घकाल तक अभिभूत करता रहता है।
अंततः वह संपूर्ण ज्ञान व श्रम-वैभव, सबके ज्ञान, आनंद, उत्कर्ष व जीवन-सुख का सर्वमान्य पर्याय भी हो जाता है। जब एक उन्नत बीज से विकसित स्वस्थ-पौध का स्वतंत्र अस्तित्व हर आगंतुक के जीवन को उल्लसित व प्रकाशित कर देने की शक्ति रखता है तो सत्याचरण व शब्द-साधना से अपने पास-परिवेश को संस्कारित करने वाले विराट व्यक्तित्व से जगती के लाभान्वित होने की तदनुसार कल्पना की जा सकती है।
सद-चिंतन का कौन सा बीज, आपके जीवन व चिंतन का पर्याय हो जाय, कौन आपके गंतव्य व मंतव्य में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए विवश कर दे, कहा नहीं जा सकता। शब्द और अर्थ के वास्तविक चमत्कार को, जीवन में आए किसी विस्मयकारी परिवर्तन के उपरांत ही महसूसा जा सकता है।
कुछ तपस्वी शब्द, कालांतर में मानव देह धारण कर लोक के कल्याण हेतु ही अवतरित होते हैं। शब्द की देह जब आत्मरूप में परिवर्तित हो चिंतन की आधारशिला बनती है तो वह अक्षरब्रह्म की इस ऊध्र्वमुखी यात्रा की प्रतिष्ठा का पर्याय हो जाती है। जीवनानुभूति की वह अंतरंगता अवश्य किसी अभीष्ट की ओर अग्रसर होकर परोक्षतः अपने परिवेश व लोक को प्रभावित करती है।
जहां जीवन ही परमार्थ के हित-चिंतन की अवधारणा हेतु प्रतिबद्ध हो, वहां जीवन की सकारात्मकता व सृजन के आनंद-मूल्यों का शत-प्रतिशत प्रतिबिम्ब स्वतः ही दिग्दर्शी होता है।
प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित उन विरल व्यक्तित्वों में से हैं जिनमें अबाध साधना के उत्स, विगत कई दशकों के उपरांत भी सृजनात्मक वैविध्य के रूप में पूरी निष्ठा के साथ सोत्साह दिखाई देता है।
आज भी उनका अथक श्रम, स्वाध्याय व चिंतनशील सृजनधर्मी व्यक्तित्व, बौद्धिक व भौतिक रूप में चिंतन वीथियों को नई ऊंचाइयां प्रदान कर ज्ञान के वैश्विक परिदृश्य को गौरवान्वित करता आ रहा है। जहां आज प्रदर्शन व अवसरवादिता के पक्षधर, प्रायः साधनात्मक पथों से कन्नी काट,अपनी तंत्र-याचना, तथाकथित चाटुकारिता से धनार्जन व पदार्जन कर स्वार्थ-सिद्धि में संलग्न हो, दुर्लभ मानव-जीवनादर्श को बाधित करने से नहीं अघाते, वहीं श्रमसाध्य जीवन व्यतीत कर, इस दृढ़-संकल्पी, साहित्यसेवी की बाल-सुलभ ज्ञान जिज्ञासा व पिपासा की अटूट चिंतन-श्रृंखला बिना किसी अवरोध के, अपने अस्तित्व की सोद्देश्यता सिद्ध करती है।
दीक्षित जी जैसे साधकों का व्यक्तित्व, जीवन की अंतिम श्वास तक ज्ञान की इस अक्षुण्ण परंपरा व ऊध्र्वमुखी लौ के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है जिससे साहित्य व संस्कृति की अपूर्व भाव-संपदा का अनहद नाद, काल व लोक को झंकृत करने की सामथ्र्य जुटाए रहता है।
साहित्यकार के समग्र चिंतन को साक्षात्कार के परिसीमित खांचे में समेटने का मोह सदैव रहता है, किंतु लघु भाव-गागर में असीमित ज्ञान-राशि को समग्रतः समेटना दुष्कर है, फिर भी इस महत्त्वपूर्ण श्रृंखला को अपूर्व बनाए रखने की अवधारणा सतत गतिमान है। बहल जी का उत्साही मन भी, इस प्रकार के संग्रहणीय अंकों के लिए उल्लसित रहता है। निश्चित ही ‘अभिनव इमरोज‘ की यह साक्षात्कार विविधा, न केवल लेखकों, पाठकों के लिए, बल्कि चिंतकों व शोधार्थियों के लिए भी अत्यंत उपादेय होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस हेतु बहल जी व उनकी टीम को साधुवाद। हार्दिक शुभकामनाएओं सहित,
सस्नेह आपका, प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश चमोला ‘शैलेश,‘’ डीन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय एवं अध्यक्ष, भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान विभाग, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
*23, गढ़ विहार, फेज -1, मोहकमपुर, देहरादून -248005, मो. 09411173339
___________________________________________________________________________________
डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित का परिचय
डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित का जन्म 6 जुलाई, 1938 को उत्तर प्रदेश, रायबरेली जनपद के बन्नावां नामक ग्राम में हुआ। पिता श्री भगवती प्रसाद दीक्षित, संत प्रकृति के तथा माता श्रीमती शिव दुलारी देवी वैष्णवी धर्मनिष्ठ महिला थीं। आपने ‘छायावादी गद्य‘ पर पी-एच.डी तथा ‘व्यावहारिक सौंदर्यशास्त्र‘ पर डी.लिट्. की उपाधि प्राप्त की। आपकी प्रमुख पुस्तकों में ‘प्रसाद का गद्य‘, ‘निराला का गद्य‘, ‘पंत जी का गद्य‘, ‘महादेवी का गद्य‘, ‘लक्षित निराला‘, ‘प्रसाद की अंतश्चेतना‘, ‘निराला की आत्मकथा‘, ‘छायावाद का व्यावहारिक सौंदर्यशास्त्र‘, ‘छायावाद की सही परख-पहचान‘, ‘प्रसाद समग्र‘, ‘निराला समग्र‘, ‘पंत समग्र‘, ‘प्रयोजनपरक हिंदी‘, ‘राजभाषा के पचास वर्ष‘, ‘भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा प्रबंधन‘, ‘प्रयोजनी हिंदी‘, ‘मीडिया लेखन कला‘, ‘जनसंचारः प्रकृति एवं परंपरा‘, ‘संचार भाषा हिंदी‘, ‘वृहद हिंदी पत्र पत्रिका कोश‘, ‘अवधी साहित्य कोश‘, ‘हिंदी अनुवाद कोश‘, ‘हिंदी राम साहित्य कोश‘, ‘ब्रज संस्कृति विश्वकोश‘, ‘अवध संस्कृति विश्वकोश‘, ‘पद्मावत प्रभा‘, ‘राम की शक्ति पूजा‘, ‘कुकुरमुत्ता‘, ‘शिव सिंह सिंगर रचनावली‘, ‘चंदन रचनावली‘, ‘सूक्ति सुधा‘, ‘आचार्य चिंतामणि‘, ‘आचार्य बेनी भट्ट‘, ‘हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका‘, ‘साहित्य का इतिहास दर्शन‘, (आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल), ‘राज्याश्रय और साहित्य‘, ‘नया साहित्य नए रूप‘, ‘लखनऊ के कवि‘, ‘आधुनिक अत्याधुनिक हिंदी कवि,‘ ‘स्वातंत्र्र्य समर में साहित्यकारों की सहभागिता‘, ‘हिंदू हिंदी‘, ‘आशु कविता‘, विश्व पटल पर हिंदी‘, ‘सेनापति तुलसी‘, ‘मानस आस्था का अर्क है‘, ‘तुलसी मत‘, ‘तुलसी जन्मभूमि‘, ‘राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और साकेत‘, ‘मिश्र बंधु‘, ‘हिंदी सौरभ‘, ‘लाला भगवानदीन‘, ‘अवधी भाषा और साहित्य संपदा‘, ‘अवधी श्रम गीत‘, ‘अवधी राम काव्य‘, ‘चिंतन मनन‘, ‘मंथन पर्व आदि अनेक पुस्तकों का लेखन किया। कई पत्रिकाओं का संपादन। ‘साहित्य भूषण सम्मान‘, ‘दीनदयाल उपाध्याय सम्मान‘, ‘साहित्य वाचस्पति उपाधि‘ आदि अनेक सम्मान प्राप्त। देश के अनेक विभागों, कार्यालयों, मंत्रालयों में अनवरत व्याख्यान। प्रस्तुत है हिंदी सेवी, समालोचक, प्रो. से हुई विस्तृत बातचीत के संपादित अंश-)
आपके जन्म, शिक्षा-दीक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और नामकरण के संबंध में यदि यथेष्ट जानकारी हो जाए तो भेट वार्ता का प्रारूप निर्मित करने में सुविधा होगी।
मेरा जन्म उत्तरप्रदेश के जनपद रायबेरली में बछराँवा के निकट लालगंज रोड पर स्थित बन्नावाँ नामक गाँव में हुआ था। बछराँवा से 3 किमी दूर स्थित इस गाँव की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। इसमें लगभग डेढ़ सौ कान्यकुब्ज ब्राह्मण-परिवार हैं। अधिकतर किसान हैं। कुछ शिक्षक हैं और कुछ पौरोहित्य कर्म से जुड़े हैं। उनके अतिरिक्त चार पाँच बैस ठाकुरों के परिवार हैं। गाँव का भूगोल तथा प्रकृति-परिवेश बड़ा विचित्र है। इसके चारों ओर बड़े-बड़े तालाब हैं। बीच में टापू जैसा गाँव है। वर्षा में यह पहले तीन चार माह जलमग्न रहता था। सम्पर्क मार्ग प्रायः टूट जाता था। वहाँ का जलस्तर तो और भी विचित्र है। वर्षा ऋतु में कुछ कुओं का पानी ऊपर उफना आता था। लोग स्वयं बाल्टी डुबोकर पानी भर लिया करते थे। गर्मी में भी जलस्तर अधिक से अधिक दस-बारह फीट नीचे जाता था। पूरे गाँव में चिकनी दोमट मिट्टी है। धान की फसल यहाँ बहुत अच्छी होती है। अब तो हल बैल और मवेशी प्रायः नहीं दिखायी देते। लोग मशीनों से अधिया खेती कराते हैं। जनता आराम तलब और आत्म मुग्ध सी हो गयी है। ज्यादातर आम आदमी हैं। न अमीर, न बहुत गरीब। इस गाँव का इतिहास लगभग तीन सौ वर्ष पुराना है। ऐसी जनश्रुति है कि हमारे एक पूर्वज बन्ना जी ने कुछ वनों को काटकर यह गाँव बसाया था। पहले इसे बनगवाँ कहा गया होगा, फिर बन्ना से जुड़कर बन्नाँव (कालांतर में बन्नावाँ) हो गया। नवाबी शासनकाल में इस गाँव को बहुत दिनों तक कर से मुक्त रखा गया था। आसफुद्दौला के शासन काल में जब नवाबी कारिंदों ने इस गाँव का अधिग्रहण करना चाहा तो गाँव के तत्कालीन स्वामी बन्ना जी के उत्तराधिकारी चिरंजू जी ने बगावत कर दी। फलतः नवाबी सेना के छापे पड़ने लगे। चिरंजू जी भूमिगत रहने लगे। एक बार पकड़ में आ गए। लखनवी दरबार में उनकी पेशी हुई। उन्होंने गाँव की जागीर समर्पित करने से मना कर दिया। उन्हें कैद कर लिया गया। वहाँ रात में जब नाच-गाने की महफिल सजी हुई थी, चिरंजू अपनी कोठरी में बंद थे। वे बार-बार यही वाक्य दुहराते हुए सुने गए-‘‘अरे रे, चूक गया।‘ सिपाहियों ने पूछा-कौन चूक गया? तो वे बोले कि जो तबलची थाप दे रहा है, लगता है कि उसकी एक उँगली घायल है, जिससे उसकी ताल बार-बार चूक रही है। नवाब ने तबलची को बुलाकर उसकी जाँच की तो एक उँगली आधी कंटी हुई पायी गयी। उन्होंने चिरंजू जी से पूछा कि क्या तुम उससे बेहतर तबला बजा सकते हो? चिरंजू ने वह चुनौती स्वीकार कर ली और फिर ऐसी संगत की कि नवाब बाग-बाग हो उठे। उन्होंने कहा-‘‘आज मनचाहा इनाम माँग लो।‘‘ चिरंजू जी ने माँगा कि हमारा गाँव कर मुक्त कर दिया जाये। तब से जमींदारी उन्मूलन तक बन्नावाँ किसी रजवाड़े के अधीन नहीं रहा। मैंने जब होश संभाला था, उस समय दीक्षित परिवार की चार शाखाएँ गाँव में थीं। हम लोग रूपये में चार-चार आने (चैंथाई स्वामित्व) के जमींदार कहलाते थे। कालक्रम में दुबे परिवार और शुक्ल परिवार भी गाँव की जमींदारी के हिस्सेदार बने और फिर 1950 के बाद हम भूमिधर किसान बन गए।
ब्राह्मण बहुल होने के कारण इस गाँव में शिक्षा का बड़ा प्रचार प्रसार था। स्कूली शिक्षा यानि मिडिल स्कूल पास व्यक्ति तो बहुत थे, पर तब तक ग्रेजुएट कोई नहीं था। पारंपरिक पांडित्य वाले लोग ज्यादा थे। गाँव में एक लोअर प्राइमरी पाठशाली थी, जिसमें पड़ोस के ही एक गाँव से कभी पंडित जी, कभी मुंशी जी पढ़ाने आते थे। तब तक इस गाँव में कोई बड़ी चोरी, डकैती, हत्याकांड, दंगा जैसी दुर्घटनाए नहीं सुनायी देती थीं। गाँव में प्रायः कथा वार्ता, कीर्तन, मानस गायन, रामलीला, नाटक, सत्संग, कवि गोष्ठी, महोत्सव, भण्डारा आदि होते रहते थे। होली बहुत धूम धाम से मनायी जाती थी। यहाँ के कई फगुवार प्रसिद्ध थे। फाग गायन की वर्ष पर्यंत तैयारी करके बाहरी गाँवों के कई लोग प्रतियोगिता करने आते थे। इस गाँव के कई लोग कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, काशी, प्रयाग, दिल्ली, अयोध्या आदि से जुड़े हुए थे, इसलिए खान-पान, पहनावा, रहन-सहन आदि की दृष्टि से वे काफी आधुनिक थे। गाँव में ऐसे कई बुजुर्ग थे, जिन्हें प्राचीन कवियों के चार-पाँच सौ छन्द कंठस्थ थे। प्रति संध्या गाँव के शिवाले में उनका यह ‘‘कवित्तहाव‘‘ होता रहता था। गाँव में कई वैष्णव, शैव एवं देवी मंदिर थे। एक स्वामी जी रामानुज सम्प्रदाय से जुड़े थे। वे आस-पास के गावों के दीक्षा गुरु थे। दो प्रसिद्ध रामायणी कथावाचक और उपदेशक थे। एक वैद्य जी थे, जो किसी रजवाड़े में राजवैद्य रह चुके थे।
इसी गाँव में आज से चैरासी वर्ष पूर्व 1938 ई० में पंडित भगवती प्रसाद दीक्षित के ओरस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। रविवार, प्रत्यूष बेला, फाल्गुन अमावस्या का दिन। परिजनों ने सूर्य देव का कृपा प्रसाद. समझ कर मेरा नाम सूर्यप्रसाद रख दिया। तब नामकरण संस्कार सूर्य पूजा (छठी) के दिन किया जाता था, अपने कुल पुरोहित के माध्यम से। बारहवें दिन भोज आदि का आयोजन किया गया। यथा समय चूड़ाकरण, कर्णवेध, उपनयन और विद्यारम्भ जैसे संस्कार सम्पन्न हुए। तब विद्यालय में प्रवेश पाँच वर्ष बाद होता था, लेकिन गाँव की पाठशाला में बच्चों की संख्या कम हो गयी थी। स्कूल के टूट जाने का खतरा था, इसलिए हमारे पंडित जी ने मेरी कुछ उम्र बढ़ाकर मुझे स्कूल में भर्ती कर लिया था। उस विद्यालय में कुल चार वर्ग थे- अलिफ, बे, अव्वल और दोम। माध्यम थी उर्दू-हिन्दी समन्वित भाषा। 1946 में लोअर प्राइमरी पाठशाला पास करके मैं बछराँवा के अपर प्राइमरी पाठशाला में भर्ती हुआ। तब पक्की सड़क नहीं थी। वर्षा के दिनों में मैं घरेलू नौकर के साथ घोड़ी पर चढ़कर आता-जाता था। शेष दिनों में संगी सथियों के साथ खेलते कूदते पैदल। 15 अगस्त 1947 को विद्यालय के ऊपर से एक हेलीकाप्टर ने कुछ पर्चे गिराये थे। बच्चे उन्हें लेकर मास्टर जी के पास आए। उसमें मैथिलीशरण गुप्त जी की एक कविता छपी हुई थी-
‘‘आज हथकड़ी टूट गयी है,
नीच गुलामी छूट गयी है।
उठो देश कल्याण करो अब,
नव युग का निर्माण करो अब।‘‘
स्कूल में लइया के लड्डू बाँटे गए थे। उसे तिरंगे झण्डे एवं रंग बिरंगी झण्डियों से सजाया गया था। स्कूल के पास ही गुरुवर चन्द्रिका प्रसाद जी का आश्रम था। मुंशी जी उस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आश्रम में जोर जोर से भाषण हो रहे थे। वे भाषण तो हमारी समझ से परे थे, पर कुल मिलाकर वह माहौल हर्षोल्लास पूर्ण था।
प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करके मैं मिडिल स्कूल में गया। तीसरे वर्ष जब बोर्ड की परीक्षा होनी थी तो गुरुवर चन्द्रिका प्रसाद जी द्वारा स्थापित गाँधी विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्कूल में उस मिडिल स्कूल का विलयन हो गया,फलतः हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा छह वर्ष बाद 1954 में हुई।
मीडिल स्कूल तक मैं एक औसत विद्यार्थी था। कारण, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। माता जी और पिता जी को मैं बाद में बड़ी कठिनाई से केवल हस्ताक्षर करना सिखा पाया। माता जी पढ़ी तो नहीं, पर कढ़ी बहुत थीं। लोक गीत, कहावतें, लोक कथायें, और लौकिक रीति रिवाज उन्हें इतने सारे याद थे कि सुनकर लोग दंग रह जाते थे। उनके हर वाक्य के आगे पीछे कोई न कोई लोकोक्ति जरूर रहती थी। गीत-गायन, वादन के कार्यक्रम उनके बिना सूने या अधूरे माने जाते थे। कब कौन रीति-रिवाज कैसे निभाने चाहिए, इसकी वे विशेषज्ञ थीं और सच्चे अर्थों में सद्गृहिणी थीं। उनका मायका लखनऊ में था, इसलिए वे अपेक्षाकृत ज्यादा सलीकेदार थीं। हमारे नाना जी भी भूतपूर्व जमींदार, बल्कि बिगड़े रईस थे। इसलिए कुछ ज्यादा ही आभिजात्य माता जी को विरासत में मिला था। उन्होंने हम छह भाई-बहनों का विधिवत पालन-पोषण किया और भरसक गृह-मर्यादा की रक्षा की। अपने गाँव घर से उनका गहरा लगाव था। बहुत अनुरोध करने पर कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ जाती थीं। यों, चित्त वहीं रमता था। उन्होंने कई पौत्र-प्रपौत्र प्राप्त कर 92 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्यागा। निधन के चार माह पूर्व पूर्ण स्वस्थ अवस्था में उन्होंने एक प्रसंग चलाकर मुझसे यह प्रतिज्ञा करायी थी कि तुम कहीं भी रहो, पर मेरी चिता को आग तुम्ही दोगे और संस्कार तुम्ही करोगे। हम लोग उनका हाल चाल फोन से नित्य मालूम करते रहते थे। भरसक साधन-सुविधायें उपलब्ध कराते रहते थे और बीच-बीच में जाकर मिल आते थे। एक दिन जब मैं इलाहाबाद आयोग की बैठक में व्यस्त था, तभी फोन से माता जी की गंभीर बीमारी का हाल मिला। मुझे कुछ पूर्वाभास हुआ और मैं तत्काल गाँव पहुँचा तो वे मेरी ही राह देख रहीं थीं। बराबर पूछती जा रहीं थीं कि सूरज अभी नहीं आए। मैंने पहुँचकर कुछ देर बात की। कुछ उपचार किया। मैं बछराँवा से एक डॉक्टर को भी साथ ले गया था। उसने भरसक प्रयास किया, पर लगभग आध घण्टे के भीतर ही सबको शुभाशीष देते हुए उन्होंने सदा के लिए आँखें बंद कर लीं। दूसरे दिन उनकी शवयात्रा में गाँव-जवार का भारी जन समूह शामिल हुआ। गंगा तट पर दाह संस्कार हुआ और फिर गाँव में अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न हुआ।
मेरे पिता जी का निधन पहले हो चुका था। वे स्वभाव से नितांत साधु पुरुष थे। न किसी से विशेष राग, न द्वेष और सदैव आत्म मग्न। हमारा संयुक्त परिवार था। पिता जी से दो बड़े अग्रज थे। सबसे बड़े ताऊ जी पं0 शिवराम दीक्षित विधुर थे और निःसन्तान थे। उनका एक मात्र व्यसन और मिशन था, आम के बगीचे लगाने का। उनकी जमींदारी के हिस्से में कई बड़े-बड़े ऊसर थे, जिनमें उन्होंने हजारों पेड़ रोपे थे। वे मजदूरों के साथ इन्हीं पेड़ों की देख-रेख में व्यस्त रहते थे। हम बच्चों को बहुत स्नेह करते थे। मझले ताऊ जी भी विधुर और निःसन्तान थे। वे अपने समय के, अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध महाजन थे। जरूरत भर की भाषा और गणित समझते थे। एक मुनीम रखे हुए थे। घर के सामने उन्होंने एक शिवालय बनवाया था और उसी के बगल में आवास । भोजन सबके साथ। स्वभाव से बहुत मितव्ययी थे, लेकिन हम तीनों भतीजों की पढ़ाई के लिए बराबर तत्पर रहते थे। हम तीन भाइयों में सबसे बड़े भाई मिडिल स्कूल तक पढ़कर खेती किसानी में लग गए। दूसरे मझले भाई हाईस्कूल करने के बाद ननिहाल (लखनऊ) में आकर पढ़ने लग गए। अकेला मैं इण्टरमीडिएट तक उनकी सेवा में रहा। यज्ञोपवीत हो जाने के बाद से उन्होंने मुझे मन्दिर-पूजा का दायित्व दे दिया था और पढ़ाई में मेरी अभिरुचि तथा सफलता से प्रसन्न होकर उन्होंने सभी घरेलू कार्यों से मुझे मुक्त कर दिया था। उसके पहले हम गाँव के बच्चों को खेती-किसानी में कुछ न कुछ हाथ बटाना पड़ता था। जैसे- जब जुताई या सिंचाई हो रही हो तो मजदूरों को नाश्ता पहुँचाने का दायित्व हमारा था। हम एक बड़ी टोकरी में खाद्य पदार्थ लेकर जाते थे और जलपान कराकर लौट आते थे। प्रति सन्ध्या जब घरेलू पशु चरागाह से लौटते थे तो उन्हें यथा स्थान खूटे से बाँधना हम बच्चों का दायित्व था। कभी-कभी अपने दुधारू पशुओं को चराने का काम आ जाता था। इसी तरह पाँस (खाद) की ढुलाई हमें करनी पड़ती थी, किन्तु हाईस्कूल तक आते-आते ताऊजी ने मेरे लिए अलग कमरा बनवा दिया था और इन सारे कार्यों से मुक्त कर दिया था। जब वार्षिक परीक्षा का परिणाम लेकर हम आते थे तो प्रथम पोजीशन देखकर वे भाव विभोर हो उठते थे। कई दिनों तक वे आने-जाने वालों को रिजल्ट दिखाते रहते थे। इण्टर परीक्षा का
परिणाम जिस दिन निकला, मैंने अखबार उन्हें लाकर दिखाया। वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्होंने एक निशान लगा लिया था। लोगों को बुला बुलाकर वे बता रहे थे कि देखो हमारा सूरज सारे जिलों में फस्र्ट आया है। कभी-कभी तो रो पड़ते थे। आज भतीजों के प्रति ऐसे वात्सल्य की कल्पना नहीं की जा सकती। परिणाम घोषित होने के पूर्व उन्होंने यह तै कर लिया था कि अब सबकी पढ़ाई समाप्त। बड़ा लड़का खेती सम्भाले, दूसरा महाजनी देखे और तीसरा कपड़े का व्यापार। नौकरी करना तब मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। संयोग ऐसा रहा कि पहली बार बोर्ड की ‘मेरिट‘ से जुड़े हमारे कालेज के प्रधानाचार्य और संस्थापक गुरुवर मुंशी जी हमारे गाँव आए और उन्होंने बधाई देते हुए ताऊजी को समझाया कि इसे उच्च शिक्षा दी जाये। गुरु जी का वचन ब्रह्म वाक्य था। अस्तु, ताऊजी ने मुझे लखनऊ जाकर बी.ए. में प्रवेश लेने की अनुमति दे दी।
मेरे पिता जी सचमुच बीतराग थे। उस समय की लोक मर्यादा बड़ी विचित्र थी। लोग बड़े बुजुर्गों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करते थे। स्त्रियाँ पर्दे में रहती थीं। घर आँगन के बाहर नहीं निकलती थीं। पिता अपने बच्चों को बड़ों के सामने गोदी में लेकर नहीं खिलाते थे। हमारी माता जी के और हम बच्चों के परिधान ताऊजी लाते थे। शेष घर गृहस्थी की खरीददारी पिता जी करते थे। हम सबकी बीमारी, पढ़ाई, शादी विवाह आदि के मामले में पिता जी का बोलना, (राय देना) अमर्यादित माना जाता था। मैंने इन तीनों भाइयों को एक दूसरे से आँख मिलाकर या मुखातिब होकर कभी बातचीत करते नहीं देखा सुना। जो बात कहनी होती थी, उसमें माध्यम हम बच्चों को बनाया जाता था। पिता जी ने पूरे जीवन में यह नहीं पूछा कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो? कहाँ नौकरी कर रहे हो? वे बस अग्रजों की आदेश-पूर्ति करते रहते थे। उनकी एक निश्चित दिनचर्या थी। सुबह तैयार होकर खेत-खलिहान की ओर चले जाते थे। दोपहर लौटकर स्नान, पूजा-पाठ, भोजन और विश्राम। अपराह्न में फिर खलिहान। सायंकाल वे मंदिर में लगभग दो घण्टे भजन, कीर्तन तथा मानस-गायन करते थे। पूर्ण अक्षर ज्ञान न होते हुए भी वे रामचरित मानस बाँच लेते थे। होलिकोत्सव में वे फाग, लेज, चहली की गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। गाँव की रामलीला में वे दशरथ का अच्छा अभिनय करते थे। उन्हें पहलवानी का बड़ा शौक था। कुल मिलाकर वे बड़े शांत, सहिष्णु, सर्वथा संत स्वभाव के थे। कभी किसी पर क्रोध नहीं किया और भरसक किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। उनका निधन भी बहुत आकस्मिक ढंग से हुआ। जाड़े की रात। अलाव के पास बैठे हुए। सहसा हृदय गति रुक गयी। मैं उन दिनों जोधपुर में था। तीसरे दिन पहुँच पाया। अंतिम दर्शन नहीं कर सका। मेरा विवाह हो चुका था और बड़ी पुत्री का जन्म भी। उनके आकस्मिक निधन का गहरा आघात हम सबको लगा। 1976 से 1999 तक मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में रहा। अवकाश प्राप्त करके सपत्नीक लखनऊ में रह रहा हूँ। यही मेरी संक्षिप्त राम कहानी है।
साहित्य की दिशा में बढ़ने के स्वप्न आपके मन में कब कैसे जागे?
उच्च शिक्षा और साहित्य की दिशा में बढ़ने के सपने मुझे 1954 के आस-पास दिखने लगे थे। इसकी प्रथम प्रेरणा मुझे अपने गाँव के निवासी पं0 चन्द्रमणि जी से मिली। वे ‘सनेही मण्डल‘ के कवि थे। पारसीक परंपरा, राधेश्यामी शैली के लोकप्रिय नाटककार थे और भागवत. तथा मानस के प्रसिद्ध प्रवचन कर्ता थे। वे ‘भारती भवन‘ नाम का एक पुस्तकालय चलाते थे। उन्हीं के देखा देखी मैंने ‘सरस्वती संदन‘ नामक एक पुस्तकालय-वाचनालय शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे पुस्तकालय को कई पुस्तकें दीं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं कुछ-कुछ तुकबंदी करने लगा था। उन्होंने समय≤ पर मेरे गीतों एवं छंदों में संशोधन किया। सन् 1954 से मेरी कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। 12वीं कक्षा में मुझे हिन्दी पढ़ाने वाले एक ऐसे गुरू मिले, जिन्होंने जीवन की धारा ही बदल दी। वे धारावाहिक भाषण देते थे। उन्होंने मुझे वाद विवाद और अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। गुरुवर श्री नृपति सिंह भदौरिया जी ने मुझे आँसू, कामायनी, मधुशाला आदि के ऐसे-ऐसे छन्द रटाये, जिनकी कोई काट न हो। हर ‘‘डिबेट टापिक‘ से संबंधित वे स्वयं ‘पवाइंट्स‘ बनाते थे और रिहर्सल करवाते थे। मेरे बाहरी प्रतियोगिताओं में स्वयं साथ-साथ जाते थे और जो ट्राफी मिलती थी, उसको लेकर कालेज में उत्सव मनाते थे। अपने प्रश्न पत्र में एक बार उन्होंने हिन्दी में मुझे 100 में 93 नम्बर दिए और उस कापी का सार्वजानिक प्रदर्शन तक कराया। उन्होंने कालेज की पत्रिका का मुझे छात्र सम्पादक बनाया और उसमें 1956 में मेरा पहला-पहला समीक्षात्मक लेख ‘‘साहित्य में लोक मंगल‘‘ छापा। इससे मेरे मन में लिखने और बोलने की क्षमता का अवश्य ही विकास हुआ होगा। मेरे ग्राम गुरु चंद्रमणि जी उन्हीं दिनों ‘रायबरेली के कवि‘ नामक एक पुस्तक लिख रहे थे। उनके पास काफी कच्चा माल था, पर वे प्रायः यात्रा पर रहते थे। वे कभी-कभी कुछ सामग्री मुझे दे जाते थे। मैं उसको परिचयात्मक निबन्ध के रूप में ढाल देता था। हिन्दी साहित्य के इतिहास से हमने रायबरेली-निवासी कुछ अल्पख्यात लेखक खोज लिए थे। इन सब पर लिखते हुए मन में यह विश्वास अवश्य जागा होगा कि मैं भी समीक्षात्मक लेख लिख सकता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के गुरुओं की प्रेरणा से मैंने तुलसी, सूर, जायसी, कबीर, प्रसाद, निराला, मैथिलीशरण, दिनकर, प्रेमचन्द आदि को विशेष रुचि के साथ पढ़ा। पहले मुझे संस्कृत अति प्रिय थी और हिन्दी तो थी ही। स्मरण शक्ति अच्छी थी, वक्तृत्व कला काफी सीख ली थी, इसलिए उत्तरोत्तर जीवन यात्रा सुविधापूर्वक बढ़ती रही।
मेरा अनुमान है कि साहित्य सेवा की अभिरुचि आपमें काव्य रचना के कारण पैदा हुई है। क्या यह सही है?
हाँ, यह सही है। हिन्दी विषय की ओर आने का मुख्य कारण था काव्य-रचना से लगाव। हाईस्कूल में पढ़ते हुए मैं नवोदित मंचीय कवि के रूप में चर्चित हो चला था। तब मेरा कंठ काफी सुरीला था और गीत गायन मैं बड़े हाव-भाव के साथ करता था। तब गाँव-गाँव में कवि गोष्ठियाँ होती रहती थीं। मैंने अपने विद्यालयी मंच से लेकर कई संस्थागत मंचों पर काव्य पाठ किया। मुझे प्रोत्साहित करने वालों में प्रमुख थे-आशुकवि जगमोहन नाथ अवस्थी जी (लखनऊ) अमरेश जी (रायबरेली) दिवाकर त्रिपाठी (उन्नाव) आदि। बी. ए. में पढ़ते हुए मैंने लखनऊ के कई साहित्यकारों का कृपा-प्रसाद प्राप्त किया, जिनमें माधुरी संपादक पं. रूपनारायण पाण्डेय, गुरुवर डॉ० भगीरथ मिश्र, डॉ.. ब्रजकिशोर मिश्र, प्रथम देव पुरस्कार विजेता दुलारे लाल भार्गव, तोरन देवी ‘लली‘, नागर जी, यशपाल जी, पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी, निशंक जी, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम अग्रगण्य हैं। इस बीच मैंने ‘मंजरी‘ नामक एक काव्य-संकलन अपने ताऊजी के सौजन्य≶ोग से प्रकाशित किया। मेरे अग्रज देवी प्रसाद दीक्षित ‘देवेश‘ और मैं ‘सुरेश‘ दोनों की कविताएँ ‘दीक्षित बन्धु‘ के नाम से उसमें समहित की गयी थीं। इस कविताई का नशा कुछ इतना ज्यादा मेरे दिलोदिमाग में बैठ गया था कि समीक्षात्मक पुस्तकें पढ़ने से उच्चाटन होने लगता। इससे बी.ए. प्रथम वर्ष का मेरा परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हुआ। निदान, एक दिन मैंने यह शपथ ली कि अब कविता नहीं लिखूगा। केवल पढ़कर और पढ़ाकर काव्य का आनन्द-लाभ करूँगा। इसी तरह आरम्भ में कुछ कहानियां, एकांकी, लेख आदि मैंने लिखे थे। उनसे भी विदा ले ली और केवल आलोचनात्मक अध्ययन में केन्द्रित हो गया। मुझे कोई न कोई छात्रवृत्ति निरंतर मिलती रही। उस युग में इतनी धनराशि मेरे लिए पर्याप्त थी, अतः मुझे कभी अभिभावकों से आर्थिक सहायता नहीं माँगनी पड़ी। मैं लखनऊ में सात वर्ष रहा। खाद्य सामग्री घर से आ जाती थी। किराये का कमरा हम दो साथियों ने ले रखा था। भोजनादि की व्यवस्था हम स्वयं कर लेते थे। सादा सात्विक मितव्ययी जीवन था। केवल किताबें खरीदने का व्यसन ही एक मात्र खर्चीला मुद्दा था। यथासमय मैंने बी.ए., एम.ए. की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। एम.ए. में सर्वप्रथम स्थान होने के कारण मुझे रायबरेली के एक नवस्थापित डिग्री कालेज से अध्यापन कार्य का निमंत्रण मिला, किन्तु धुन सवार थी पीएच.डी. करने और विश्वविद्यालय में नौकरी करने की। उसी बीच भगवत् कृपा से मुझे तीन वर्षों के लिए यू.जी.सी. की फेलोशिप मिल गयी। लगातार जुटकर 1963 में मैंने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया। उसके तुरंत बाद विवाह हो गया और उसी बीच जोधुपर विश्वविद्यालय में नौकरी लग गयी। तब से मैं शोध-समीक्षा में केन्द्रित होकर साहित्य सेवा में भरसक संलग्न हूँ।
आपके कैशोरकाल की कुछ खट्टी मीठी स्मृतियाँ अवश्य होंगी? सम्भव है, उनसे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आए हों?
अपने किशोरकाल की जब सुधियाँ सँजोता हूँ तो मन में कुछ कडुवाहट भी भर जाती है। कभी-कभी मुझे घर के आहाते में लगे नीम के पेड़ (तने) से बँधे हुए, पीटे जाते हुए, रोते चिल्लाते हुए कर्जमंद गरीब मजदूरों के स्वर मुझे सुनायी देते हैं, जो पोत, (लगान) न अदा कर पाने के कारण दण्डित किए जाते थे। मुझे वह दृश्य भी रह-रहकर याद आ जाता है, जब सावन-भादों के महीनों में अनाज उधार लेने वालों की लम्बी पंक्ति घर के सामने लग जाती थी। उन दिनों प्रायः बाढ़ आती रहती थी, जिससे बहुत सारी खेती नष्ट हो जाती थी। चैत्र से आषाढ़ तक तो लोग किसी प्रकार ‘निर्वाह कर लेते थे, पर सावन-भादों में अन्न का संकट आ जाता था। एक कहावत प्रचलित थी कि सावन में सुवा (तोता) भी उपास (उपवास) करता है, यानि तोते को देने के लिए दो चम्मच आटा भी कई लोग नहीं जुटा पाते थे। तब बिजली नहीं थी, वाटर पम्प नहीं थे। प्रायः सूखा भी पड़ जाता था। चीनी, केरोसिन और कपड़ा लेने के लिए कई-कई मील चलकर कोटेदार के पास जाना होता था। उन दिनों ब्रह्म भोज (दावतें) खाने का बड़ा शौक था। आस-पास के गांवों से लोग यह संदेश मेरे घर भेज देते थे कि अमुक दिन इक्कीस ब्राह्मण लेकर आइए। इन ब्रह्म भोजों में तरह-तरह की लीलायें और प्रतियोगिताएँ होतीं थीं। लोग कौतुकी दृष्टि से देखते थे कि किसने कितनी पूड़ियाँ खायीं या प्रति चवन्नी इनाम लेकर कितने लड्डू पेड़े खाए। तब एक से एक भोजन भट्ट थे। इन दंगली भोजन भट्टों को देखने के लिए मैं भी भोजयात्रा में कभी-कभी सम्मिलित हो जाता था। इससे बड़ा लोमहर्षक, बल्कि भयावह दृश्य होता था महाभोज का। उसमें गाँव-जॅवार का पूरा जनसमूह सम्मिलित होता था। किसी को व्यक्तिगत नियंत्रण न देकर केवल डुग्गी पिटवा दी जाती थी। इस भोज में स्थायी नागरिकों के अतिरिक्त कितने कुदुवा (यायावर, घुमन्तू) लोग आकर पंगत में बैठ जाएँगे, इसका पूर्वानुमान कोई नहीं लगा पाता था। गृहस्वामी युक्ति पूर्वक भोजन सामग्री की तात्कालिक व्यवस्था करता था। इन्हें खिलाने के लिए विशेषज्ञ लोग बुलाये जाते थे। ये भोजनार्थी जितना खाते थे, उतना ही माल चुरा लेते थे। उनकी खूराक भी आश्चर्य जनक थी। यदि कोई पूड़ी सब्जी मिष्ठान्न यानि सब पदार्थ परोसने लगे तो इनका पेट ही नहीं भर पाता था। इनका मुँह बाँधने के लिए पूड़ी के साथ केवल पिसी घुटी शकर दी जाती थी। खटाई एवं नमकीन की बिल्कुल मनाही। बीच में पानी भी नहीं। शकर फाँकते-फाँकते इनका मुँह बन्द हो जाता था। दस बारह सुहारियों (बड़ी पूड़ियों) से ज्यादा नहीं खा पाते थे। बचपन में मैंने ऐसे भोजों में तीन-तीन हजार कुदुवे भोजनार्थी देखे हैं। इधर दस वर्षों से कुदुवा-प्रथा समाप्त हो गयी है। अब तो ब्रह्म भोजों में बहुत मनुहार करने से लोग आते हैं और वे भी प्रायः अवयस्क। एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से जुड़े होने के कारण जनेऊ हो जाने के बाद मैं बहुत दिनों तक यथासमय सुस्वादु भोजन से वंचित रहा। तब कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपने परिजनों द्वारा बनायी गयी रसोई के अतिरिक्त कहीं भोजन नहीं कर सकता था। मैंने सात वर्षों तक प्रातः काल केवल खिचड़ी खाकर गुजर-बसर की। मुझे प्रातः पूजापाठ करके नौ बजे बछराँवा कालेज के लिए रवाना होना पड़ता था। तब तक इतने बड़े संयुक्त परिवार में मेरे लिए पवित्र (अनूठी) रसोई नहीं तैयार हो सकती थी। किसी प्रकार लकड़ी जलाकर चूल्हे में खिचड़ी भरी. बटलोई चढ़ा दी जाती थी और वह स्वतः पक जाती थी। पूजनोपरान्त वह प्रसाद पाकर मैं पढ़ने चला जाता था। सांयं पाँच बजे तक घर लौटता था। तब गाँवों में चाय एवं नाश्ता का चलन नहीं था। केवल चना-चबैना मिलता था। भोजन की बारी रात दस बजे के आस-पास आती थी। जलपान के रूप में गुड़ का प्रचलन था या राब के शर्बत का। कभी-कभी फसली फल मिल जाते थे। सभी बड़े यही उपदेश देते रहते थे कि ‘कम खाओ, गम खाओ।‘ व्रत के नाम पर उपवास बहुत करने पड़ते थे। स्वयं पाकी होने का इतना अभ्यास करा दिया गया था कि लखनऊ में बी.ए. करते हुए कभी कोई समस्या नहीं हुयी। यज्ञोपवीत करते हुए आचार्य जी ने यह संकल्प कराया कि मैं दो बार संध्योपासन जरूर करूँगा और दोनों वक्त शिव मन्दिर की पूजा भी। बारह से अट्ठारह वर्ष की आयु तक यह आध्यात्मिकता मेरे दिलोदिमाक में इस तरह भरी रही कि घर वालों को यह शंका होने लगी कि कहीं मैं वैरागी न हो जाऊँ। कुण्डली में मेरा राशिनाम था संतप्रसाद और वृत्ति में लिखा हुआ था साधु जीवन। इन सबके कारण खेल-कूद के प्रति कभी रुचि ही नहीं पैदा हुयी। बस दो रुचियाँ निरंतर रहीं। एक तो अन्त्याक्षरी, वाद विवाद, संगीत प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियों में गीत गायन और दूसरी रामलीला तथा नाटकों में अभिनय। हमारे गाँव की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध थी। मैं जूनियर हाईस्कूल में था, तभी लक्ष्मण रूप में परशुराम से जोशीला संवाद करने का अभ्यास मुझे कराया गया था। मैंने जोर-जोर से चिल्लाकर और रुके बिना सारा संवाद बोलकर लोगों को इतना खुश कर दिया कि मुझे कई वर्षों में कई सारे इनाम मिले। इसके बाद छह सात वर्षों तक मैं राम की भूमिका में रहा। आस-पास के कई कस्बों में होने वाली रामलीला में मुझे राम का ‘सरूप‘ बनाया जाता था। दशहरे पर जब रामजी की सवारी निकलती थी तो धार्मिक जनता इतना प्रणिपात करती थी, इतना चढ़ावा अर्पित करती थी कि मन पुलकित हो जाता था। रामलीला शुरू होने के दस दिन पूर्व से रोज गाँव का नाई मेरा उबटन (प्रसाधन) करने आता था। पुरोहित जी की पूरी देख रेख रहती थी। तब लोगों में यह विश्वास था कि जो रामजी का स्वरूप
धारण करता है, उसमें प्रभु जी का भावावतार हो जाता है। इन सब कार्यक्रमों का जाने-अनजाने यह प्रभाव अवश्य पड़ा कि गदहपचीसी की उम्र में भी मेरी चित्तवृत्ति विचलित नहीं हुयी। मैं हमउम्र किशोरों के ‘साथ कम और समाज के प्रतिष्ठित कवि-लेखक, पंडित, पुजारी, शिक्षक वर्ग के साथ ज्यादा जुड़ा रहा। इण्टर तक मेरे आदर्श रहे-मेरे ग्राम्य गुरु चन्द्रमणि जी, मेरे मानस गुरु मुंशी चन्द्रिकाप्रसाद (गुरूजी) और स्नातक कक्षा से पीएच.डी. पर्यन्त मेरे आदर्श बने रहे-हिन्दी विभाग के कई गुरुजन। साहित्यकारों में नागर जी, आशुकवि मोहन, पं. रूपनारायण पाण्डेय, भगवती बाबू आदि। इन सबके सान्निध्य के कारण जीवन में कई मोड़ आए, जैसे सिविल सेवा में उत्तीर्ण होकर भी मैं शिक्षण सेवा से जुड़ा रहा।
लखनऊ प्रवास के बीच तरुणावस्था में आपने अपने में क्या परिवर्तन देखा?
शोध कार्य में प्रवेश लेने के बाद मेरा अध्ययन केन्द्र बना विश्वविद्यालय टैगोर पुस्तकालय और आचार्य नरेन्द्रदेव अंतरराष्ट्रीय छात्रावास। वहाँ विभिन्न विषयों के शोधार्थियों से संपर्क हुआ। असली लखनवी अदायें तभी देखने को मिलीं। उनसे बहस करते हुए विभिन्न विषयों की जानकारी मुझे मिली और बौद्धिक आभिजात्य के कुछ संस्कार भी। खानपान की बंदिशें अब समाप्त हो गयीं थीं। पहनावे में भी आधुनिक यानि सूटेड बूटेड। टाई लगानी शुरू कर दी थी। यद्यपि दिनचर्या में पुरानी पढ़ाकू प्रकृति कायम थी। उन दिनों छात्रावास में पढ़ रहे अन्तेवासी को कोई असमय छेड़ता नहीं था। क्लास में टॉप करने का जुनून प्रायः विद्यार्थियों में सवार रहता था, इसलिए मेरा अध्ययन अबाध गति से चलता रहा। अपने प्रोफेसरों को देखकर महत्वाकांक्षा जग गयी थी विश्वविद्यालय में शिक्षक होने की। बड़ी विकट स्पर्द्धा थी, इसलिए बाहरी दुनिया की चकाचैंध से भरसक कटा रहा। पहले फिल्मों के प्रति बड़ी अरुचि थी। मेरे ग्राम-गुरु ने भली प्रकार यह समझा दिया था कि फिल्म देखने से बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं, सो बी०ए० करने तक मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी। एक बार मेरे अग्रज जबरदस्ती पकड़कर ले गए तो मैं मनमारे बैठा रहा। जहाँ नाच गाना शुरू होता था, वहाँ आँखें बंद कर लेता था। मेरे इस नीरस स्वभाव और आचार्य श्री द्वारा लादे गए विकट ब्रह्मचर्य व्रत के कारण कभी कोई प्रणय-प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ,। शायद समय ही नहीं मिला या साहस ही नहीं हुआ। मैंने गाँव में एक पुस्तकालय खोल रखा था। लोगों के पढ़ने के लिए घर-घर किताबें पहुँचाता था। वहां भरसक एक साक्षरता अभियान भी चलाता था। भारत सेवक समाज की एक शाखा खोल रखी थी। उसकी टीम यदा कदा सफाई अभियान चलाती थी। नुक्कड़ नाटक खेलती थी और सामाजिक दायित्व संभालती थी। तरुणावस्था आते-आते काफी आधुनिक तो गया था, किन्तु लोक भीरुता और आदर्श प्रियता बराबर बरकरार रही।
हिन्दी विषय को अपना कैरियर बनाने की प्रेरणा कैसे कहाँ से प्राप्त हुई?
मेरी प्रिय भाषाएं थी संस्कृत और हिन्दी। विभिन्न प्रकार के दैहिक, भौतिक परिवर्तनों के बावजूद ग्रामीण प्रकृति एवं कृषि संस्कृति के भीतर रहते हुए मैं हिन्दी भाषा साहित्य की दिशा में अपेक्षाकृत ज्यादा सफल हुआ। बी.ए. कक्षा तक यह असमंजस रहा कि मैं एम.ए. संस्कृत में करूँ था हिन्दी में? किन्तु उसी दौरान संस्कृत विभाग के अन्तः कलह एवं शिक्षकों के जड़ व्यवहार से क्षुब्ध होकर, दूसरी ओर हिन्दी विभाग के कई गुरुजनों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से संमोहित होकर मैं मन वचन कर्म से हिन्दी विभाग से जुड़ गया। दो वर्ष बड़े सुख से बीते। एम.ए. कर लेने के बाद, जैसा सुन रखा था, मेरे मन में यह दुराशा व्याप्त हो गयी थी कि टॉपर होने के कारण मुझे यथाशीघ्र नियुक्ति मिल जाएगी। कुछ ही दिनों बाद यथार्थ बोध हुआ, जिसने उद्विग्न कर दिया। मुझे विभाग में कई वर्षों से बैठे हुए बेरोजगार टॉपर दिखे। तब सारे पद तदर्थ नियुक्तियों से भर दिए जाते थे। राजनीतिक हस्तक्षेप अपनी अति पर था। पूरा गुप्त साम्राज्य चल रहा था। मैंने शोध में प्रवेश ले लिया था। संयोगवशात् यू0जी0सी0 की फेलोशिप मिल गयी थी। रातोंदिन जुटकर मैंने तीन वर्षों में थीसिस पूरी कर ली। तभी परिवार ने वीटो लगा दिया और मुझे विवाह करना पड़ा। प्रश्न उठा, स्थायी आजीविका का। मैंने आवेदन पत्र भेजने शुरू किए। रायबेरली कालेज और शाहजहाँपुर के कालेज से नियुक्ति के न्यौते मिले थे, पर मन नहीं माना। उससे ज्यादा राशि फेलोशिप की थी। इस बीच मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग में इण्टरव्यू दिया, गवर्नमेंट गजटेट पोस्ट के लोभ वश। वहाँ से नियुक्ति पत्र आया, किन्तु बहुत विलंब से। उसके पूर्व जोधपुर विश्वविद्यालय में मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार हिन्दी शिक्षण मेरा कैरियर बन गया।
आपका जोधपुर-प्रवास कैसा रहा?
मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय में इण्टरव्यू दिया और नियुक्ति पत्र पाते ही जुलाई 1963 में कार्यभार ग्रहण कर लिया। भौगोलिक दूरी के बावजूद विश्वविद्यालय-सेवा का आकर्षण बड़ा प्रबल था। अस्तु, वहाँ तेरह वर्ष बिताये। वहीं तीनों बच्चे जनमे और बढ़े। सहधर्मिणी मंजु ने वहीं गृहस्थी जमायी। परम्परावादी आचार्य, अलंकार शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित रसाल जी (हिन्दी विभागाध्यक्ष) से मुझे भरपूर संरक्षण मिला। 4 वर्षों तक सुकवि-समीक्षक कुँवर चन्द्रप्रकाश जी की अध्यक्षता में रहा। पाँच वर्षों तक प्रसिद्ध आधुनिक आलोचक डॉ. नामवर सिंह के नेतृत्व में काम किया और उसी बीच दो वर्षों तक एक विराट विजन के रचनाकार ‘अज्ञेय जी‘ का सान्निध्य प्राप्त किया। जोधपुर में मैंने मुनि जिनविजय जी के निर्देशन में पाठालोचन-विद्या सीखी। ‘राजस्थान पत्रिका‘ के ‘कुलिश जी‘ का संपादन देखा। हिन्दी व्रती राठी जी के साथ ‘राष्ट्रभाषा आन्दोलन‘ चलाया और रंगकर्मी कुलश्रेष्ठ जी के नाट्य क्लब से जुड़ा रहा। जोधपुर में मेरा शिक्षक, शोधक, समीक्षक रूप निर्विन गतिमान रहा। बारह वर्षों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान सामने नहीं आया। लोगों से भरपूर स्नेह सम्मान मिलता रहा। सात वर्ष बाद ही वरिष्ठता क्रम में सोलहवें स्थान पर होने के बावजूद वहाँ रीडर के रूप में मेरा चयन कर लिया गया था। बस, शासकीय अनुमति की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्कालीन विभागाध्यक्ष, मेरे गुरुवर की ओर से भेजा हुआ एक आवेदन पत्र मुझे इस आदेश के साथ मिला कि इसे तुरंत भरकर भेजो। अस्तु, आवेदन किया, इण्टरव्यू दिया और जिस दिन कार्यकारिणी से पुष्टि हुई, उसके दूसरे दिन लखनऊ में रीडर के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कालक्रम में यहीं आवास-व्यवस्था हो गयी, परिवार ठौर-ठिकाने लग गया और जहाज का पंछी फिर अपने जहाज पर लौट आया। कुल मिलाकर सब अच्छा रहा।
लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में आपने 24 वर्ष (यानी दो युगों) तक कार्य किया। साढ़े बारह वर्ष आप विभागाध्यक्ष रहे। यह कार्यकाल कैसा रहा?
1976 से 1986 तक मैं हिन्दी विभाग में एकमात्र रीडर के रूप में कार्यरत रहा। विश्वविद्यालय व्यवस्था में सुधार का संकल्प लेकर दो वर्षों तक विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में उपाध्यक्ष-अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहा। एक वर्ष विश्वविद्यालय कार्यकारिणी का सदस्य रहा। इन सबके साथ-साथ मैंने साहित्यिकी संस्था, उत्कर्ष, उद्भव चाणक्य, संचार श्री, साहित्य भारती, प्रभास, खोज आदि पत्रिकाएँ समय≤ पर चलायीं। उसी बीच कई वर्षों तक बछराँवा में डिग्री कालेज स्थापित करने के अभियान में लगा रहा। साथ ही पठन-पाठन, शोधपत्र, पुस्तक-लेखन का क्रम चलाता रहा। पत्र-पत्रिकाओं में छपने का तब बड़ा शौक था। कभी-कभी पुस्तक समीक्षाएँ, ज्यादातर सैद्धांतिक शोध-समीक्षा से संबद्ध लेखन। तब पैसा देकर छपवाने का चलन नहीं था। संपादक साग्रह लेख मँगवाते थे। हाँ, समय बहुत कम देते थे। कभी-कभी मानदेय भी भेज देते थे। यों, पत्रिकाएँ. तो नियमित आती ही थीं। ऐसी पत्रिकाओं का विपुल भण्डार मेरे पुस्तकालय में सुरक्षित है। इनके कारण पुस्तकों, पाण्डुलिपियों चित्रावली तथा पत्रिकाओं के संकलन की एक हाॅवी मन में पैदा हो गयी। जोधपुर से जब लखनऊ के लिए चला तो मालगाड़ी का आधा डिब्बा किताबों के बण्डलों से भरा हुआ था और आधा घर गृहस्थी के उपकरणों से। लखनऊ में ‘साहित्यिकी‘ नामक जो आवास बनवाया, उसकी दूसरी मंजिल में संप्रति यह पुस्तकालय चल रहा है। आज उसमें लगभग पच्चीस हजार पुस्तकें और पत्रिकाएँ हैं। मेरा प्रयास रहा है कि हर महत्वपूर्ण पत्रिका अथवा विशेषांक, मूल अथवा फोटोकाफी तथा आवश्यक पाण्डुलिपियाँ हमारे संग्रह में अवश्य हों। यदा-कदा लोग दूर-दूर से दुर्लभ ग्रंथों की खोज में आते हैं तो उनकी सहायता करते हुए सार्थकता की अनुभूति होती है। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को लगता है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ‘साहित्यिकी‘ में अवश्य मनचाही सामग्री हर समय निःशुल्क उपलब्ध है। इन बारह वर्षों में समीक्षा से ज्यादा मैं शोध विधा में ज्यादा केन्द्रित रहा। वह भी अपेक्षाकृत ऐतिहासिक शोध में।
यहाँ कार्य करते हुए आपने शोध समीक्षा की दिशा में काफी पहल की है। उसके संबंध में कुछ बताइए।
मैंने यह अनुभव किया कि समकालीन रचनाओं एवं रचनाकारों पर किया गया कार्य खोज न होकर समीक्षा है। खोज उसकी की जाती है, जो खो गया हो। मैंने आदिकाल से लेकर द्विवेदी युग तक के भूले-बिसरे साहित्यकारों, पत्रकारों, भाषाविदों, हिन्दी प्रचारकों, संस्थाओं और ऐतिहासिक घटनाचक्रों को शोध समीक्षा का विषय बनाया। जैसे सतीप्रथा के साहित्यिक साक्ष्य क्या है? गदर एवं जलियाँवाला काण्ड के बारे में तत्कालीन साहित्य क्या कहता है? विभिन्न विचारधाराओं का विकास कैसे हुआ? जनपदीय बोलियों और विश्व हिन्दी का क्या भविष्य है? तुलनात्मक साहित्य, लोकसाहित्य, ज्ञान विज्ञानपरक लेखन और रोजगारपरक लेखन का विकास कैसे किया जाये?
शोधकार्य से विश्लेषण, सर्वेक्षण, इण्टरनेट आदि को कैसे जोड़ा जाये? इन दिशाओं में कार्य करते हुए, पाठ्यक्रम में इन्हें पढ़ाते हुए, इन पर लिखते हुए, बोलते हुए आज लगभग साठ वर्ष हो गए। इधर जीविका से जुड़ जाने, मुख्यतः ए.पी.आई. की छद्म पूर्ति के कारण हिन्दी शोध का स्तर बहुत गिर गया है, जबकि शोधकार्य को ही ज्ञान क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है। इसको बचाने-बढ़ाने का भरसक प्रयास मैंने किया है और यावत्जीवन करते रहने के लिए मैं प्रतिश्रुत हूँ।
आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक हिन्दी एवं पत्रकारिता के अध्यक्ष के रूप में दायित्व वहन किया है। वह कार्यकाल आपकी दृष्टि में कैसा रहा?
मुझे 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर-अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। आरंभ में ही मुझे यह अनुभव हुआ कि हिन्दी भाषा-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन अन्वेषण के पीछे मुख्य चार ध्येय होने चाहिए (1) लगभग डेढ़ हजार वर्षों के भाषा साहित्य का समग्र संज्ञान तथा इतिहास बोध। (2) इस विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को जीविका के समुचित संसाधन प्रदान करना। (3) नयी पढ़ी में सम्यक मानुष भाव भरना। (4) हिन्दी के संपर्क भाषा होने के कारण, उसके सहारे राष्ट्रीय भावैक्य की स्थापना का प्रयास करना।
इन्हीं बिन्दुओं के अनुरूप मैंने निश्चय किया कि हिन्दी पाठ्यक्रम का नव निर्माण और सुविचारित पठन-पाठन होना चाहिए। इसी भाव से प्रेरित होकर मैंने साहित्याध्यात्म, हिन्दीतर राज्यों का हिन्दी साहित्य, तुलनात्मक भारतीय साहित्य, विश्व हिन्दी, प्रयोजन मूलक हिन्दी (अनुवाद, वेटिंग, दुभाषिया, डबिंग, संक्षेपण, रूपांतरण, भाष्य) पत्रकारिता (जनसंचार, जनसंपर्क, मीडिया लेखन, फीचर, रेडियो वार्ता, पटकथा, रिपोर्ताज, समाचार लेखन संपादन, प्रचार साहित्य (विज्ञापन) संभाषण कला (कमेंट्री, संचालन, उद्घोषण) लोक वांग्मय, जनपदीय साहित्य, पाठालोचन, भाषा शिक्षण, सर्जनात्मक प्रशिक्षण, रंगमंच, राजभाषा प्रशिक्षण आदि की शुरूआत की।
रोजगार परक पाठ्यक्रम को स्थापित करने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा? इस क्षेत्र में जो सफलता मिली, उसके हेतु कौन-कौन हैं?
यह पाठ्यक्रम काफी चुनौती भरा हुआ था। विभाग में न पर्याप्त विशेषज्ञ थे और न उपकरण। मैंने स्ववित्तपोषित नीति के अनुसार इसकी शुरुआत की। सहयोगियों ने नए विषयों को स्वयं पढ़-पढ़कर मेरे साथ-साथ पढ़ाना शुरू किया। अपने संसाधनों से हमने एक प्रयोगशाला तैयार की। कई विशेषज्ञों ने अतिथि शिक्षक के रूप में हमें सहयोग दिया। इस कार्यकाल में कई प्रकाशन, कार्यशालायें और गोष्ठियाँ हुयीं। अनुवाद का जो द्विवर्षिय एम.ए. पाठ्यक्रम चला, उसका वित्तीय संस्थाओं, विशेषतः बैंकों ने स्वागत किया। वार्षिक परीक्षा होने के पूर्व ही बैंकों ने कैंपस इण्टरव्यू करके इन छात्रों की अग्रिम बुकिंग कर ली। उन्हीं दिनों कई देशी-विदेशी टी.वी. चैनल्स शुरू हुए थे। 1990 में हमने पत्रकारिता पाठ्यक्रम शुरू किया। हमारे मीडिया-छात्रों को कई विभागों में स्थान मिला। यहाँ राजभाषा का जो प्रशिक्षण शुरू हुआ था, उसे उत्तीर्ण करके हमारे अनेक विद्यार्थी राजभाषा अधिकारी हो गए। कई भाषा-शिक्षण से जुड़े गए। हमारे विभाग ने यू.जी.सी. नेट परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग शुरू की। लोक साहित्य, लोक संस्कृति की श्रीबृद्धि हेतु विभाग ने लखनऊ के पड़ोसी जिलों में लोक-सर्वेक्षण कराया। विभाग में लोक वांग्मय का पुस्तकालय तैयार किया गया। ये सारे कार्यक्रम सरकारी अनुदान के बिना, मात्र सहकारिता के सहारे चले। विभाग में दस-दस रूपये में आठ पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गयीं। जो बचत हुई उससे तीस राष्ट्रीय गोष्ठियाँ हुईं। ‘ज्ञानशिखा‘ त्रैमासिक के उनतीस विशेषांक प्रकाशित हुए और एक दर्जन शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए। इस प्रकार हिन्दी विषय के साथ जुड़ा हुआ हीनताबोध काफी कुछ धुल गया। संभावनाओं के कई नए क्षितिज खुल गए। फलतः यू.जी.सी. ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्मित कराते हुए इस ‘लखनऊ माडल‘ को अनुमन्यता देदी। इस सफलता के हेतु हैं, मुख्यतः मेरे सहयोगी एवं अधिकारी।
आपका विभाग भारतीय भाषाओं का भी पठन-पाठन कराता रहा है। आपने उस दिशा में नया क्या जोड़ा?
हमारा विभाग 1950 से हिन्दी के साथ आधुनिक भारतीय भाषा विभाग रहा था। तमिल, ‘ मराठी और बंगाली भाषायें बहुत दिनों से पढ़ायी जा रही थीं। इस बीच तेलुगु, मलयालम, गुजराती और पंजाबी भाषायें जोड़ी गयीं। ‘विश्व हिन्दी‘ की रूप-रचना करते हुए फिजियन, सरनामी, त्रिनी, मॉरिशन आदि के साथ-साथ प्रवासी लेखन को यहाँ बढ़ावा दिया गया। अवधी भाषा का एक केन्द्र यहाँ स्थापित हुआ और साथ ही महत्वपूर्ण जनपदीय विभाषाओं के अध्ययन की शुरूआत हुई।
आप शोध को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। आपके पीएच.डी., डी. लिट् के शोध प्रबंध सराहे गए हैं। अस्तुः शोध की गुणवत्ता वृद्धि हेतु आपने क्या-क्या कार्य किए?
मेरे दोनों शोध ग्रंथ प्रकाशित हैं। हिन्दी जगत ने उन्हें सराहा है। शोध के स्तरोन्नयन की दिशा में मैंने सर्वाधिक श्रम किया हैं। मेरा यह शुरू से मत रहा है कि शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र है विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रदेय होता है शोध कार्य। मैं बहुत दिनों से हिन्दी शोध की दशा-दिशा को लेकर दुःखी हूँ। आप सहमत होंगे कि इन दिनों हिन्दी शोध मुख्यतः समकालीन कविता और कथा कृतियों की पुस्तक-समीक्षा में सिमट गया है। खोज का अर्थ है खोये हुए को खोजना। वास्तविक खोज या तो इतिहास में जाकर होती है या जन सर्वेक्षण के माध्यम से। युवा शोधार्थी नयी मौलिक सैद्धांतिक खोज प्राचीन साहित्य, भाषाशास्त्र, काव्यशास्त्र, इतिहास दर्शन जैसे विषयों में सहजतः नहीं कर सकते। इन्हें लोक साहित्य एवं भाषा सर्वेक्षण के लिए भेजना अथवा पुरातात्विक महत्व वाले हस्तलेखों की खोज हेतु प्रेरित करना अपेक्षाकृत ज्यादा हितकर होगा। निजी संग्रहालयों में न जाने कितना वांग्मय दबा पड़ा है। जनपदीय बोलियों का लोक साहित्य विलीन होता जा रहा है। हिन्दी परिवार की विभाषाओं के सामने कई समस्यायें हैं। न जाने कितने कवि-लेखक हैं, जिनका प्रामाणिक जीवन वृत्त नहीं बन पाया है, किन्तु दुर्भाग्य कि इन विषयों पर शोधकार्य करना-कराना बंद हो गया है। शोधकार्य समकालीन प्रकाशित विज्ञापित साहित्य में सीमित है। वह कुछ प्रभावशाली जीवित व्यक्तियों में केन्द्रित हो गया है। निर्देशक आदान-प्रदान के सहारे जिनको कृतार्थ करना चाहते हैं, उन पर शोध-विषय दे देते हैं और फिर वे इसे प्रतिष्ठा-प्रतीक मानकर अपने परिचय में छपा देते हैं कि उनके व्यक्तित्व-कर्तृत्व पर अमुक विश्वविद्यालय ने शोध कराया है। इन दिनों यह एक उद्योग बन गया है। महाविद्यालयों के शिक्षकों को निर्देशक बना देने के कारण स्थिति अनियांत्रित सी हो गयी है। विभागाध्यक्षों, शोध समितियों, संयोजकों, निर्देशकों के पास शोधोपयुक्त मौलिक तथा उपयोगी विषयों की कोई तालिका नहीं है। एक-एक कवि पर कई-कई सौ थीसिसें लिखी जा चुकी हैं। भूतलेखन, चैर कर्म और तस्कर व्यापार भी जोरों पर चल रहा है। निर्देशन नाममात्र का होता है। विभागों में शोध कक्ष, पुस्तकालय, शोधवृत्ति आदि की व्यवस्था न के बराबर है। सरकार जो फेलोशिप देती है, वह राशि इतनी ज्यादा होती है कि शोधार्थी शोध-साधना से विमुख होकर गार्हस्थ भोग से जुड़ जाता है। परीक्षण कार्य एक व्यवसाय अथवा कर्मकाण्ड बनकर रह गया है। वाइवा तो वसूली का वाह-वाह हो गया है। शोध प्रबंधों का श्रेणीकरण (उत्तम श्रेणी, मध्यम या अधमश्रेणी का निर्धारण) होता नहीं है। सब धान बाईस पसेरी माना जाता है। इन शोध प्रबंधों का बहुत कम प्रकाशन हो पाता है। कुछ धनी मानी व्यक्ति किसी पेशेवर प्रकाशक को अग्रिम धन देकर सौ पचास डमी प्रतियाँ ए.पी.आई. में दर्ज कराने के लिए बनवा लेते हैं। अधिकतर शोध प्रबंध अध्ययन के इतिहास में अपना योगदान दर्ज न कराकर गोदामों में सड़ते रहते हैं अथवा रद्दी के भाव बिकते रहते हैं।
इस दुर्दशा से द्रवित होकर हमने विभाग में कई वर्षों तक शोध-उन्नयन का अभियान चलाया। हमने निश्चित किया कि जीवित सक्रिय रचनाकारों पर रिसर्च न करायी जायेगी। जब राष्ट्रस्तरीय लेखक की अपनी एक छवि स्थिर हो जाये, तब उसे शोध का विषय बनाया जाये। काव्य, कथा, नाट्य लेखन आदि की प्रवृत्तियाँ और शैलियाँ जब साहित्येतिहास में अपना स्थान बना लें तब उन को शोध का आलबंन बनाया जाये। शोध विषयों की आवृत्ति तो कदापि न होने पाए। अल्पख्यात प्राचीन रचनाकारों को वरीयता दी जाये। अप्रकाशित, असंकलित-रचनाओं, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों पर प्रकाश डाला जाये। लोक वांग्मय मुख्यतः जनपदीय साहित्य का जिलेवार सघन सर्वेक्षण, विश्लेषण कराया जाये, जिससे हिन्दी - साहित्य के इतिहास का सही पुनर्लेखन हो, हिन्दी की अपनी भाषिक प्रकृति-संस्कृति निर्मित हो और हिन्दी के अपने स्वतंत्र साहित्यशास्त्र का निर्माण हो सके।
इस दृष्टि से मैंने ‘विभाग में एक शोध कक्ष स्थापित किया। एक शोध संग्रहालय बनवाया। तब तक (1987) के स्वीकृत शोध प्रबंधों को इकट्ठा कराया। स्वीकृत शोध विषयों की तालिकाएं तैयार की। मैंने प्रतिवर्ष शोधोपयुक्त सौ विषयों की स्टैण्डर्ड लिस्ट बनवायी। विशेषज्ञता के अनुसार निर्देशकों-परीक्षकों की नियुक्ति करायी। एक साथ पाँच-पाँच मौखिकी परीक्षाओं को पूल करके उन्हें शोध संगोष्ठी का रूप दिया। शोधार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य की गयी। प्रति सप्ताह शोध पत्र-वाचन का क्रम चला। उसी के अनुसार प्रगति-रिपोर्ट बनायी गयी। विभाग के यशस्वी शिक्षक और हिन्दी के प्रथम शोधोपाधि प्राप्त विद्वान डॉ. बड्थ्वाल के जन्म दिवस को ‘शोध दिवस‘ के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अंतर्गत शोध-प्रयोगशाला, शोध प्रदर्शनी, शोध पत्रिका और शोध संगोष्ठी की व्यवस्था की गयी। विभागीय शोध समिति के सहयोग से लगभग साढ़े तीन सौ स्वीकृत किन्तु अप्रकाशित शोध प्रबंधों का सार संक्षेप ‘शोध सर्वस्व‘ के नाम से प्रकाशित किया गया। बारह वर्षों के इस अभियान का सुफल मिला। एक योजना के अन्तर्गत अवध क्षेत्र के लगभग पाँच जिलों का साहित्यिक सर्वेक्षण विभागीय शोधार्थियों के साथ किया और सैकड़ों कवियों, लेखकों, लोक कलाओं, लोक नाट्यों, लोक गीतों का साथ ही भाषा बोली के विभिन्न रूपों का अनुसंधान करके पर्याप्त मौलिक तथा उपयोगी सामग्री जुटाई। इससे एक विश्वास जागा कि यदि शोध-समीक्षा से जुड़े हम शिक्षक संकल्पबद्ध हो जाएँ तो सरकारी अनुदान के बिना भी, स्वल्प साधनों के सहारे काफी कुछ शोधोद्धार कर सकते है। मेरा मत हैं कि शोध क्षेत्र में नए नियमन की जरूरत है। यदि हम विभिन्न मंचों से शुभेच्छा पूरित पुरजोर माँग करेगें तो जड़ व्यवस्था में भी न्यूनाधिक परिवर्तन होगा अवश्य।
लखनऊ से आपका भावात्मक नाता रहा है। यहाँ से विस्थापित होने पर आपको दारुण दर्द हुआ होगा। लौटकर आने पर फिर कैसा लगा?
लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, शोध कार्य करते हुए ‘हम फिदाए लखनऊ‘ वाला भाव हर समय दिलोदिमाग़ में रहता था। जब यहाँ से जोधपुर गया तो लखनऊ ज्यादा याद आया। कारण, लखनऊ में मेरी ननिहाल थी। बचपन से ही यहाँ आवागमन होता रहता था। यहाँ के साहित्यिक समाज से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला था। यहाँ की नफासत बहुत पसन्द थी। मेरे मूल स्थान (बन्नावाँ) की दूरी यहाँ से मात्र 50 किमी है, इसलिए आरंभ से ही लखनऊ में रच बस गया था, किन्तु रिसर्च के दौरान जब यथार्थ बोध हुआ और यह पता चला कि मुझसे वरिष्ठ दस बारह लोग कई वर्षों से तदर्थ छमाही नियुक्ति वाली प्रतीक्षा सूची में हैं और यह भी कि राजनीतिक हस्तक्षेप हद से ज्यादा है, तो मुझे लखनऊ छोड़कर मरुवास का निर्णय लेना पड़ा। चार पाँच वर्षों तक विज्ञापन का इंतजार करता रहा। आखिरकार शासन ने जब तदर्थ सेवा वाले, (प्रतीक्षा सूची वाले) शिक्षकों को एक अध्यादेश द्वारा स्थायी कर दिया तो नए चयन की संभावना समाप्त हो गयी। उन दिनों राजस्थान में कुछ अतिरिक्त भत्ते मिलते थे। दूसरे वहाँ अंधों में कानाराजा बन गया था। अस्तु, मन मानकर जोधपुर में ही बसने का संकल्प ले लिया। वहीं हाउसिंग बोर्ड से एक मकान ले लिया और लखनऊ के बारे में भूल गया। किन्तु 1976 में जब गुरुवर (विभागाध्यक्ष जी) का आदेश हुआ तो लखनवी मोह फिर जाग्रत हो गया। दैव योग से निर्विघ्न नियुक्ति हो गयी और मैंने यहीं रीडर के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। यहाँ विभाग में लगभग चैबीस वर्ष नौकरी की। अब रिटायर हुए बीस वर्ष हो गए हैं। बीच-बीच में कुछ बाहर के प्रलोभन दिखे, पर लखनऊ छोड़कर अन्यत्र जाने का मन नहीं हुआ।
लखनऊ विश्वविद्यालय में आपकी सक्रियता कई क्षेत्रों में रही है। अपने कार्य कलाप पर हुछ प्रकाश डालिए।
लखनऊ विश्वविद्यालय मेरी मात्र संस्था है। इसकी शरण में न आता तो मैं उच्चशिक्षा न प्राप्त कर पाता। इस संस्था से कई रूपों में मेरा जुड़ाव रहा। विद्यार्थी रूप में मैं कई परिषदों में सक्रिय रहा। शोधार्थी रूप में ‘रिर्सज स्कालर ऐसोशिएशन‘ का दो वर्षों तक अध्यक्ष रहा। शिक्षक रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में 1 वर्ष उपाध्यक्ष तथा एक वर्ष अध्यक्ष रहा। हिन्दी और पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष रूप में लगभग साढे बारह वर्षों तक अध्ययन मण्डल, विभागीय समिति, शोध समिति, फैकेल्टी बोर्ड, कार्यकरिणी, सीनेट, निर्माण विभाग, केन्द्रीय टैगोर पुस्तकालय, परीक्षा संचालन मूल्यांकन समिति, सांस्कृतिक समिति, त्रिकाल इन्फार्मेटिक्स (मीडिया सिंडीकेट), विश्वविद्यालय प्रकाशन आदि संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य किया। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष और गर्व है कि किसी स्तर पर मेरे साथ विद्यार्थियों, सहयोगियों, कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से कभी कोई अवांछनीय व्यवहार नहीं किया गया। मेरे विदाई समारोह में इस पर सुखद आश्चर्य प्रकट करते हुए तत्कालीन कुलपति जी ने कहा था कि यह विभाग का दीक्षित युग था। इस बीच हिन्दी विभाग की फाइल में दर्ज. आज तक कोई शिकायत या विवाद मुझे नहीं दिखा है। वस्तुतः मुझे मेरे पच्चीस वर्षों के शिक्षण कार्य काल में किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहा। विभागीय सदस्यों, शिक्षकों, शिष्यों और कर्मचारियों को समय समय पर समझाते हुए मैंने लगभग नब्बे प्रतिशत पाठ्यक्रम बदल दिया था। शोध विषय और निर्देशक मैंने अपने विवेकाधिकार के अनुसार तै किए। निष्कर्ष यह कि पूरे मन से और अवाध रूप से कार्य करने का अवसर यहां मिला।
सुना जाता है कि सरकारी अनुदान के बिना आपने संचार भवन का निर्माण अपने संसाधनों से, अपनी देख रेख में करवाया था। यह कैसे संभव हुआ?
पत्रकारिता का संचार भवन और हिन्दी विभाग के कई कमरे मैंने दिहाड़ी पर बनवाये हैं। सृजन पीठ और साहित्यिक वाटिका भी इसी प्रकार बनवायी है। इन वर्षों में लगभग तीन दर्जन विचार गोष्ठियाँ करवायीं। कभी किसी ने उँगली नहीं उठायी। मैं सबसे यहीं कहा करता था कि उत्तरप्रदेश सबसे बड़ा हिन्दी प्रदेश है और उसकी केन्द्रीय स्थली है राजधानी लखनऊ। इस विश्वविद्यालय का बड़ा गरिमा पूर्ण इतिहास रहा है। लखनऊ नगर में और अवध मण्डल में एक से एक महान कवि, कथाकार, नाटककार, भाषाविद्, समीक्षक और पत्रकार हुए हैं तथा आज भी हैं। उनकी गौरवमयी परंपरा को विकसित करना हम सबका कर्तव्य है। यह हमारी मातृ संस्था है। हम यहाँ अधिकारी न होकर मात्र हिन्दी सेवी होकर रहें। तब हमारे विभाग में भौतिक संसाधनों की बड़ी कमी थी। राज्य सरकार केवल वेतन जुटा देती थी। दस दस वर्षों तक भवन की रंगाई-पुताई और मरम्मत नहीं होती थी। फर्नीचर का अभाव हो गया था। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रकाशन, सेमीनार आदि की स्थिति दयनीय थी। शिक्षणेतर कर्मचारियों में अराजकता और विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता अपनी अति पर थी।
विद्वान प्रोफेसर यहाँ कुलपति होते डरते थे। छात्र नेता पिस्तौल लेकर चयन समिति में घुस जाते थे। दलाली का धंधा जोरों पर था। शासन लगभग निरुपाय था। भगवत कृपा से तभी प्रोफेसर महेन्द्र सोढ़ा जैसे कुलपति की नियुक्ति हुई। उन्होंने स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की योजना चलाई। मैं अपने विभाग में पहले से ही पत्रकारिता, अनुवाद, राजभाषा, मीडिया लेखन, सुगम हिन्दी, भाषा शिक्षण और सर्जनात्मक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निजी संसाधनों से चला रहा था। इस पहल को देखकर सोढ़ा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सभी विभागों को बुलाकर रोजगार परक कार्यक्रम चलाने हेतु प्रेरित किया। अपने विशेषाधिकार से सबको स्वीकृति दे दी और कार्यपालक नियम बनवा दिए। एक सत्र के भीतर पचासों कोर्सेज चल पड़े। फलतः प्रतिवर्ष करोड़ों की धनराशि विश्वविद्यालय को प्राप्त होने लगी। लोगों को यथेष्ट मानदेय मिलने लगा तो वे अतिरिक्त उत्साह के साथ इनके संचालन में जुट गए। कुछ अच्छे कर्मचारी भी मिल गए। फीस से अर्जित यह धनराशि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से कई गुना ज्यादा थी। इस धनराशि से चुनिंदा विशेषज्ञ बुलाये जाने लगे। प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का जीर्णोद्वार हुआ। पूरे परिसर का कम्प्यूटरीकरण हो गया। फर्नीचर, स्टेशनरी, वाहन और अन्य भौतिक संसाधन आवश्यकता के अनुरूप जुटा लिए गए। फलतः एक वर्ष के भीतर ही हमारे छात्रों का ‘प्लेसमेंट‘ होने लग गया। हमने एम.ए. अनुवाद का पूरे देश में प्रथम पाठ्यक्रम यहाँ चलाया। कई बैंकों के अधिकारियों ने कैम्पस इण्टरव्यू करके कई अनुवादकों की अग्रिम बुकिंग कर ली। पत्रकारिता में एम.ए. करने वाले हमारे कई विद्यार्थी विभिन्न चैनलों में पहुँच गए। कई छात्रों के जनसंपर्क अधिकारी का पद मिला। बहुतों ने राजभाषा प्रतियोगिता पास कर ली। कुछ विज्ञापन समितियों में चले गए। कुछ रेडियो टी.वी. के कैजुवल आर्टिस्ट हो गए। यानि बेरोजगारों की संख्या बहुत कम हो गयी। शुल्क से हमें जो राशि मिलती थी, उससे हम अतिथि शिक्षक बुलाते थे, दो तीन सेमिनार कराते थे, विभागीय शोध पत्रिका के प्रतिवर्ष तीन अंक निकालते थे, अपनी प्रयोगशाला चलाते थे, प्रवेश से लेकर परीक्षा तक का दायित्व स्वयं वहन करते थे और बीस प्रतिशत विश्वविद्यालय को देते थे। मैंने यह अनुभव किया कि जब साथी शिक्षकों को मान तथा मानधन मिलने लगता है, जब छात्र गंभीरता पूर्वक कैरियर निर्माण में जुट जाते हैं तो खाली दिमाग वाला शैतान न केवल निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ विकास में व्यस्त हो जाता है। उन दिनों हमारे सहयोगी दस बजे से छह बजे तक विभाग में कार्य करते थे। हर तरह का कार्य, चाहे वाटिका में क्यारी बनानी हो, या रंगमंच की तैयारी करनी हो। हम सबने तै किया कि यू.जी.सी. की नेट परीक्षा के लिए छात्रों को रोज दो घण्टे निःशुल्क कोचिंग दी जाये। इससे हमारे विद्यार्थियों को अभूतपूर्ण सफलता मिली। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को समझाते हुए मैंने उन्हें प्रेरित किया कि हम सब पर परीक्षा में नकल करने का लांछन लगाया जा रहा है। आइये, हम सब निरीक्षक रहित परीक्षा करके दिखायें। हमने प्रेस वालों को सूचित किया कि तीन घण्टे के भीतर वे कभी भी आकर देख सकते हैं। मैंने अनुभव किया कि ज्यादातर विद्यार्थी भावुक होते हैं। यदि किसी शिक्षक ने प्रभावित कर लिया तो छात्र आजीवन उसके प्रति श्रद्धालु तथा निष्ठावान बना रहता है। मैंने दो तीन बार ऐसा महसूस किया कि आयोजन के बीच चल रहे जलपान में अराजक तत्वों ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो विभाग के विद्यार्थी स्वतः प्रेरित आगे बढ़कर रक्षा पंक्ति में खड़े हो गए। मेरा अनुभव है कि शिक्षक में यदि शिष्य वत्सलता है, अध्यापन कौशल है, विद्वता है और उसका आचरण सर्वथा मर्यादित है तो आज भी विद्यार्थी उससे नजर मिलाकर बात नहीं कर पायेंगे। जो अव्यवस्था दिखती हैं, उसके दोषी हैं राजनीतिक दल, जिन्होंने शिक्षा संस्थाओं को दलीय राजनीति की नर्सरी बना रखा है। मैंने यह देखा है कि सहयोगियों और विद्यार्थियों का सहयोग मिल जाये तो साधनों के अभाव में भी बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग की सहायता से हम 14 सितंबर को हिन्दी दिवस पर विचार गोष्ठी करते थे और उसके बाद लगभग ढाई सौ विद्यार्थियों शिक्षकों का दल मुँह पर पट्टी बाँधकर और हाथों में हिन्दी प्रयोग की तख्ती लेकर पूरे परिसर की जो मौन परिक्रमा करता था, उसका हिन्दीकरण की दिशा में बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता था। हमने आयोजनों का एक बड़ा सस्ता फार्मूला बना रखा था। पाँच सौ रूपये में क्षेत्रीय संगोष्ठी और पाँच हजार में राष्ट्रीय संगोष्ठी। यह राशि हिन्दी विद्यार्थी परिषद् और शोध समिति के बच्चे प्रतिवर्ष चंदे के रूप में जुड़ा. लेते थे। हमने आयोजनों के एक बार बैनर बनवा लिए, एक बार निमंत्रण पत्र छपवा लिए, एक बार सजावटी फूल खरीद लिए, जो कई-कई वर्षों तक चले। विभाग में हमने पर्याप्त वाद्ययंत्र, कंप्यूटर, टी0वी0, रेडियो, माइक, लाइट इक्युपमेंट, कैमरा, वीडियो और छोटे बड़े बर्तनों का प्रबंध कर रखा था। कभी भी एक घण्टे में फटाफट मंच तैयार हो जाता था। लखनऊ नगर में समागत विद्वान वक्ताओं की कमी न थी। बाहरी विद्वानों को हमारे सहयोगी अपने वाहनों से ले आते थे। अपने घरों में रोक लेते थे। छात्रायें खुद चाय बना लेती थी। रंगोली और साज सज्जा कर लेती थीं। बच्चे थोक बाजार से खाद्य सामग्री ले आते थे। घर-घर निमंत्रण पात्र पहुँचा देते थे। पत्रकार शिष्य उसकी बढ़िया रिपोर्टिग कर डालते थे। भारतीय हिन्दी परिषद् का जो अधिवेशन 1989 में यहाँ हुआ था, उसे लोग आज भी एक नमूना मानते हैं। उसकी लागत थी मात्र दस हजार रूपये। लोगों ने इसे सेतुबन्ध कहा था। इसी प्रकार विभागीय, स्वर्ण जयंती, शोध और प्रकाशन की स्वर्ण जयंती, व्यावहारिक समीक्षा की राष्ट्रीय संगोष्ठी, पत्रकारिता भवन का लोकार्पण, स्टूडियो का उद्घाटन, हिन्दी प्रयोगशाला का उद्घाटन, त्रिकाल इंफार्मेटिक्स की स्थापना, तुलसी जन्मभूमि संगोष्ठी, आल्हा महोत्सव आदि अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कई कार्यशालायें, कई प्रशिक्षण शिविर और विचार गोष्ठियाँ समय≤ पर यहाँ सम्पन्न होती रहीं।
आज ज्यादातर विभाग अन्तः कलह ग्रस्त हैं। यू०पी० को राजनीति का गढ़ माना जाता है। फिर आप यह सौजन्य सौहार्द कैसे स्थापित कर पाए?
हमारे विभाग में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के पीछे दो मुख्य कारक रहे हैं। प्रथम, विभागाध्यक्ष के कत्र्तृव्याधिकारों का विकेन्द्रीकरण। मैंने यह अनुभव किया कि शैक्षिक प्रशासन अफसरशाही द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि विभाग के सभी शिक्षक, कोई उन्नीस, कोई बीस, यानि लगभग एक ही स्तर के हैं। सब अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ। कहीं-कहीं तो कनिष्ठ व्यक्ति अपने वरिष्ठ जनों की, तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित प्रतीत होता है। नौकरशाही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और विभाग प्रमुख आई.ए.एस. अधिकारी के बीच योग्यता का बड़ा अन्तर दिखाई देता है। दूसरे सरकारी अधिकारियों के पास ट्रांसफर करने, मुवत्तल करने, प्रमोट या डिमोट करने, नोटिस देने और चरित्र पंजिका में मनचाही इन्ट्री करने का अधिकार होता है। इसलिए अधीनस्थ कर्मचारी वरिष्ठ जनों से डरते भी हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालयी व्यवस्था में अध्यक्ष न किसी का ट्रांसफर कर सकता है, न मुवत्तली। किसी को ‘मेमो‘ देने तक की प्रथा यहाँ नहीं है। आज तक उपस्थिति रजिस्टर में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर तक नहीं किए। वर्षों से यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल कार्यकारिणी समिति कर सकती है, किन्तु कोई अध्यक्ष, डीन तथा कुलपति इस प्रक्रिया में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होता है और अपकृत्य करने वाले महारथी यहाँ के स्थायी निवासी यानि पुराने घाघ होते हैं। वे प्रायः सत्ता और छात्र शक्ति से जुड़े रहते हैं। मैंने यह अनुभव किया कि अपने सहयोगियों से सौहार्द पूर्ण ‘संबंध बनाने चाहिए और उन्हें प्रकारांतर से समझाया जाना चाहिए। मुझे जब-जब सूचना मिली कि अमुक शिक्षक आज कक्षा नहीं ले रहे हैं तो मैं किसी को कहे बिना उनकी कक्षा में जाकर पढ़ा आया। इसकी जानकारी होने पर वे मिले, कई बहाने यानि मौखिक स्पष्टीकरण देते हुए। मैंने बड़े शिष्ट तरीके से केवल यहीं समझाया कि कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। जब सहयोगियों ने यह देखा कि चाहे कोई जरूरी काम हो अथवा चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति कार्यालय में आ जाये, तो भी अध्यक्ष जी अपनी कक्षा नहीं छोड़ते हैं, तो इसका गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। इसके साथ-साथ यदि कक्षाध्यापन में कुछ नए-नए प्रयोग होते रहें, तो इस कार्य से कभी ऊब नहीं होती। मैंने सभी साथियों से यह अनुरोध किया कि कक्षा में समय से आयें-जायें, सही परिधान अपनायें, नोट्स न ‘डिक्टेट‘ करे, रोज नया टापिक घोषित करके, मंच पर खड़े होकर प्रभावशाली लेक्चर दें। नए-नए प्रयोग करते रहें। मैंने बहुत तरह के अडियो-वीडिया रिकार्ड एकत्र करा लिए थे। जिस रचनाकार पर बोलना होता था, उससे संबंधित ‘जरूरी दृश्य अथवा उसकी रिकार्डेड वायस प्रायः कक्षा में उपलब्ध करा दी जाती थी। इससे शिक्षक-शिक्षार्थी दोनों को नयी स्फूर्ति मिलती रही। वहां जो वाद विवाद-संवाद होता था, उससे विषय का स्तर उठता चला गया।
शिक्षकों में सौहार्द भाव भरने के ध्येय से मैंने टाइम टेबल में तीस मिनट का टी-ब्रेक रखवा दिया। बंद कमरे में चपरासी चाय व कुछ नाश्ता रख देता था और लोग किसी भेद भाव के बिना परस्पर हँसी मजाक करते हुए चाय पीते थे। इस अनौपचारिक वार्तालाप के बीच ही मैं सबको जरूरी सूचनाएँ दे देता था और विभागीय निर्णय से अनौपचारिक ढंग से अवगत करा देता था। इस टी ब्रेक से स्वतः यह सूचना मिल जाती थी कि कौन कौन आज छुट्टी पर हैं।
परस्पर सद्भाव पूर्वक अपील करते हुए मुझे इस कार्य में एक सफलता यह मिली कि निर्देशक स्वयं पूरी थीसिस पढ़ने के बाद ही उसे जमा कराने की अनुमति देते थे। हमारे शोध-मण्डल में सात सदस्य होते थे। मैं विशेष आमंत्रित के रूप में निर्देशक को भी बुला लेता था और सबसे गोपनीय ढंग से एक एक नाम ले लेता था, इन शर्तों के साथ कि प्रस्तावित परीक्षक प्रोफेसर पद पर हो, विषय विशेषज्ञ हो, उस सत्र में पहले कभी न आया हो, वह अतिवृद्ध न हो और अच्छी छवि वाला हो। मैं अपना कोई नाम स्वंय नहीं देता था, यह सोचकर कि जो आयेंगे वे अपने ही होंगे। जब पाँच रिपोर्ट आ जाती थीं, तो उन्हें पूल करके वाइवा के बहाने एक शोध संगोष्ठी का आयोजन हो जाता था। मौखिकी के दिन शोधार्थी के साथ रेस्टोरेंट जाने या उसकी दावत खाने का सख्त निषेध था। अन्य परीक्षाओं के संबंध में भी पहले से ही काफी शुचिता हमारे विभाग में निभायी जाती थी। यदा कदा पोजीशन को लेकर राग-द्वेष दिख जाता था। एम0ए0 मौखिकी में पारदर्शिता लाने के ध्येय से मैंने विभाग में रिहर्सल कराना शुरू किया, ताकि विद्यार्थी यह जान सके कि वाइवा में कैसी तैयारी की जानी चाहिए। इस आंतरिक मूल्यांकन से यह भी पता चल जाता है कि सर्वश्रेष्ठ पोजीशन वाले परीक्षार्थी कौन हैं? वाइवा के पहले विद्यार्थियों को बुलाकर मैं उन्हें प्रशिक्षण देता था और जोर देकर कहता था यदि किसी ने किसी छात्र नेता के जरिये सिफारिश करवायी तो उसका अर्थ होगा कि वह व्यवस्था में साधक नहीं, बल्कि बाधक है। मैंने स्वयं इतने वर्षों में किसी परीक्षक को किसी प्रकार का संकेत नहीं दिया। प्रथम-द्वितीय स्थान वाले परीक्षार्थियों को मैं दो दो बार वाइवा के लिए बुलाया करता था। मुझे जहाँ संदेह हुआ, उनके द्वारा बनाये गए प्रश्न पत्र को मैंने इतना माडरेट कर दिया कि ‘गेस क्वेश्चन‘ की प्रथा कुछ दिनों में समाप्त हो गयी। इसकी कीमत भी मुझे कभी-कभी चुकानी पड़ी। एक बार मेरी विभागाध्यक्ष की पुत्री एम.ए. हिन्दी परीक्षा में बैठी तो द्वितीय वरिष्ठ होने के नाते मुझे ही परीक्षा कार्य का संचालन करना पड़ा। उस परीक्षार्थी ने मुझे अधीनस्थ समझकर मुझ पर हर तरह से दबाव डाला यानी पेपर आउट कराना चाहा। वाइवा में हद से ज्यादा नंबर पाना चाहा, किन्तु वस्तुनिष्ठ परीक्षण-प्रक्रिया अपनाने के कारण वह केवल दूसरा स्थान प्राप्त कर सकी। कोप भाजन होने के कारण मुझे कुछ कीमत चुकानी पड़ी, पर लोगों के लिए यह एक दृष्टांत बना गया।
विभागीय सौमनस्य के लिए मैंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। तब अध्यक्ष पद स्थायी होता था। मैंने महसूस किया कि विभाग में अध्यक्ष के बाद प्रायः बाबू (विभागीय क्लर्क) को महत्व दिया जाता है और सेकेण्ड मैन तक को प्रतिपक्षी सन्दिग्ध या पराया माना जाता है। महत्व न पाने से तब या तो लोग विरोधी हो जाते हैं या उदासीन। संप्रति अधिकतर लोग सत्ता और अर्थ प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। अस्तु उन्हें अपने संग जोड़े रखने के उद्देश्य से मैंने विभागीय इकाइयों का विकेन्द्रीकरण कर दिया। विभाग के पन्द्रह वरिष्ठ जनों को शोधकार्य, सेमिनार, समय सरिणी, विभागीय प्रकाशन, शोध पत्रिका, एम.ए. अनुवाद, एम.ए. पत्रकारिता, एम.ए. प्रयोजनी हिन्दी, प्रयोगशाला, लोक साहित्य, रंगमंच, विद्यार्थी परिषद और पाठ्य पुस्तक निर्माण योजना का प्रभारी बना दिया। सबके पृथक् कार्यालय, सबके साथ शोध सहायक और सबके निजी बैंक खाते। इस व्यवस्था ने उन सभी लोगों का व्यवहार बदल दिया, जो स्वभावतः प्रभादी थे। इन इकाइयों के बीच शुद्ध स्पर्धा चल पड़ी। उन्हें लगा, जीवन में पहली बार ऐसी पद-प्रतिष्ठा मिली है। इससे अध्यक्षीय अधिकारों में कोई कटौती नहीं हुयी, बल्कि उसका प्रभामण्डल बढ़ गया। कुलपतियों को जब दिखा कि इनके साथ पच्चीस शिक्षक और पचास सक्रिय शोधार्थी हैं और सब उनके अनुकूल हैं तो उन्होंने शक्ति केन्द्र के रूप में विभाग को मान्यता दी। हमारे किसी प्रस्ताव को किसी कुलपति ने शायद ही कभी अस्वीकार किया हो।
आपने प्रयोजन मूलक हिन्दी की शुरुआत की। अब उसकी स्थिति क्या है?
मुझे एक चिन्ता बहुत दिनों से सता रही थी कि अच्छे विद्यार्थी हिन्दी की ओर न आकर अर्थशास्त्र, ऐन्थ्रो, अंग्रेजी आदि विषयों की ओर क्यों चले जाते हैं? तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष निकला कि संप्रति विद्यार्थियों की प्राथमिकता है रोजगार। यह रोजगार उन विषयों में ज्यादा दिखाई देता है। दूसरे, जो विषय सिविल परीक्षाओं में ज्यादा लोकप्रिय हैं, उधर विद्यार्थी खिंचे चले जाते हैं। इस स्थिति से प्रेरित होकर प्रयोजन मूलक हिन्दी पाठ्यक्रम लागू करने का संकल्प लिया गया। इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम की शुरूआत 1977 में हो गयी थी। तब हमारे विभागाध्यक्ष थे पं. हरिकृष्ण अवस्थी जी। एक दिन उनके पास केन्द्र सरकार के शिक्षा सचिव जी का एक परिपत्र आया जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव था। पंडित जी हिन्दी को रोजगार का विषय बनाने से सहमत नहीं थे। हिन्दी में रोजगार की कहाँ कैसी संभावना है, इस पर भी उस पीढ़ी ने तब तक विचार नहीं किया था। अस्तु, यह समस्या उन्होंने मुझे सौंप दी। मैं सांसद श्री सत्यनारायण मोटूरि जी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए ‘फंक्सनल‘ हिन्दी पाठ्यक्रम और उस पर हुई बहस से अवगत था। उसका निचोड़ मैंने पंडित जी के समक्ष रखा, तो वे न केवल ‘सहमत हुए, बल्कि उसे तत्काल लागू करने के लिए समुद्यत हो गए। दो दिन बाद पाठ्यक्रम समिति और फैकल्टी बोर्ड की बैठकें होनी थीं। गुरुवर ने आदेश दिया कि एक अच्छी प्रस्तावना के साथ चार प्रश्न पत्रों और संदर्भ ग्रंथों का पूरा प्रारूप एक वैकल्पिक वर्ग के रूप में तैयार करके दो, तो मैं इन समितियों में रखू। मैंने पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें पत्रकारिता, अनुवाद, रंगमंच तथा राजभाषा के चार थ्योरी पेपर और एक प्रायोगिक तथा मौखिकी का प्रश्न पत्र प्रस्तावित किया गया था। पंडित जी के प्रभाव से यह पाठ्यक्रम यथावत् पारित हो गया। तब तक नए विषयों की जानकारी सर्वसामान्य शिक्षकों को नहीं थी। उन्होंने आदेश दिया कि हर प्रश्न पत्र में आधा प्रश्न पत्र तुम पढ़ाओ और आधे के लिए किसी सहयोगी को तैयार कर लो। इस वैकल्पिक वर्ग को नाम दिया गया एम.ए. स्पेशल। श्रेणी सुधार के उद्देश्य से इसमें विद्यार्थियों की काफी भीड़ भर गयी। इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर विभागाध्यक्ष बनते ही मैंने एम.ए. पत्रकारिता और एम.ए. अनुवाद के द्विवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, स्ववित्त पोषित नीति के अंतर्गत लगभग बारह वर्षों तक चलाये। प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का डिप्लोमा पाठ्यक्रम तो था, पी.जी. पाठ्यक्रम सर्वप्रथम हमारा था। इसमें पीएच.डी., डीलिट तक की व्यवस्था थी। आठ विद्यार्थियों से शुरू किया गया यह विषय कुछ ही वर्षों में बी.ए., एम.ए. तथा रिसर्च में अनुमन्य हो गया। चूंकि एम.ए. करते करते प्रशिक्षुओं को अच्छे से अच्छे अखबारों और चैनलों में नौकरी मिलने लगी, इसलिए इन पाठ्यक्रमों की ओर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुलपति के माध्यम से मंत्रियों और अधिकारियों की सिफारिसें आने लगीं। इस बीच पत्रकारिता एवं जनसंचार का स्वतंत्र विभाग बन गया था, उसका अपना भवन बन गया था। एक वातानुकूलित स्टूडियो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था हो गयी थी। सिटी रेडियो का केन्द्र खुल गया था। एक फीचर सिंडिकेट स्थापित हो गया था। डाक्यूमेन्ट्री फिल्में बनने लगी थीं। इसलिए इस विभाग की चर्चा दूर-दूर तक होने लग गयी थी। मैंने प्रवेश परीक्षा आदि में पूरी शुचिता का पालन किया-कराया, जिससे इसकी साख बढ़ती चली गयी। इस विभाग में ‘त्रैमासिक संचार श्री‘ नाम की शोध प्रत्रिका और परिसर से संबंधित एक पाक्षिक प्रशिक्षण पत्रिका शुरू हुई। कई कार्यशालायें और राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित हुयीं। जन सम्पर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया लेखन आदि के कई कार्यक्रम चले, जिससे जन जन में यह विश्वास घनीभूत हो गया कि पत्रकारिता-अनुवाद एवं मीडिया लेखन नितांत रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम हैं। इसी का एक स्वतंत्र संस्करण ‘साहित्यिक पत्रकारिता‘ नामक एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम मैने एम.ए. हिन्दी साहित्य के एक वैकल्पिक वर्ग में रखा।
मेरी जानकारी में अनुवाद का द्विवर्षीय एम.ए. पाठ्यक्रम सबसे पहले आपने शुरू किया था। इसकी परिकल्पना कहां से मिली?
अनुवाद तो विश्व ज्ञान का गवाक्ष है। विश्वमानव को परस्पर जोड़ने, उन्हें अधिकाधिक सूचनाएँ देने का बहुत बड़ा माध्यम है यह। अस्तु, द्विवर्षीय एम0ए0 अनुवाद का पाठ्यक्रम 1990 से यहाँ शुरू किया गया। इसके अंतर्गत वेटिंग, डबिंग, इन्टरप्रिटिंग, सार लेखन, पारिभाषिक शब्दावली, संक्षिप्ताक्षर निर्माण, मशीनी अनुवाद, संपादन, रूपांतरण, आदि कई पक्षों का समावेश किया गया। इस प्रशिक्षण में नगर के वरिष्ट अनुवादकों एवं राजभाषा अधिकारियों ने बड़ा सहयोग किया। इसकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ी कि दो वर्ष बाद इसमें कैम्पस इण्टरव्यू होने लगे। हमारे इस पाठ्यक्रम से प्रेरित होकर यू.जी.सी. ने इसे अपनी प्राथमिकता सूची में स्थान दे दिया।
आपने कई रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए थे। उस दिशा में कैसी सफलता मिली?
प्रयोजन मूलक हिन्दी के अंतर्गत पहले सत्यनारायण जी ने केवल अनुवाद और पत्रकारिता की पहल की थी। हमने इसके बारह नए रूप बनाये-
- रंगमंच, इसके अंतर्गत रंग आलेख तथा संवाद लेखन का प्रावधान किया गया। इसे विज्ञापन तथा समाज
- सुधार परक नुक्कड़ नाट्य से जोड़ा गया।
- माध्यम लेखन-इसके अंतर्गत रेडियो, टी.वी. की कई नयी विधाओं का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जैसे रेडियो वार्ता, फीचर, रिपोर्ताज, संस्मरण, परिचर्चा, समीक्षा, स्तम्भ लेखन, समाचार लेखन, शीर्षकीकरण, व्यंग्य लेखन, टेली फिल्म, टेली ड्रामा, डाक्यूड्रामा, पटकथा लेखन और सोशल मीडिया।
- प्रचार साहित्य- जैसे नारा (स्लोगन) लेखन, सूक्ति, विज्ञप्ति, पैंफ्लेट, ब्रोस्योर, स्टीकर, बैनर, पोस्टर, विभागीय मुख पत्रिका का संपादन, जनसंपर्क कार्यालय का संचालन आदि ।
- राजभाषाः- अर्थात् टिप्पण, प्रारूपण, पत्राचार, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालयी हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी कम्प्यूटिंग आदि।
- सर्जनात्मक प्रशिक्षण अर्थात् काव्य रचना, कथा लेखन, रंग आलेख, चरितात्मक लेखन (जीवनी, रेखाचित्र), सैटायर, ललित निबंध आत्म संस्मरण, आत्मकथा, समीक्षा प्रविधि, शोध प्रौद्योगिकी, आदि।
- ज्ञान विज्ञान लेखन अर्थात् छात्रोपयोगी संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश और स्फुट पाठ्य सामग्री का निर्माण।
- कोशकारिता अर्थात् पर्यायवाची कोश, शब्दकोश, पात्र कोश, काव्यकोश, उद्धरण कोश, विचार कोश, चरित कोश, संदर्भ कोश आदि की रचना प्रक्रिया।
- संभाषण कला, इसके अंतर्गत वाचिक कला (वाक् कला) अर्थात् कमेंट्री, उद्घोषणा, कम्पेयरिंग और अभिभाषण कला का प्रशिक्षण।
- लोक वांग्मय- अर्थात् एक क्षेत्र विशेष और विभाषा विशेष के लोक गीतों, लोक गाथाओं, लोक कथाओं, लोक नाट्यों, लोकोक्तियों, अभिप्रायों और कथानक रूढ़ियों का संकलन संपादन तथा विश्लेषण।
- भाषा शिक्षण-अर्थात् मानक हिन्दी, जनपदीय बोलियाँ, अहिन्दी भाषियों विदेशियों के लिए सुगम (स्पोकेन) हिन्दी, सही वर्तनी, लिपि, उच्चारण और व्याकरण का प्रशिक्षण।
- हिन्दी कम्प्यूटिंग, अतंर्जाल प्रशिक्षण- हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान, कोचिंग लिखित-मौखिक भाषा का प्रायोगिक प्रशिक्षण, टंकण, सुलेख, आशु लेखन, प्रूफ पठन आदि।
- पाठालोचन- लिपि विज्ञान, पाठ संपादन आदि।
अनुदान के बिना ये पाठ्यक्रम कैसे चल पाए? इसका कोई फार्मूला हो तो कृपया बताएँ?
हमें कोई अनुदान नहीं मिला था। मैंने माँगा भी नहीं। शुल्क रखा गया न्यूनतम 800 वार्षिक। बस मन में दृढ़ संकल्प था कि यदि इन विषयों के सैद्धांतिक-प्रायोगिक अध्ययन-अध्यापन द्वारा विद्यार्थियों को निष्णात कर दिया जायेगा तो जीविकोपार्जन की इतनी उग्र समस्या नहीं रह जाएगी। कठिनाई यह थी कि इन विषयों में हिन्दी में पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं। मैंने भरसक पाठ्य सामग्री एकत्र करके और वरिष्ठ जनों के व्यावहारिक स्वानुभव का उपयोग करते हुए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया। नयी पीढ़ी में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुक्त संवाद के माध्यम से उनके चिंतन में धार धरी जा सकती है। समस्या केवल यथास्थितिवाद से मुक्ति की है। चूंकि विश्वविद्यालय में राजभाषा प्रशिक्षण नामक स्ववित्त पोषित दक्षता पाठ्यक्रम की शुरूआत हिन्दी विभाग ने की थी, इसलिए सबसे अधिक विवाद हमें झेलना पड़ा। तब कई विभागाध्यक्षों ने यह तर्क दिया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का संबंध महत्तर मूल्यों से है, न कि बाजार मूल्य या कि रोजगार से। बहुत समझाने पर, मुख्यतः तत्कालीन कुलपति के सहयोग से कुछ संशोधनों के साथ हमारा पाठ्यक्रम पारित हो पाया था। इसकी देखा-देखी रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की बाढ़ आ गयी। जो विभाग इस नीति से नहीं जुड़े वे, पीछे चले गए। आज का कटु सत्य यह है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम हटा दिए जायें तो राज्य विश्वविद्यालयों का वित्तीय ढाँचा चरमरा जाये। अब तो केन्द्र और राज्य का समूचा शिक्षा तंत्र विश्वविद्यालयों पर यह दबाव डाल रहा है कि अधिकाधिक रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम चलाये जायें। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ कि शुरू में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली को दो बार मैंने आवेदन भिजवाये, इन रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए तो वहाँ आचार्य द्वय (डॉ. नगेन्द्र और डॉ. नामवर) के हस्तक्षेप के कारण वे अस्वीकृत हो गए। लगभग एक दशक के बाद इन दोनों को मैंने यह कहते हुए सुना कि “दीक्षित तुम ठीक थे। कैरियर से जोड़े बिना हिन्दी नहीं चल पाएगी।‘‘ आज इस प्रयोजन मूलक हिन्दी के एम.ए. पाठ्यक्रम लगभग सत्तर विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं।
मेरी जानकारी में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी आपके सदुद्योग से निर्मित हुआ था? यह कैसे संभव हुआ?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हिन्दी के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण हेतु एक कमेटी गठित की थी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिन्दी विभागाध्यक्ष उसके संयोजक थे। मेरे साथ डॉ. तारकनाथ बाली, डॉ. अरविन्दाक्षण, डॉ. जयप्रकाश तथा डॉ. रमेश गौतम उसके सदस्य थे। इसके तीन वर्ष पूर्व डॉ. शिवप्रसाद सिंह के संयोजन में एक समिति बी.एच.यू. में बनायी गयी थी। उसकी कई बैठकें दो वर्षों में हुयीं, किन्तु कोई सहमति नहीं बन पायी। अंततः उनके द्वारा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया, उसे लागू करने के लिए अधिकतर विश्वविद्यालय तैयार नहीं हुए। मैंने यह अनुभव किया कि सही पाठ्यक्रम के निर्धारण में ये पाँच बाधक तत्व हैं-
- दलीय विचारधारा अर्थात् पाठ्यक्रम को लाल पीले रंग से रंगने का दुराग्रह।
- प्रकाशक से प्राप्य रॉयल्टी, उत्कोच यानी आर्थिक प्रलोभन।
- क्षेत्रीयता का दुराग्रह जैसे कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में हर प्रश्न पत्र में राजस्थानी रचनाकारों को स्थान दिया जाये, बिहार में अधिकतर बिहारी पढ़ाये जायें और इसी प्रकार विभिन्न बोलियों के तथा अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी रचनाकारों का कोटा अनिवार्यतः आरक्षित किया जाये।
- जातीय, सांप्रदायिक और लिंगीय संकीर्णता, जैसे दलित साहित्य, स्त्री विमर्श, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग आदि को प्रश्रय देने का दुराग्रह।
- रुचि विपर्यय, जैसे किसी को सूर-तुलसी पसन्द नहीं, किसी को अज्ञेय-मुक्तिबोध पसन्द नहीं। मैं जब
जोधपुर विश्वविद्यालय पहुँचा (1963 में) तब वहाँ आधुनिक कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, मैथिलीशरण का नाम नहीं था। केवल रत्नाकर और ब्रजभाषा के आधुनिक कवियों को स्थान दिया गया था। कुछ अर्से बाद दूसरे विभागाध्यक्ष आए, वे छायावाद के पोषक थे, किन्तु अज्ञेय, मुक्तिबोध आदि को पाठ्यक्रम में रखने को तैयार नहीं हुए। पाँच वर्ष बाद जो तीसरे विभागाध्यक्ष आए, वे प्रगतिवाद एवं नयी कविता के प्रतिमान बनाने में लगे रहे। इस प्रकार का असंतुलन पूरे हिन्दी जगत में विद्यमान दिखा। मैंने इस समिति के माध्यम से एकरूपता लाने का प्रयास किया। तदर्थ सबसे पहले. पाठ्यक्रम के दर्शन पर विचार हुआ। सबने यह स्वीकार किया कि पाठ्यक्रम के ये पाँच ध्येय होने चाहिए
- विगत लगभग 1500 वर्षों के हिन्दी भाषा-साहित्य की प्रवृत्तियों और प्रतिभाओं का संज्ञान विद्यार्थी को हो जाये।
- ऐसा पाठ्यक्रम बने जो नयी पीढ़ी में मानुष भाव का संचार करे।
- हिन्दी भारत की संपर्क भाषा है, इसलिए उसका मुख्य दायित्व है कि साहित्य द्वारा राष्ट्रीय भावैक्य का विकास करे।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम का धर्म है कि वह जीविकोपार्जन में सहायक हो।
- जैसे मेडिकल की शिक्षा लेकर विद्यार्थी चिकित्सक बन जाते हैं, उसी तरह साहित्य की शिक्षा पाकर वह साहित्य का पारखी और सर्जक बन जाए, यानी व्यावहारिक समीक्षा सिखायी जाये।
इस पंच सूत्री लक्ष्य को केन्द्र में रखकर यह निश्चय किया गया कि इन आठ विषयों को ‘कोर कोर्स‘ में रखा जाये और इस व्यवस्था का अनुपालन न करने वाले विश्वविद्यालय के हिन्दी पाठ्यक्रम को यू.जी.सी. की मान्यता न मिले-(1) भाषाशास्त्र (2) प्राचीन काव्य (3) आधुनिक काव्य (4) हिन्दी भाषा साहित्य का इतिहास (5) साहित्य सिद्धांत/हिन्दी काव्यशास्त्र (6) हिन्दी गद्य साहित्य (7) प्रयोजन मूलक हिन्दी (8) तुलनात्मक भारतीय साहित्य।
यह निश्चय किया गया कि स्थानीय उपयोगिता के आधार पर निम्नलिखित विषयों में से बीस प्रतिशत पाठ्यक्रम हर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्मित कर सकता है-(1) जनपदीय विभाषा (2) लोक वांग्मय (3) व्यावहारिक समीक्षा (4) नाटक रंगमंच (5) विशेष कवि लेखक (6) निबंध/लघु प्रबंध लेखन।
यह भी संस्तुत किया गया कि निम्नलिखित कवियों, लेखकों का अध्ययन अलग अलग प्रश्न पत्रों में अवश्य कराया जाये-कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, देव, बिहारी, घनानन्द, भारतेन्दु, महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रेमचन्द , जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, नागर, फणीश्वनाथ रेणु, मोहन राकेश, रामचन्द्र शुक्ल, नन्द दुलारे बाजपेयी, नगेन्द्र, रामविलास शर्मा। इनके अतिरिक्त इतिहास में अल्प चर्चित रचनाकारों को द्रुत पाठ के अंतर्गत स्थान दिया जाये। द्रुतपाठ में व्याख्यायें न पूछी जायें। किसी भी प्रश्न पत्र में व्याख्यांश 25 प्रतिशत से अधिक न हो। समीक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाये। हर प्रश्न पत्र में निर्धारित कवियों-लेखकों के पाठ्यांश (टेक्स्ट) का निश्चय यथोचित ढंग से विभागीय अध्ययन मण्डल करे। सुलभ संदर्भ ग्रंथों का निर्धारण करना भी उसी का दायित्व है। इस समिति ने आग्रह किया कि कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, सूरसागर, रामचरित मानस/विनय पत्रिका/कवितावली, भारतेन्दु कृत नाटक, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, उर्वशी, गोदान, चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, वाणभट्ट की आत्मकथा, आषाढ़ का एक दिन, चिंतामणि आदि के श्रेष्ठ पाठ्यांशों को स्थान अवश्य दिया जाये। इनके संकलन चाहे विभाग तैयार कराये या इस सामग्री से ओत प्रोत बने बनाए संकलन विभाग स्वयं तै करें। समीक्षात्मक प्रश्न साठ प्रतिशत हों और द्रुत पाठ से संबंधित टिप्पणियाँ पन्द्रह प्रतिशत हों। इन मुद्दों को लेकर तीन दिन बहुत खुलकर बहस हुई। अंत में सभी मित्रों ने मेरे इस ‘लखनऊ माडल‘ पर सहमति व्यक्त करते हुए मुझे अधिकृत कर दिया कि मैं इसका प्रारूप बना डालूँ। यह बड़े सुखद आश्चर्य का विषय है कि इस प्रारूप को लेकर हिन्दी जगत ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करायी। सेमेस्टर पद्धति आने के बाद इसके कई नए माड्यूल बनाए गए परंतु मूलभूत ढाँचा वही है। इसमें मेरा श्रेय नहीं है। यह सब सहसदस्यों के सहयोग सद्भाव का सुफल है।
शोध प्रशिक्षण के लिए अपने लखनऊ एमफिल पाठ्यक्रम की, जो पहल की, उसकी मूलभूत अवधारणा क्या थी?
लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने सबसे हिन्दी एम.फिल. पाठ्यक्रम चलाया। इसमें पहली बार देशांतरी हिन्दी (विश्व हिन्दी), आकर भाषा (अपभ्रंश, पुरानी हिन्दी), हिन्दीतर राज्यों का हिन्दी साहित्य, शोध प्रविधि, पाठालोचन जैसे विषय रखे गए। राष्ट्रीय भावैक्य की दृष्टि से तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला, मराठी, गुजराती, तथा पंजाबी के दक्षता, डिप्लोमा और तुलनात्मक अध्ययन के पाठ्यक्रम चलाये गए। तुलनात्मक शोध पर ज्यादा जोर दिया गया। जनपदीय अवधी भाषा और लोक साहित्य को वरीयता दी गयी और भाषा शिक्षण (मानकीकरण) के लिए ‘‘लैंग्वेज लैब‘ की स्थापना की गयी। सर्जनात्मक लेखन में हमारे नगर के रचनाकारों ने काफी सहयोग दिया। रंगमंच के विद्यार्थियों ने नाट्य मंचन करते हुए रंग कर्म की प्रैक्टिकल परीक्षा दी। पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने भित्ति पत्रिका बनाकर प्रायोगिक संपादन कार्य सीखा हिन्दी अधिकारियों के साथ राजभाषा प्रशिक्षुओं ने अनुवाद और कार्यालयी पद्धति सीखा, पुरातत्व केन्द्रों में जाकर छात्रों ने पाठालोचान सीखा और अपनी प्रयोगशाला में सबने संभाषण, उच्चारण वाचन कला तथा लोक धुनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह समन्वितः पाठ्यक्रम लगभग बारह वर्षों तक चला। जहाँ जहाँ मेरा उपाय चला, मैंने इसे लागू कराया। यदा कदा उत्तराधिकारियों ने असुविधा का तर्क देकर भले ही कुछ फेरबदल कर लिया हो, यों इस सर्वसमावेशी पाठ्यक्रम को व्यापक समर्थन मिला है।
पाठ्यक्रम कितना ही अच्छा हो, यदि पठन पाठन अच्छा न हुआ तो सब व्यर्थ हो सकता है। अपने इस दिशा में क्या किया?
साहित्य की अध्यापन पद्धति में यथासमय कुछ नए-नए प्रयोग मैंने किए। मुझे महसूस हुआ कि मंच पर खड़े होकर किताब बाचने वाली पद्धति से विद्यार्थी ऊब गए हैं और दूसरे बैठे-बैठे नोट्स डिक्टेट करना उच्चतर कक्षाओं में शोभनीय नहीं है। श्रव्य दृश्य माध्यमों के द्वारा विद्यार्थीपीढ़ी को आकृष्ट करने की जरूरत है और सार्थक संवाद की जरूरत है। इसके लिए पहली जरूरत यह है कि पाठ्यांश कम किया जाये। प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण कृति के टीका-भाष्य लिखे जा चुके हैं। उनके सहारे जो जिस पाठ का जब चाहे, अर्थ समझ सकता है। हमें चाहिए कि कक्षा में हम इन कवि-लेखकों के वस्तु-शिल्प पक्ष का तथा उनके समग्र प्रदेय का आकलन करें और उस आकलन प्रणाली से विद्यार्थियों को अवगत करायें। अभी तक जो पद्धति प्रचलन में है, उसमें वर्ष पर्यन्त संदर्भ प्रसंग सहित मात्र व्याख्यायें समझायी जाती हैं। टेक्स्ट समाप्त हो जाने का अर्थ है पाठ्यक्रम समाप्त। हमने प्रत्येक प्रश्न पत्र में पन्द्रह से बीस तक टापिक तै किए और उन पर व्याख्यान कराकर फिर वाद विवाद संवाद कराया। लेक्चर में एकरसता न आने पाए, इस ध्येय से उस कवि-लेखक से संबंधित चित्रावली, हस्तलेख, रिकार्डेड वाॅयस आदि दिखाए-सुनाए। इससे नयी रुचि पैदा हुई, विचारोत्तेजना पैदा हुई और बेहतर जानकारी मिली। विद्यार्थियों ने भित्ति पत्रिका में अपने उद्गार प्रकट किए। शनिवारीय गोष्ठी में सबने बारी-बारी से अपने-अपने आलेख पढ़े और विचार गोष्ठियों में भरसक सहभागिता की। श्रव्य-दृश्य सामग्री के संचय हेतु पुरानी पत्रिकाओं को खंगाला गया।
आकाशवाणी-दूरदर्शन और अखबारों से काफी सहायता मिली। इस नगर से इंशा अल्लाखां, मिश्रबन्धु, महादेवी वर्मा, निराला, प्रेमचन्द, आचार्य नरेन्द्रदेव, बदरीनाथ भट्ट, नन्ददुलारे बाजपेयी, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवतीचरण वर्मा, पढ़ीस, बंशीधर शुक्ल, रघुवीर सहाय, रमईकाका, कुंवर नारायण आदि काफी जुड़े रहे हैं। अतः उनकी सामग्री विशेष रूप से संजोयी गयी।
आपने अपने विभाग में लखनऊ प्रकोष्ठ की स्थापना की थी। इसके पीछे क्या प्रयोजन था।
प्रत्येक विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वह स्थानीय संपदा को भरसक उजागर करे। मैंने विभाग में इस प्रकोष्ठ की स्थापना करके यहाँ से जुड़े कई साहित्यकारों के संग्रह एकत्र किए। तब तक कम लोगों को ज्ञात था कि लखनऊ के मिश्र बन्धुओं का कितना बड़ा योगदान रहा है? पढ़ीस, वंशीधर, रमई काका का काव्य किस कोटि का है? हमारे विभाग का यह सौभाग्य रहा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रो0 अय्यर, जो केरल के निवासी थे और संस्कृत के विशिष्ट विद्वान थे। तब हिन्दी और संस्कृत का संयुक्त विभाग . हुआ करता था। हिन्दी इकाई के प्रभारी (अध्यक्ष) थे द्विवेदीयुगीन प्रसिद्ध नाटककार गुजरात के निवासी पं. बदरीनाथ भट्ट। उनकी स्मृति में यहाँ नाटय प्रशिक्षण योजना शुरू की गयी।
स्वतंत्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष और समूचे हिन्दी जगत के कालक्रम से द्वितीय वरिष्ठ प्रोफेसर हुए डॉ. दीनदयालु गुप्त। गुप्त जी ने ब्रज क्षेत्र में कई वर्षों तक घूम-घूमकर ‘अष्टछाप तथ्य बल्लभ सम्प्रदाय‘ की जो खोज की थी, उसका ऐतिहासिक महत्व है। उनके कई सहयोगी शिक्षक हिन्दी क्षेत्र में गण्यमान रहे हैं। डॉ. केसरी नारायण शुक्ल आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अन्तेवासी थे। ‘आधुनिक काव्यधारा‘ पर उन्होंने अपनी जो थीसिस लिखी थी, उसे पहल का श्रेय प्राप्त हुआ था। डॉ. शुक्ल ने लंदन एवं मास्को विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ायी थी। यहाँ कई वर्षों तक व विभागाध्यक्ष और कला संकायाध्यक्ष रहे। डॉ. भगीरथ मिश्र काव्यशास्त्र और मध्यकालीन काव्य के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्हें हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास निर्मित करने का श्रेय प्राप्त है। पं. हरिकृष्ण अवस्थी राजनीति में व्यस्त हो गए, अन्यथा तुलसी साहित्य पर उनको असाधारण अधिकार प्राप्त था। डॉ. सरयूप्रसाद अग्रवाल ने अकबरी दरबार के कवियों पर अच्छा कार्य किया था। डॉ. त्रिलोकीनारायण दीक्षित ने कई संत कवियों को नए सिरे से प्रतिष्ठित किया था। डॉ. विपिन बिहारी त्रिवेदी परवर्ती अपभ्रंश तथा रासो साहित्य के विद्वान थे। डॉ. हीरालाल दीक्षित ने केशवदास पर पहला पहला शोध प्रबंध लिखा था। डॉ. ब्रजकिशोर मिश्र आलोचना सम्राट पं0 कृष्ण बिहारी मिश्र जी के सुपुत्र थे। अवध के कवियों पर लिखा गया उनका शोध प्रबंध महत्वपूर्ण है। अध्यापक रूप में वे बहुत लोकप्रिय थे। उनकी स्मृति में यहाँ शनिवारीय व्याख्यान माला शुरू की गयी। डॉ. सरला शुक्ल ने जायसी के परवर्ती सूफी कवियों पर अच्छा शोध कार्य किया था। डॉ. देवकीनन्दन श्रीवास्तव द्वारा ‘तुलसी की भाषा‘ पर लिखा गया शोध प्रबंध बहुप्रशंसित रहा है। इन सबकी अपेक्षा विभाग को बेहतर ख्याति प्रदान की थी डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने जो प्रथम डी. लिट उपाधि प्राप्त विद्वान थे और आदिकालीन साहित्य के विशेषज्ञ थे। गुप्त जी ने डॉ. प्रेमनारायण टंडन के सहयोग से इसे ब्रजभाषा अध्ययन का केन्द्र बना दिया था। उनके द्वारा दस खण्डों में प्रकाशित ‘सूर ब्रजभाषा कोश‘ एक विशिष्ट देन है। डॉ. गुप्त की स्मृति में विभागीय पुस्तकालय का नामकरण किया गया। गुप्त जी ने डॉ. शंकरलाल यादव की नियुक्ति करके यहाँ लोक साहित्य की शुरुआत करायी थी। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए विभाग में अवधी परिषद् की स्थापना की गयी और अवधी त्रै. पत्रिका निकाली गयी।
कुलपति आचार्य नरेन्द्रदेव श्रेष्ठ प्रशासक होने के साथ साथ पालि भाषा, बौद्ध साहित्य और समाजवादी दर्शन के अधिकारी विद्वान थे। वे प्रति सप्ताह एक पीरियड लेने विभाग में आते थे। हिन्दी का स्वतंत्र विभाग बनाने का मुख्य श्रेय उन्हीं को है। उन्हीं के सौजन्य से सुगर फैक्ट्री बिसवाँ, सीतापुर के स्वामी सेक्सरिया से एक ऐसा अनुदान मिला, जिससे विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन के अन्तर्गत लगभग पचहत्तर शोध प्रबंध प्रकाशित किए गए। मैं यह कह सकता हूँ कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी एक विभाग में परिमाण और स्तर की दृष्टि से ऐसा प्रकाशन नहीं हुआ है। आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में यहां राजभाषा कक्ष की स्थापना की गयी।
इस विभाग में पूरे विश्वविद्यालय की ओर से ‘ज्ञानशिखा‘ नामक शोध त्रैमासिकी का प्रकाशन किया गया था। बीच में कुछ अवरोध आ गया। आचार्य जी की जन्मशताब्दी के अवसर पर मैंने उसका पुनरारंभ कराया और बारह वर्षों में उसके कुल उनतीस विशेषांक निकाले। इसी बीच हिन्दी प्रकाशन को सुव्यवस्थित किया गया तथा उसकी स्वर्ण जयंती मनायी गयी और साथ ही ‘फुटकर बिक्री शुरू की गयी। नए शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ नयी आवश्यकता (विशेषज्ञता) के अनुरूप की गयी। इस विभाग में उन दिनों बी.ए. से पीएच.डी. स्तर तक लगभग ढाई हजार विद्यार्थी और चैबीस शिक्षक थे। यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा विभाग था और है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वान पूरे देश में फैले हुए हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा, राव राजा श्यामबिहारी, शुकदेवबिहारी (मिश्र बन्धु), महा कवि अनूप शर्मा, रामविलास शर्मा, कुँवरनारायण, गिरिजाकुमार माथुर, रघुवीर सहाय, चन्द्रप्रकाश सिंह, रामचन्द्र तिवारी आदि यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। विभागीय स्वर्ण जयंती के अवसर पर विभाग के ऐसे भूत पूर्व छात्रों को अभिनन्दित किया गया। लखनवी बोली बानी और लखनवी लहजे को आज मानक माना जाता है। लंदन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. रुपर्ट स्नेल ने इस विश्वविद्यालय के साथ यह समझौता किया कि उनके आठ विद्यार्थी प्रतिवर्ष यहाँ छह-छह महीने रहकर बोलचाल की सही हिन्दी सीखेंगे। एक दिन मैंने उनसे जिज्ञासा की थी. कि आपने दिल्ली, काशी, प्रयाग के बजाय लखनऊ को क्यों वरण किया? उन्होंने कहा ‘दिल्ली की हिन्दी पंजाबी से और काशी, प्रयाग की हिन्दी पण्डों, तीर्थ यात्रियों यानि जनपदीय बोलियों से प्रेरित है। सबसे शुद्ध हिन्दी लखनऊ में बोली जाती है। हमारे विभाग में विदेशियों के लिए ‘सुगम हिन्दी‘ नामक यह डिप्लोमा कई वर्षों तक सफलतापूर्वक चला।
लखनवी जबान ‘उर्दवे मुअल्ला‘ कीन खाफ दुरूस्त मानी जाती है। वस्तुतः लखनऊ उर्दू (हिन्दुस्तानी) का प्रसिद्ध घराना रहा है। हमारे विभाग के एम0ए0 हिन्दी पाठ्यक्रम में उर्दू साहित्य का इतिहास तथा गालिब का दीवान, वर्षों से निर्धारित है। हम आज भी यह मानते हैं कि हिन्दी के प्रथम कहानीकार थे रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्ला खाँ। प्रथम उपन्यासकार थे- उमरावजान अदा के लेखक हादी रुसवा। प्रथम नाटककार थे इन्दरसभा के रचनाकार अमानत।
इस विभाग ने सभी महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। विभाग का पूरा नाम है- “हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग। इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मैंने ‘‘भाषा संगम‘ नाम की एक संस्था खोली। उसमें टैगोर, ज्ञानेश्वर, त्यागराज, सुब्रह्मण्य भारती, शंकरदेव आदि की जयंती-गोष्ठियाँ समय≤ पर आयोजित की गयीं। 14 सितम्बर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ तुलनात्मक भारतीय साहित्य के कई पाठ्यक्रम चलाये गए। बँगला का स्नातक पाठ्यक्रम भी हमारे विभाग का ही अंग है।
आपने सस्ती पाठ्य पुस्तकें सुलभ कराने की एक योजना विभाग में चलाई थी। उसका अनुभव कैसा रहा?
इस विभाग में 1975 में भारत सरकार की बीस सूत्री योजना के अंतर्गत सस्ती पाठ्य पुस्तकें सुलभ कराने का अभियान पं० हरिकृष्ण अवस्थी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। बीच में गतिरोध आ गया। मैंने 1988 में इसका भरसक परिविस्तार किया। बी.ए. में बाहरी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित जो आठ पुस्तकें लगायी जाती थीं, उन्हें बंद करके ‘हिन्दी प्रकाशन‘ की ओर से आठ संपादक मण्डल बनाकर हमने पाठय पुस्तके खुद संपादित, प्रकाशित और वितरित करायीं। प्रति पुस्तक मूल्य दस रूपये मात्र। इससे स्तरीय रचनाओं को स्थान मिला। उससे विभाग को तथा संपादकों को अर्थलाभ भी हुआ। उससे ‘विभागीय विकास निधि‘ की स्थापना की गयी जिससे तीन कमरे बने। बारामदों में ग्रिल लगी। एक प्रयोगशाला और स्मार्ट रूम बना। फर्नीचर, स्टेशनरी, क्राकरी आदि की व्यवस्था हो गयी। इस प्रकार विभाग बहुत कुछ स्वावलम्बी हो गया।
आपने विज्ञापन, अनुवाद और ग्राहक शुल्क के बिना 12 वर्षों तक अपनी शोध पत्रिका के 29 अंक निकाले। इसके
संसाधन क्या थे?
हमने ‘ज्ञानशिखा‘ के जो विशेषांक बनाये, वे अधिकांशतः पाठ्यक्रम से संबंधित थे। ऐसे विषयों से संबंधित थे, जिन पर अच्छी पुस्तकें तब सुलभ नहीं थी। जैसे भाषा प्रौद्योगिकी, अनुवाद कला, साहित्यिक पत्रकारिता, राजभाषा, प्रयोजन मूलक हिन्दी, लोक वार्ता, ब्रजावधी, विश्व हिन्दी, तुलनात्मक साहित्य, इतिहास दर्शन, रंगमंच, सर्जनात्मक प्रशिक्षण, पाठालोचन आदि। हमने पत्रिका के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त प्रतियाँ छपवाकर उन्हें पुस्तकाकार सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करा दिया, जिससे पत्रिका की लागत निकलती रही और हम अनुदान, शुल्क एवं विज्ञापन के बिना इसे बारह वर्षों तक चलाते रहे। इसके हर अंक में हर सहयोगी शिक्षक ने कुछ न कुछ लिखा अवश्य। इससे लिखने पढ़ने की क्षमता का विकास होता रहा।
आपने विभागीय प्रशासन के प्रबंधशास्त्र से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था। वह प्रयोग कैसा रहा?
हमारी विभागीय व्यवस्था कई दृष्टियों से उल्लेखनीय, बल्कि अविस्मरणीय बनी हुई है। हमने विद्यार्थियों की सहभागिता और शिक्षकों की अंतरंगता को बढ़ावा दिया। हर एक के स्वागत एवं विदाई के कार्यक्रम धूम-धाम से हुए। बीच-बीच में कई कई बार सब लोग साहित्यिक पिकनिक पर गए। आपातकाल के बाद अराजकता बहुत बढ़ गयी थी। उस बीच परिसर मंे कई दुर्घटनाएँ हुयीं। ‘इन्ट्रोपार्टी‘ के नाम पर अराजकतत्वों द्वारा वसूली की जाने लगी थी। जब हमारे विभाग में उसकी आवाज पहुँची तो मैंने पिकनिक पर चलने का उनका प्रस्ताव मान लिया। सब खुश थे, यह सोचकर कि वहाँ मनचाही मस्ती करेंगे, पर जब वहाँ जाकर देखा कि बगीचे में दरियाँ बिछी हुयी हैं, सरस्वती जी का एक बड़ा चित्र धूप बत्ती के साथ रखा हुआ है, तो वे शांत होकर मंगलाचरण करने बैठ गए। फिर मैंने विभाग के गौरवपूर्ण इतिहास और वर्तमान युग बोध को लेकर लम्बा तथा अति संवेदनशील वक्तव्य दिया और साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया तो सब भाव विभोर हो गए। चंदा बसूलने के बजाय विद्यार्थी खुद तरह तरह के व्यंजन लेकर आए थे। सबने उस अन्नकूट का आनंद लिया और यह महसूस किया कि यहाँ अराजकता नहीं चलने पाएगी।
मैंने यह अनुभव किया कि यदि शिक्षक चरित्रवान, विद्वान एवं शीलवान है तो आज भी उसका सम्मान है। इधर नव धनाढ्य वर्ग के बच्चों में तेजी से कुलक्षण, भरते जा रहे हैं। उसके लिए ‘साहित्याध्यात्म‘ का सहारा लेना उपयोगी होगा। दूसरे, यदि शिक्षकों-शिक्षार्थियों को बराबर विभागीय आयोजनों में व्यस्त रखा जाये तो न खाली दिमाग होंगे और न शैतानों का निवास। सबका सही उपचार है- शिष्य वत्सलता और विभाग से, विषय से लगाव। छात्र समुदाय को प्रभावित करने के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलानी होंगी। मेरा यह अनुभव रहा है कि यदि सामने पाठ्य पुस्तक नहीं है तो विद्यार्थी का मन कक्षा-केन्द्रित नहीं हो पाता है। लेकिन दूसरी ओर हिन्दी की सब पाठ्य पुस्तकें कुल मिलाकर इतनी महँगी हैं कि निम्न मध्य ग्रामीण वर्ग का विद्यार्थी उन्हें नहीं खरीद सकता। मैंने देखा कि ‘पद्मावत‘ के तीन खण्ड निर्धारित हैं, पर खरीदनी होती है पूरी पुस्तक। मैंने इन सभी पुस्तकों के निर्धारित अंशों की फोटो स्टेट कापियाँ विभाग में तैयार करा ली और केवल कागज की लागत पर छात्रों को उपलब्ध करा दी। इससे पठन-पाठन में गंभीरता आ गयी। मेरा यह अनुभव रहा है कि उत्सवधर्मिता के सहारे विभाग और विषय के प्रति लगाव पैदा किया जा सकता है। दूसरी ओर सहयोगी शिक्षकों के प्रति आत्मीयता निभाते हुए, उनका हित चिंतन करते हुए विभाग में एका बनाया जा सकता है। मैंने पाया कि कई शिक्षकों के पास अपने प्रकाशन नहीं हैं। उनके पीछे पड़ पड़ करके, प्रकाशक की व्यवस्था करके, खुद लंबी भूमिकाएं लिख करके मैंने उनकी थीसिसें छपवायीं। चयन/पदोन्नति को लेकर मैंने स्पष्ट नीति अपनायी कि सब वरिष्ठता क्रम के अनुसार होगा। किसी अज्ञात कुलशील का जोखिम नहीं लिया जाएगा। कोई थीसिस भरसक ‘रिजेक्ट‘ नहीं होगी। विभागीय पुस्तकों की खरीद बुकसेलर्स की उस सूची से होगी, जो संबंधित अध्यापक संस्तुत करेंगे। विभागीय पुस्तकालय-वाचनालय नित्य चार घण्टे खुलेगा। विभाग में आयी पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ विभाग की संपत्ति होंगी।
शोधार्थी निर्देशक के घर न जाकर विभाग में निश्चित समय एवं स्थान पर संपर्क करते रहेंगे। ग्यारह से पाँच बजे तक कोई शिक्षक एवं शिक्षार्थी विभागाध्यक्ष से संपर्क कर सकता है। इस पारदर्शिता का सुपरिणाम हुआ, जैसा कि अखबारों ने लिखा और कुलपति ने स्वीकारा कि ऐसा सौहार्द और किसी विभाग में नहीं दिखता।
शिष्टाचार तथा सौजन्य लखनऊ में अपेक्षाकृत ज्यादा है। यहाँ बातचीत में गाली गलौज, मारपीट, अखबारबाजी, छात्र शक्ति का शोषण, गुण्डागर्दी, कानूनी लिखत-पढ़त यानी खुराफात अपेक्षाकृत बहुत कम है। मैं भारत के कई विश्वविद्यालयों में गया हूँ। मैंने देखा कि एक पाठ्यपुस्तक के बदल देने से भूचाल आ जाया करता है। लखनऊ मंे ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझसे पहले एक दौर आया था जब चयन/पदोन्नति को लेकर हाईकार्ट में कई वाद चले, फिर भी परस्पर सम्बंध नहीं बिगड़े। लोग साथ-साथ चाय पीते और कोर्ट आते जाते रहे। आज मैं कह सकता हूँ कि शिक्षक, शोधक, लेखक होने से कहीं ज़्यादा सफलता मुझे विभागाध्यक्ष रूप में परस्पर सौहार्द स्थापित करने में मिली है।
इस प्रसंग में एक विसंगति की ओर भी ध्यान जाता है। पहले विभाग की अध्यक्षता आँख बंद करके वरिष्ठ व्यक्ति को दे दी जाती थी। डॉ. दीनदयालु गुप्त बीस वर्षों तक विभागाध्यक्ष रहे और मैं साढ़े बारह वर्ष (रिटायरमेंट की तिथि तक)। दोनों का कार्यकाल निरापद रहा। यों, मैंने देखा है कि यदि कोई गलत आदमी रोटेशन में इस आसन पर बैठ जाता है तो वह भार हो जाता है। जब से संतुष्टीकरण की नीति अपनाकर रोटेशन के अनुसार अध्यक्ष नियुक्त होने लगे हैं, कलह तथा असहयोग बढ़ गए हैं। 2 या 3 वर्ष के अल्पकाल में कोई दूरगामी विकास योजना फलीभूत नहीं हो पाती। इस अल्पकालिक अध्यक्ष का कोई प्रभाव, लिहाज या नियंत्रण भी नहीं स्थापित हो पाता। लोग या तो अवमानना करते हैं या उदासीन रहते हैं या बदले की कार्रवाई करने लगते हैं। विभाग में प्रायः छोटे छोटे गुट बन जाते हैं। यह विडंबना की बात है कि विभागीय रणनीति में फँसकर लोग नेताओं और कर्मचारियों की चाटुकारिता तो करते हैं, पर अपने समकक्ष सहयोगी से तालमेल नहीं बिठा पाते। कोई अहं से ग्रस्त, कोई कुण्ठा, आशंका से। मेरा मत है कि वरिष्ठता क्रम के बजाय विभागीय बीस प्रतिशत वरिष्ठ शिक्षकों के बीच से विधिवत गठित चयन समिति द्वारा अध्यक्ष का चयन कराया जाये और कार्यकाल पाँच वर्षों का रखा जाये। चयन करते हुए विद्वता, व्यवहार और प्रशासनिक क्षमता पर ध्यान दिया जाये। उसे कुछ समय का कार्यालयी प्रशिक्षण भी दिया जाये। साथ ही विभागीय समिति को सक्षम बनाया जाये। विश्वविद्यालय की व्यवस्था मूलतः विभाग केन्द्रित होती है। विभागाध्यक्ष उसकी धुरी होता है। प्रयास करना चाहिए कि विभागीय विकास की निरंतरता बनी रहे। मेरे साथ एक दुर्घटना यह हुई कि मेरे बाद दो तीन उत्तराधिकारी ऐसे आए, जिनके पास न विजन था, न नीयत। द्वेष वश किए-कराये गए कार्यों को बंद करा देने से ही उनके अहं की तुष्टि हुई। यह हीनता ग्रंथि और कुंठा की उपज थी। यह दीगर बात है कि लखनऊ में कुछ योजनाओं के बंद हो जाने के बावजूद पूरे देश ने उन्हें अपनाये रखा। यह सुनकर ‘सोचकर दुःख होता है कि लाखों रूपयों की बचत मैंने हिन्दी तथा पत्रकारिता, इन दो विभागों में जमा करायी थी, जिसका सही उपयोग ये उत्तराधिकारी नहीं कर सके। फलतः वह ‘लैप्स‘ हो गयी। सर्व सामान्य शिक्षक इस दिशा में प्रायः उदासीन रहे। सार्वजनिक हित के लिए लोग प्रायः प्रतिवाद नहीं करते। ‘वन मैन शो‘ ही चलता रहता है। सब केवल पीठ पीछे भुनभुनाते हैं।
अधिकतर अध्यक्ष अपने साथियों को अभिभूत नहीं कर पाते। कारण, वे अपने को दूसरे की तुलना में बेहतर विद्वान नहीं सिद्ध कर पाते। वे उदार हृदय अथवा बड़े मन वाले आकाश धर्मा अध्यक्ष सिद्ध नहीं हो पाते। परीक्षा की कूटनीति चयन की रणनीति, टी.ए., डी.ए. की उगाही और अफसरी की लालसा उन्हें जुटकर समर्पित भाव से विभागीय विकास नहीं करने देती। मैंने यह नीति अपनायी कि विभाग के पूर्व शिक्षक ही विशेषज्ञ सदस्य, एवं परीक्षक (प्राथमिकता पूर्वक) रखे जाँयें। मैंने चार पाँच व्याख्यानमालाएं चला रखी थीं, ताकि विद्वानों का आवागमन होता रहे। विभागीय स्वर्ण जयन्ती समारोह इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। उसमें विख्यात विद्वानों का, जो विभागीय पूर्वछात्र थे, एक कुंभ जैसा सम्पन्न हुआ। इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण यह विभाग चर्चा में आया। इसे उत्कृष्टता केन्द्र बनाया गया। आज तक उसका सुफल प्रसाद मिल रहा है। बीच के कुछ वर्षों को छोड़कर मैं निरंतर विभाग से जुड़ा रहा। वहाँ अधिकतर मेरे सुशिष्य है। मुझे स्नेह सम्मान देते हैं। मेरा घर ‘साहित्यिकी‘ एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, हिन्दी शोध केन्द्र है। यहाँ पठन-पाठन, निर्देशन की निःशुल्क व्यवस्था है। कोरोना काल के पूर्व तक शोधार्थियों विद्यार्थियों की यहां भीड़ लगी रहती थी। विभाग से यह नाता जीवन पर्यंत रहेगा। विभाग न होता तो आज जो हूँ, न हो पाता। लगभग 65 वर्षों का नाता है। परिसर में प्रवेश करते ही सहसा साकेत की ये पंक्तियाँ मन में गूंज उठती हैं-
‘जयदेव मंदिर देहली, समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा और एक वराटिका। ‘फूले फले साहित्य की यह वाटिका‘।
आपके समीक्षा-सिद्धांत क्या हैं? वर्तमान समीक्षा तथा हिन्दी के भविष्य पर विचार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइए।
मेरा प्रयास रहा है, शिविरबद्ध समीक्षा को पुनः वस्तुनिष्ठ समीक्षा बनाया जाये। प्रतिबद्धता केवल साहित्य, समाज और जीवन के प्रति हो। सभी मतवादों का स्वागत करें, किन्तु स्वायत्त होकर। दूसरे, समीक्षा को पाठ केन्द्रित किया जाये। केवल पल्लवग्राही टिप्पणियाँ नहीं। मेरा अनुभव है कि यदि किसी अच्छी रचना को कई बार पढ़ा सुना-जाता है तो उसके उत्तमांश और प्रतिपाद्य हमारी स्मृति में पैठ जाते हैं। उनको अंतर्मन में दुहराते हुए नए-नए बिन्दु स्वतः उभरते जाते हैं। उन्हें व्यवस्थित कर लेने से सही समीक्षा स्वयमेव निर्मित हो जाती है। यही व्यावहारिक समीक्षा की भी कसौटी है। मेरी अल्पमति में, किसी बने बनाए काव्यशास्त्र का अंधानुकरण न करके हम कृति की राह से और समग्र व्यक्तित्व (जीवनवृत्त एवं परिवेश) के भीतर से होकर गुजरें। उसके महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समेकित चिन्तन करें। उसका आनुपातिक मूल्यांकन करें। रचनाकारों की रेटिंग‘ करते रहें। राग-द्वेष, लफ्फाजी और रुचि-विपर्यय (सनक) से बचें। समीक्षा को अंतर्विद्यापरक और शोध केन्द्रित बनाएँ। प्राचीन एवं समकालीन समस्त साहित्य को अपना लक्ष्य बनाएँ। सभी प्रवृत्तियों और विधाओं से स्वयं को भरसक जोड़ें। तुलनात्मक भारतीय साहित्य को विशेष प्रश्रय दें। जनपदीय भाषा-साहित्य और लोक वांग्मय का सर्वेक्षण-विश्लेषण करें-करायें। हिन्दी की अपनी अनुप्रयोगात्मक सैद्धांतिकी स्थापित करें। सदैव नए, मौलिक और उपयोगी विषय चुनें। संयत-संतुलित निष्कर्ष निकालें और शोध-समीक्षा को विश्वसनीय बनायें। मेरा यह भी आग्रह है कि प्राचीन अल्प चर्चित श्रेष्ठ रचनाकारों का पुनर्मूल्यांकन करके इतिहास में सम्यक् स्थान देकर उनका साहित्यिक श्राद्ध करें। लुप्तप्राय श्रेष्ठ पाण्डुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और विवेचन करें। भाषा प्रौद्योगिकी को यंत्र के साथ-साथ रचना तंत्र से भी जोड़ें। साहित्येतिहास का पुनर्लेखन करें। हिन्दी को जीविकोपार्जन से जोड़ते हुए राष्ट्रीय एजेण्डा पर अमल करें। उसका प्रबंध विज्ञान बनाएँ। सत् साहित्य का तकनीकी प्रशिक्षण दें। पाठकीयता-पठनीयता को बढ़ावा दें। परंपरा, प्रगति दोनों पर ध्यान दें। शोध का स्तरोन्नयन करें। विश्व हिन्दी को सुप्रतिष्ठित करें। भाषा-साहित्य को जन संचार और शिक्षण-माध्यम के उपयुक्त ढालें और उसको महत्तर मानवीय मूल्यों से सम्बद्ध कर दें।
समीक्षा की शुरुआत आपने कब कैसे की, कुछ प्रकाश डालिए।
शोधकार्य से मुक्त हो जाने के बाद 1964 में मैं समीक्षात्मक लेखन में जुट गया। एम0ए0 में ‘साकेत‘ पढ़ाने वाले मेरे एक गुरुवर, पता नहीं क्यों, ‘साकेत‘ की बड़ी खिल्ली उड़ाते थे, जबकि मैं इस काव्य पर मुग्ध था। डॉ0 नगेन्द्र कृत ‘साकेतः एक अध्ययन‘ मैं पढ़ चुका था, पर उससे संतुष्ट नहीं था, तभी ‘साकेतः कुछ पुनर्विचार‘ पुस्तक लिखी गयी।
इसे लोगों ने बहुत सराहा। अस्तु 1965 में मेरे मन में यह भरोसा जागा कि मैं समीक्षा लिख सकता हूँ। इसी बीच पीएच.डी. शोध प्रबंध को छपवाने का मन हुआ।
राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली के श्री ओमप्रकाश जी से बात हुयी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस शोध प्रबंध को ‘प्रसाद का गद्य‘, ‘निराला का गद्य‘, ‘पंतजी का गद्य‘ और ‘महादेवी का गद्य‘ ‘नामक चार खण्डों में विभाजित कर दिया जाए। तब तक प्रसाद जी की नाट्य कृतियों, कथाकृतियों से, निराला के कुछ उपन्यासों और कहानी संकलनों से, पंत की कुछ भूमिकाओं से और महादेवी के रेखाचित्रों से ही लोग अवगत थे। मैंने पहली बार (1960-63 के बीच) निराला के कई अपूर्ण उपन्यास, कई अप्रकाशित कहानियाँ, बाल साहित्य, अनूदित साहित्य, जीवनियां और सम्पादकीय टिप्पणियाँ खोजीं। मैंने पंत जी के द्वारा लिखित उपन्यास, कहानी संकलन, आत्म संस्मरण, समीक्षा और निबंध लेखन से हिन्दी पाठकों को अवगत कराया। महादेवी जी के कई नए निबंध उस बीच मुझे प्राप्त हुए। इन कवियों के गद्य पर विचार करते हुए मेरी एक नयी स्थापना सामने आयी कि छायावादी गद्य में और उनके काव्य में भाव-भाषागत बड़ा साम्य है, इसलिए इसे ‘छायावादी गद्य‘ भी कहा जा सकता है। जिस तरह प्रगतिवाद का विस्तार कविता के साथ-साथ कथा लेखन, नाट्य लेखन और समीक्षा में हुआ है, उसी तरह से छायावादी गद्य का भी हुआ है। इस ग्रंथमाला का बड़ा स्वागत हुआ।
आपने व्यावहारिक सौन्दर्यशास्त्र का नया नामकरण किया है। उस पर कुछ बताइए।
‘‘छायावादी कवियों के सौन्दर्य विधान‘‘ पर मेरा डी. लिट् शोध प्रबंध 1974 में स्वीकृत हुआ था। उसे मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया ने छापा। जोधपुर विश्वविद्यालय में मैं कई वर्षों से प्रसाद और निराला का काव्य पढ़ा रहा था। ‘कामायनी‘ का अध्यापन करते हुए मुझे जगह-जगह कई नए अर्थ सूझे। वह मेरी परम प्रिय कृति है। उससे
संबंधित समीक्षाओं और टीकाओं से तृप्ति नहीं हुयी थी। जो नयी सूझें उपजी, उनको व्यवस्थित करते हुए मैंने ‘प्रसाद साहित्य की अंतश्चेतना‘ नामक पुस्तक लिखी। यह मेरे एम.ए. के लघुशोध प्रबंध ‘‘प्रसाद का प्रेम दर्शन‘‘ का परिवर्धित परिमार्जित रूप है। इसका प्रथम संस्मरण कलम घर, जोधपुर से छपा था। दूसरा संस्करण नचिकेता प्रकाशन दिल्ली से। बैसवारा अंचल से जुड़े होने के कारण निराला मुझे बहुत प्रिय थे और हैं। मैंने देखा कि निराला ने बैसवारी लहजे के और शब्दों के जो विशिष्ट प्रयोग किये हैं, उन्हें दूरवर्ती लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने उनके आँचलिक प्रयोगों का संग्रह किया और उनके अनदिखे पक्षों को लेकर ‘अलक्षित निराला‘ नाम की समीक्षा कृति लिखी। ‘राम की शक्ति पूजा‘ वर्षों से पढ़ा रहा था। उस पर कई नामी गरामी लोगों ने भी टिप्पणियाँ की हैं पर मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ अनकहा रह गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने ‘राम की शक्ति पूजा‘ पर केन्द्रित व्यावहारिक समीक्षा की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 1992 में आयोजित की। उसमें काव्यशास्त्र, समाजशास्त्र, मिथक, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन, भाषाशास्त्र और शैली विज्ञान से संबंधित वरिष्ठ विद्वानों को इस आशय से आहूत किया था कि अपने शास्त्र को इस कविता पर घटित करके यह सिद्ध करें कि उनकी समीक्षा प्रणाली के सहारे ही इस कविता का सही अर्थ वोधन-अर्थापन संभव हैं? सबने आजमाकर दिखाया किन्तु सबका समाहार यह रहा कि इसके अर्थापन के लिए कोई एक आलोचना प्रणाली पर्याप्त नहीं हैं। वस्तुतः कोई कालजयी कृति . केवल किसी एक प्रणाली यानी हकहरी दृष्टि से पूरी तरह नहीं ‘खुलती। इसका पूरा अर्थबोधन समेकित समीक्षा द्वारा ही संभव है। ‘अभिव्यक्ति प्रकाशन‘ इलाहाबाद की माँग पर मैंने व्यावहारिक समीक्षा पर यह पहली पुस्तक संपादित की। इसी बीच उ.प्र. हिन्दी संस्थान ने मुझसे प्रसाद समग्र, निराला समग्र, पंत समग्र नामक एक ग्रंथमाला लिखवायी, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहतर साबित हुयी। इन कृतियों में प्रसाद की अंतश्चेतना, प्रसाद का गद्य, अलक्षित निराला, निराला का गद्य और पंत का गद्य, का यथोचित सन्निवेश हो गया है। इस बीच महादेवी जी की कुछ नयी गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुयीं थीं, उन्हें समाविष्ट करके ‘महादेवी की गद्य‘ का परिवर्दि्धत संस्करण नेशनल पब्लिसिंश हाउस दिल्ली से प्रकाशित कराया गया। ये पुस्तकें व्यावहारिक समीक्षा से प्रेरित हैं।
आपकी ‘राम की शक्ति पूजा‘ टीका बहुत लोकप्रिय रही हैं उसके लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली?.
लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्षों तक मैं निराला स्पेशल आथर और ‘राम की शक्ति पूजा‘ पढ़ाता रहा। एक दिन मेरे कई सहयोगियों (भूतपूर्व विद्यार्थियों) ने इस माँग के साथ मेरा घेराव किया कि आप जैसे कक्षा में पढ़ाते रहे हैं, वैसे ही बोलते जाँये, हम लोग बारी-बारी से उसे नोट कर लेंगे। मैं मना न कर पाया। नवरात्र के आठ दिनों में मेरे आठ छात्रों ने एक एक करके मेरे व्याख्यानों को लिपिवद्ध करके सचमुच यह कार्य कर डाला। उन्होंने प्रकाशक से उसका अनुबंध करा लिया। यह भाष्य लोगों को बहुत पसंद आया। इसके कई संस्करण निकले। अगले संस्करणों में सरोज स्मृति, और कुकुरमुत्ता की व्याख्या समीक्षा भी जोड़ दी गयी।
निराला की आत्मकथा तैयार करने का विचार मन में कैसे आया?
निराला को पढ़ते-पढ़ाते तथा उन पर शोध करते हुए मैंने यह लक्ष्य किया कि उनके आत्मकथ्य समूचे साहित्य में अंकित है। मैं उन्हें कालक्रमानुसार संयोजित करने में लग गया। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, किन्तु इससे निराला की आत्मकथा तैयार हो गयी। शीर्षक था ‘दुःख ही जीवन की कथा रही।। इस पर दर्जनों समीक्षाएँ लिखी गयी हैं। यह कहा गया कि यह पहली आत्मकथा है, जो स्वयं लेखक (निराला) द्वारा नहीं लिखी गयी है, बल्कि किसी अन्य के द्वारा (मेरे द्वारा) बनायी गयी है, जबकि इसका एक-एक शब्द एवं प्रत्येक कथन निराला के साहित्य से ही ससंदर्भ उद्धृत किया गया है। यह न संस्मरण है, न जीवनी। यह है निराला की अपनी कहानी, निराला की जुबानी। निश्चय ही यह एक विशिष्ट कोटि का प्रयोग है। इसके पहले न ऐसे कोई आत्मकथा बनी थी, न इन पचास वर्षों में अभी दूसरी कोई बन पायी है। इसके चार संस्करण हुए हैं, परिवर्तन परिवर्द्धन सहित।
आपके लेखन का प्रमुख केन्द्र रहा है छायावाद। इधर उसी के सहारे आपने हिन्दी के अपने व्यावहारिक सौन्दर्यशास्त्र की नीव डाली है। क्या इसे दूसरे काव्यान्दोलनों पर भी घटित किया जा सकता है?
समीक्षा की हर कसौटी पर प्रत्येक बोध, विद्या और प्रविधि का लागू किया जा सकता है। छायावाद मेरे अध्ययन का प्रिय विषय रहा है। छायावादी गद्य के बाद ‘छायावाद का व्यावहारिक सौन्दर्यशास्त्र‘ लिखते हुए मैंने कष्ट पूर्वक यह महसूस किया कि हिन्दी का अपना समीक्षाशास्त्र विकसित नहीं हो रहा है। सौन्दर्यशास्त्र नाम की एक नयी समीक्षा प्रणाली उन दिनों आयातित की गयी थी। उसमें बिंब, प्रतीक, कल्पना, अप्रस्तुत विधान यानि पाश्चात्य कसौटी को ही आधार बनाया जा रहा था। मैंने सोचा कि ‘एस्थेटिक्स‘ तो है संवेदना, जिसे भारतीय ज्ञानेन्द्रिय बोध के रूप में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द कहा गया है। रूप से चाक्षुष बिम्ब बनते हैं। यह अग्नि तत्व है। रस षट्रस का विषय है, यह जल तत्व है। स्पर्श से छुअन या स्फुरण का बोध होता है, यह वायु तत्व है, गंध से अनुभूति मिलती है। यह पृथ्वी तत्त्व है और शब्द से ध्वनि-नाद प्रकट होता है, यह आकाश तत्व है। इन पंच तत्वों के सहारे सर्जना-समीक्षा करना व्यावहारिक संवदेना शास्त्र का विषय है। मैंने छायावादी चतुष्टय को केन्द्र में रखकर उनके शब्द-प्रतिशब्द का जो वर्गीकृत-विश्लेषण किया, विद्वानों ने पीठ थपथपाते हुए कहा कि यह छायावादी काव्य कोश है और यह हिन्दी का अपना संवदेनाशास्त्र है।
छायावाद अकेली युग प्रवृत्ति है, जिसका शताब्दी समारोह मनाया गया है, जबकि लोग उसे कालातीत सिद्ध करने पर आमादा थे। आपको अब कैसा लग रहा है?
छायावाद का शताब्दी समारोह मनाते हुए श्री अरुण माहेश्वरी (वाणी प्रकाशन, दिल्ली) ने पन्द्रह-बीस दिनों का समय मुझे दिया, इस आग्रह के साथ कि छायावाद की सौ वर्षों की यात्रा पर एक पुस्तक उन्हें तत्काल चाहिए। यथासमय प्रयागराज में यह लोकार्पित हुयी। लोगों ने उसे मान्यता दी तो श्रम सार्थक हो गया। स्पष्ट है कि मेरा
अधिकाधिक लेखन छायावाद में केन्द्रित रहा है और अभी होता जा रहा है। मुझे काव्योत्कर्ष की दृष्टि से इसके समक्ष दूसरे काव्यांदोलन हलके लगते हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं कामायनी पर वृहद् भाष्य लिखू। मैं यह मानता हूँ कि कला और मनीषा की दृष्टि से ‘मानस‘ के बाद यह हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार छायावाद के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए मैंने ‘छायावाद की सही परख पहचान‘ करने का प्रयास किया और इसी नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की। आज मुझे इस सुख संतोष का अनुभव हो रहा है कि छायावृत्ति के सहारे छायावाद का पुनरवलोकन किया जा रहा है।
प्राचीन काव्य में आपकी रुचि कब कैसे विकसित हुई?
मैं तुलसी साहित्य‘ का अध्येता ही नहीं, आराधक हूँ। ‘रामचरित मानस‘ तो मेरे मन मानस और अंतस में बसा है। उस पर लिखते हुए कभी मौलिकता का दंभ न करके अपनी आस्था का अर्घ्य चढ़ाता रहा हूँ, इसीलिए तुलसी विषयक अपनी पहली कृति का शीर्षक मैंने रखा था-‘तुलसी मानसः आस्था का अर्घ्य ।‘ कालक्रम में मुझे यह सूझा कि नानक पंथं, कबीर पंथ, गांधीवाद, अरविन्द दर्शन की तरह तुलसी का अपना विशिष्ट मतवाद क्यों नहीं चला? शायद उसके निगमागम सम्मत होने या समन्वय सिद्धांत अपनाने के कारण। मुझे लगा कि तुलसी साहित्य में कुछ ‘क्वचिदन्यतोपि‘ भी है। उसे उद्घाटित करना चाहिए। मुझे लगा कि उनका समन्वय समझौता तो नहीं ही है। इस बिन्दु को लेकर मैंने उनके जीवनादर्श, समाजादर्श, लोकादर्श, काव्यादर्श का वर्गीकृत विश्लेषण करते हुए एक समेकित ‘तुलसी मत‘ की स्थापना की जो प्रकाशित होने के बाद लोगों का स्नेह भाजन सिद्ध हुआ।
आपने तुलसी के प्रामाणिक जीवन वृत्त, विशेषतः जन्म भूमि पर बहुत लिखा है। अब आगे क्या योजना है?
तुलसी जन्म भूमि का प्रकरण वर्षों से लंबित था। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक शोध परियोजना के अंतर्गत मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जन्म भूमि के दावेदार तीनों स्थानों राजापुर (बाँदा) सोरों (एटा) सूकरखेत (गोण्डा) की मैंने पहले आडियो वीडियो रिकार्डिंग की।
सम्बंधित दस्तावेज और ग्रंथ एकत्र किए। फिर तीनों स्थानों के दस दस विद्वानों को बुलाकर सैकड़ों प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच तीन न्यायमूर्तियों की उपस्थिति में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया, जिसका अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि जनश्रुतियों, भाषिक, सांस्कृतिक प्रयोगों, पांडुलिपियों और अवांतर कथनों के अतिरिक्त किसी पक्ष के पास तुलसी के पूर्वजों की अचल सम्पत्ति (जमीन जायदाद) का कोई ‘डाक्यूमेंटेड रिकार्ड‘ नहीं है, इसलिए तुलसी का अंतस्साक्ष्य या आत्मकथ्य ‘तुलसी तिहारो घर जायो है‘ को ही एकमात्र आधार माना जाएगा। इस आत्मकथा के अनुसार 500 वर्ष पूर्व तुलसी का जन्म ‘औध राज्य‘ में हुआ था। तात्पर्य यह कि तुलसी जन्मस्थली है सूकरखेत, जो उन दिनों सूबाये औध में आता था। सम्प्रति वह गोण्डा जिले में है। इस प्रकरण को लेकर तुलसी जन्म भूमि नाम से मेरी एक पुस्तक अयोध्या शोध संस्थान से प्रकाशित हुयी। मेरा आग्रह है कि अयोध्या में तुलसी स्मारक ‘परिसर में स्थित ‘तुलसी चैरा‘ गोस्वामी जी को प्रिय था। वहीं उन्होंने
अधिकांश मानस की रचना की थी। ऐसी संभावना है कि वह उनकी कर्म स्थली रही हो। इसके प्रामाणिक अन्वेषण की आवश्यकता है।
लोग तुलसी कबीर को बाँटने पर आमादा हैं, जबकि आप दोनों के भक्त हैं। यह कैसे संभव है?
मध्ययुगीन कवियों में कबीरदास भी मुझे प्रिय हैं। मैंने ‘संत कबीर और महात्मा गाँधी‘ नाम की पुस्तक इन दोनों से प्रभावित होने के कारण ही लिखी थी। नेशनल पी.जी. कालेज लखनऊ के गाँधी अध्ययन केन्द्र में मैंने कबीर एवं गांधी जी पर कई भाषण दिए थे। उन्हीं की परिणति है यह पुस्तक। मेरी दृष्टि में तुलसी कबीर परस्पर पूरक हैं। दोनों भक्त हैं, दार्शनिक हैं, समाज सुधारक हैं। इनमें किसी को छोड़ना घातक होगा। मेरे प्रिय कवि हैं जायसी। वे मेरे पूर्व जनपद से जुड़े हुए कवि हैं। पद्मावत की टीकाओं में मुझे कई जगह अन्यथा अर्थ या अनर्थ मिले। कारण, इनमें कोई भी टीकाकार बैसवारी अवधी से जुड़ा हुआ नहीं था। फारसी लिपि में लिखी हुयी अवधी भाषा सहजतः पकड़ में नहीं आती। देशज अवधी शब्दों के फारसी में लिखे कई वैकल्पिक पाठों के सहारे कई अर्थ भेद प्राप्त होते है। उनसे प्रेरित होकर मैंने ‘पद्मावत प्रभा‘ नामक एक टीका लिखी। मेरा मत है कि पाठालोचन को पुनः समीक्षा से जोड़ा जाये। यह कार्य केवल आचार्य श्रेणी के वरिष्ठ शिक्षकों के ही वश का है।
आपने रीतिकाव्य के पुनर्मूल्यांकन का भी बीड़ा उठाया है। उस दिशा में क्या प्रगति है?
मध्यकाल के उन कवियों को मैंने अपने अध्ययन का विषय बनाया, जिनके न सब मूल ग्रंथ प्राप्य हैं और न उन पर पर्याप्त शोध समीक्षाएं लिखी गयी हैं, जैसे चिंतामणि, बेनीभट्ट, बेनीप्रवीन, चंदन, सेनापति आदि। गौण कवियों में देवकीनन्दन, भावन, भौन, गोकुल, गिरिधारी आदि। इनकी कई ग्रंथावलियां मैंने संपादित प्रकाशित की हैं। सेनापति इतने बड़े आचार्य कवि है पर तब तक उन पर कोई किताब प्राप्य नहीं थी। साहित्य अकादमी ने मुझसे यह पुस्तक लिखवायी और छापी। मैंने तोषनिधि, सरदार कवि, कविन्द, रघुनाथ, सुंदर, ग्वाल, श्रीपति, बोधा, श्रीधर, ब्रजनिधि, सेंगर आदि लगभग एक दर्जन कवियों की रचनावलियाँ तैयार की हैं, जिनमें कई प्रकाशनाधीन हैं। मैंने प्राचीन परंपराओं को बचाने की कोशिश की है। मैंने गूढ़ काव्य, चित्रकाव्य पर भी दो पुस्तकें लिखी हैं। हिन्दी आशु कविता के स्वरूप और इतिहास विकास को लेकर 1978 में मैंने यह पुस्तक छपवायी थी, ताकि लोग इस लुप्त प्राय कला को पहचानें। इसी ध्येय से मैंने हिन्दी के अपने निजी काव्यशास्त्र की माँग की है। कई गोष्ठियाँ करके मैंने ‘हिन्दी का अपना काव्यशास्त्र‘ नामक एक पुस्तक ‘संपादित-प्रकाशित, की पर अभी तृप्ति नहीं हुई है। इस दिशा मे प्रयास जारी है।
आप इतिहास के पुनर्लेखन की बात जब तब करते हैं। इस दिशा में क्या योजना चल रही है?
हिन्दी साहित्य के प्रचलित इतिहास को लेकर मैं दुःखी हूँ। मेरा निश्चित मत है कि पुरानी हिन्दी 7वीं शती से बोलचाल के साथ साहित्य सृजन में भी चलती रही है। तब गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी (डिंगल) मैथिली, दकनी, अवहट्ट आदि हिन्दी परिवार की विभाषाएँ थीं। इन्हें इतिहास में स्थान देना चाहिए। दूसरे, इतिहास का काल-विभाजन करते हुए केवल आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल नाम ही रखे जा सकते हैं। पूरे युग की कोई एक प्रवृत्ति (कोई एक नाम) न संभव था और न है। इसलिए वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, रासो काल, संधिकाल, देश भाषा, काल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य काल, दूसरी ओर निर्गुण सगुण, रामाश्रयी कृष्णाश्रयी, रीति बद्ध, सिद्ध, मुक्त, आदि उपनाम यानी वर्गीकरण निरर्थक हैं। भारतेन्दु, महावीर प्रसाद द्विवदी जैसे व्यक्तिगत नामों का कोई औचित्य नहीं है। मेरा स्पष्ट मत है कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि समूचे युग यानी कोटि कोटि भारतीयों के जनमानस की प्रवृत्तियाँ न होकर केवल कुछ गिने चुने लोगों द्वारा चलाए गए आंदोलन हैं। आधुनिक काल के इतिहास यानी अठारहवीं ई. से आज तक के विकास को मैंने नवजागरण काल, स्वातंत्र्र्य संघर्ष काल, स्वातंत्र्र्योत्तर तथा समकाल नाम दिए हैं। मेरा मत है कि इतिहास लिखते हुए हमें उर्दू भाषा-साहित्य, जनपदीय भाषा साहित्य, लोकवांग्मय, तुलनात्मक भारतीय साहित्य, विचारधारा के विकास क्रम तथा विदेशियों द्वारा लिखित हिन्दी भाषा साहित्य का भी समावेश अपने इतिहास क्रम में करना होगा। मौखिक इतिहास का भी सहारा लेना होगा और दलीय प्रतिबद्धता से मुक्त होकर एक वस्तुनिष्ठ इतिहास बनाना होगा। नए सिरे से विचार करना होगा कि क्या सचमुच नयी कविता दूसरी समकालीन कविता से, नई कहानी अन्यान्य कहानियों से और नवगीत अन्यान्य गीतों से नितांत पृथक् हैं। यदि यह नयापन एक अनिवार्य युग बोध है तो यह हिन्दी उपन्यासों, नाटकों और शोध-समीक्षा में ‘नव‘ विशेषण एक आंदोलन के रूप में क्यों नहीं उभरा? मेरी यह भी पुरजोर मांग है कि हिन्दी में जो नयी विधायें इधर विकसित हुयीं हैं, जैसे विज्ञान लेखन, कोशकारिता, अनुवाद, मीडिया लेखन, भाषा प्रौद्योगिकी आदि, उन्हें भी साहित्य के इतिहास में समेटना अब जरूरी हो गया है। इसी के साथ हिन्दीतर राज्यों और प्रवासी लेखकों द्वारा रचित हिन्दी साहित्य को भी अपने इतिहास में स्थान देना आवश्यक है। इतिहास लेखन करते हुए हर व्यक्ति और प्रवृत्ति को उसके स्तर के अनुरूप आनुपातिक स्थान देना और तदुपयुक्त विशेषण शब्द देना इतिहास दर्शन की मुख्य शर्त है। इन सूत्रों को लेकर चार खण्डों में मैंने ‘हिन्दी साहित्येतिहास की भूमिका‘ प्रकाशित करायी है, जो इतिहास लेखन की एक प्रविधि बन सकती है। इतिहास दर्शन के इसी क्रम में उल्लेखनीय हैं मेरी ये सात-आठ पुस्तकें- (1) राज्याश्रय और साहित्य, जिसमें सत्ता और साहित्यकार का इतिहास तथा डेढ़ हजार वर्षों के सम-विषम संबंधों का विवरण दर्ज है। (2) स्वातंत्र्र्य समर में साहित्यकारों की सहभागिता-इसमें 1857 से 1947 तक के स्वातंत्र्र्य संग्राम से जुड़े हुए साहित्यकारों का प्रदेय दर्शाया गया है। (3) मिश्रबन्धु (4) लाला भगवानदीन-ये दोनों पुस्तकें साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित की गयी हैं। (5) हिन्दी गौरव (100 प्रतिनिधि हिन्दी सेवी) जो केन्द्रीय हिन्दी संस्थान से प्रकाशित हुई है। भूले बिसरे रचनाकारों के प्रत्यभिज्ञान के रूप में एक कोश निर्माणधीन हैं।
आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास-विकास में केन्द्रित होकर मैंने ‘नया साहित्य नए रूप‘ और ‘हिन्दी का आधुनिक-अत्याधुनिक काव्य‘ नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया। तब तक मैं नयी कविता, अकविता, नई कहानी, अकहानी और नवगीत आदि नारों से सहमत था। उसी तर्ज पर नव नाटक, नव समीक्षा का नारा मैंने भी छेड़ दिया था। कुछ ही वर्षों बाद यह बोध जाग्रत हुआ कि ये सब नकली नारे हैं फलतः इनसे मेरा मोह भंग हो गया। मेरा आग्रह है कि साहित्य के इतिहास दर्शन के आलोक में सामूहिक प्रयास से इतिहास का पुनर्लेखन कराया जाए।
अवधी लोक वार्ता की भी आप प्रायः चर्चा करते रहते हैं? इसके बारे में आपकी क्या योजना है? अवधी के आधुनिक साहित्य की दिशा में क्या योजना है?
लोक साहित्य और अवधी भाषा में मेरी जन्मजात रुचि है। अवधी के इतिहास विकास को लेकर मेरी दो कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं- (1) अवधी भाषा और साहित्य संपदा (2) अवधी (प्रकाशक-साहित्य अकादमी, नई दिल्ली)।
अवधी लोक साहित्य को लेकर मेरी चार पुस्तकंे प्रकाशित हुई हैं- (1) अवधी लोक वांग्मय (2) अवधी श्रमगीत (3) लोकगाथा (4) अवधी लोक कथायें। मैंने ‘आधुनिक अवधी काव्य‘ शीर्षक प्रथम काव्य-संकलन 1977 में प्रकाशित किया था, जिसे कई विश्वविद्यालयों में स्थान मिला। मैंने अवधी परिषद्, अवधी पत्रिका और अवधी शोध की शुरुआत की, फलतः आधुनिक अवधी अनुमन्य हो गयी है। उसका सर्वांगीण विकास आवश्यक है।
आपकी एक विशिष्ट उपलब्धि है पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की स्थापना। इसमें रिसर्च तक की व्यवस्था करने, भव्य भवन बनवाने, स्टूडियो तैयार कराने और सर्वांगीण विकास करने में आपने बड़ा श्रम संघर्ष किया है। आज इस विभाग की स्थिति से आप संतुष्ट है न?
पत्रकारिता विभाग की स्थापना करते हुए वहाँ मैंने आठ दस वर्षों तक अध्यापन किया। पढ़ते पढ़ाते जो सूझा उसे ‘हिन्दी पत्रकारिताः प्रकृति और परंपरा‘ तथा जन पत्रकारिता, जन संचार और जन संपर्क नाम की दो पुस्तकें लिखीं। संचार भाषा हिन्दी, नामक एक पुस्तक मीडिया लेखन कला पर लिखी। पत्रकारिता का कोश तैयार किया। इसी तरह कई छोटी बड़ी पुस्तकें तैयार कीं।
विश्व हिन्दी का पाठ्यक्रम आपका है। क्या प्रवासी लेखन उसी का प्रतिरूप है? जहां तक मेरी जानकारी है, पहली बार है।
विश्व पटल पर हिन्दी ‘नामक एक पुस्तक मैंने पहले पहल तैयार की थी। इस दिशा में और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है?
हिन्दी शोध के विषय में आप की क्या धारणा है?
शोध मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। मैं चाहता हूँ, वह प्रविधि न होकर प्रौद्योगिकी रूप में स्थापित हो। इसी ध्येय से ‘शोध प्रौद्योगिकी‘ नामक पुस्तक मैंने प्रकाशित की। मैंने इसमें लगभग एक हजार शोधोपयुक्त विषय सुझाए हैं तथा शोध के स्तरोन्नयन के उपाय भी। मेरा आग्रह है कि अन्तर्विद्यापरक, पाठालोचन, सर्वेक्षणपरक, तुलनात्मक तथा लुप्तप्राय विषयों पर अधिक शोध हो। प्रायोजित शोध हो सही निर्देशन एवं सही मूल्यांकन हो। शोध ग्रंथों का प्रकाशन हो। शोधकों को सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए शोध की पूर्ण ‘ओवर हालिंग‘ की प्रक्रिया मैंने सुझाई है।
पिछले दो दशकों से मैं देख रहा हूँ कि आप भाषा विषयक विभिन्न समस्याओं को लेकर उद्विग्न हैं। भाषा की प्रौद्योगिकी बने, उसमें तरह तरह के कोश बनें, अधिकाधिक अनुवाद हों, उसका मानकीकरण हो यानी व्याकरण, लिपि, उच्चारण, वर्तनी आदि सही हो जाएं और हिन्दी सर्वांग संपन्न हो जाए। इस संदर्भ में अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
भाषा के नए-नए रूपों को ध्यान में रखकर मैंने दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं -(1) इक्कीसवीं शती की हिन्दी (2) भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा प्रबंधन। अनुवाद समस्या पर मेरी पुस्तक है- ‘अनुवाद प्रविधि। एक पुस्तक राजभाषा पर है। कोशकारिता से तो मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अब तक के प्रकाशित मेरे कोश हैं- (1) वृहद् हिन्दी पत्र पत्रिका कोश (2) राम साहित्य कोश (3) अवधी शब्द कोश (4) अवधी साहित्य कोश (5) अवध संस्कृति विश्व कोश (6) ब्रज संस्कृति विश्वकोश (7) सूक्ति सुधा (8) हिन्दी अनुवाद कोश। मेरी भाषा प्रौद्योगिकी केवल कम्प्यूटर (मशीन) तक सीमित नहीं है। मैंने मनोभाषिकी, मिथक भाषा, प्रतीक भाषा, गूढ़ भाषा (लक्षण व्यंजना) तथा काव्य भाषा की चर्चा भी की है। भाषा प्रबंधन में भाषा की संप्रेषण शक्ति तथा युक्तिबल का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही भाषा, विभाषा, बोली, राजभाषा, कामकाजी भाषा, शिक्षा की माध्यम भाषा, संचारभाषा, विश्व व्याप्त हिन्दी के सात रूपों और रोबोटिक्स (रोबोट भाषा) का प्रश्न भी विचारणीय रहा है। हिन्दी में ज्ञान विज्ञान परक लेखन की बड़ी आवश्यकता है ताकि नयी शिक्षानीति में हिन्दी हर स्तर पर शिक्षण की माध्यम भाषा बन सके।
ये प्रश्न तो आपकी प्रयोजनी हिन्दी के साथ भी जुड़े हुए हैं?
गत चार दशकों से मैं प्रयोजन मूलक हिन्दी अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। इस ध्येय से- मैंने चार पुस्तकें प्रकाशित की हैं- (1) प्रयोजनी हिन्दी (2) राजभाषा के पचास वर्ष (3) प्रयोजनपरक हिन्दी (प्रयोजनमूलक हिन्दी)।
इनके अतिरिक्त स्फुट निबंधों के मेरे कई संकलन प्रकाशित हुए हैं- (1) चिंतन पर्व (2) मंथन पर्व (3) मनन पर्व (4) शोध और समीक्षाः नए उपक्रम (5) शोध समीक्षाः नए संदर्भ आदि। मेरा आग्रह है कि ऐसे विषयों पर ध्यान दिया जाए जिनसे रोजगार मिले और ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई हो सके, साथ ही जनसंवाद स्थापित हो जाए।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है जिस क्षेत्र में पाठकीय सामग्री का अभाव दिखा और जहाँ पुनर्विचार करने की विवशता महसूस हुई, वहाँ मुझे कलम रगड़नी पड़ी है।
आपकी अपनी दृष्टि में, बिना असंयत दर्पोक्ति और बिना लोकशील वाले आत्म गोपन के, आत्मविश्वास के सहारे आपकी विशिष्ट उपलब्धियाँ क्या हैं?
अपनी पुस्तकों के संबंध में मौलिकता का दंभ प्रकट करना लोकशील के विरुद्ध होगा। मैं मात्र इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि मेरे लेखन के पीछे न तो कोई संकीर्ण वैचारिक शिविर बद्धता रही है और न बाजारू वृत्ति। अपनी अधिकतम सूझ बूझ के सहारे गत 50 वर्षों में औसत 8 घण्टे नित्य श्रम करके मैंने इन्हें लिखा है। एक-एक शब्द से जूझते हुए और - छाया शब्द के फलितार्थ की खोज करते हुए ‘छायावृत्ति‘ के आलोक में मैंने पहली बार छायावाद की मूल भूत प्रवृत्तियों की भरसक सही पहचान करायी है। इसके काव्योत्कर्ष का आकलन करते हुए इसे शाश्वत वैश्विक मानवीय राग चेतना का सर्वोत्कृष्ट काव्य आंदोलन सिद्ध किया है। समीक्षा क्षेत्र में मैंने पाठ केन्द्रित व्यावहारिक समीक्षा, भाषा टीका और पाठालोचन को भी महत्व दिया है। उच्चतर पाठ्यक्रमों से संबंधित विषयों पर मैंने स्तरीय लेखन की कोशिश की है, ताकि विद्यार्थियों को चालू कुंजियों का सहारा लेने की नौबत न आए। हिन्दी को प्रयोजन मूलक (रोजगारोमुख) रूप देने की और श्री सत्यनारायण मोटूरि जी के दो विषयों को बीस विषयों तक विस्तारित करने का प्रयास मैंने किया है। भाषा प्रौद्योगिकी को कम्प्यूटर के साथ-साथ रचना तंत्र, या शिल्प विधि से भी जोड़ा है, साथ ही भाषा प्रबंधन का एक नया अनुशासन प्रस्तावित किया है, ताकि राजभाषा का कार्यान्यवन सत्य निष्ठा के साथ हो। इसके कुछ व्यावहारिक सुझाव मैंने दिए हैं। मेरे विचार से हिन्दी तब पूर्ण समृद्ध होगी, जब उसमें ज्ञान विज्ञान की अधिकाधिक पाठ्य सामग्री भर जाएगी। इस ध्येय से मैंने आसाधारण श्रम करते हुए लगभग आध दर्जन इन्साइक्लोपीडिया और आध दर्जन शब्द कोश निर्मित किए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने जन पत्रकारिता एवं जनसंचार भाषा की पहली-पहली बार रूप-रचना की है। मेरी कोशिश रही है, हिन्दी भाषा और साहित्य के भविष्य का पूर्वाभास करनेध्कराने की। जनपदीय भाषाओं, विशेषतः अवधी भाषा-साहित्य और उसके लोक साहित्य को बचाने-बढ़ाने की दिशा में वर्षों से मैं प्रयत्नशील हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रही है- इतिहास दर्शन के आलोक में हिन्दी भाषा साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की। मैंने एक सर्व समावेशी ढाँचा तैयार किया है। मेरी बहुत बड़ी चिंता यह है कि हिन्दी की पुरानी श्रेष्ठ पाण्डुलिपियाँ और उसका बहुत सारा अप्रकाशित साहित्य नष्ट प्राय है। मैंने अपने सीमित साधनों से आचार्य चिंतामणि, कवि चंदन, बेनी भट्ट, शिव सिंह सेंगर, हफीजुल्ला खां, बेनी प्रवीन, कवि गिरिधारी, देवकीनन्दन जैसे कई आचार्य कवियों की ग्रंथावलियाँ प्रकाशित की हैं। सत्ता और साहित्यकार के बनते बिगड़ते सम्बंधों के इतिहास को लेकर तथा
स्वाधीनता आंदोलन में हिन्दी साहित्यकारों की भूमिका को लेकर बैसवारा से लेकर काकोरी तक मैं वर्षों भटकता रहा हूँ। यह लेखन उसी का कृपा प्रसाद है।
मैंने कई प्राचीन कवियों के हस्तलेखों का प्रकाशन तथा पुनर्मूल्यांकन किया है। मेरा मत है कि कबीर विद्रोही से कहीं ज्यादा भक्त थे तथा रहस्य-दर्शन से जुड़े साधक थे। मेरा आग्रह है कि कबीरपंथ, अरविंद दर्शन आदि की तरह ‘तुलसी मत‘ की स्थापना की जाये। उसके प्रचार प्रसार से आज की अनेक विकृतियों का उन्मूलन होगा। मैंने यह कोशिश की है कि जिन रचनाकारों ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर उसके बावजूद वे उपेक्षित रह गए हैं, उन पर जरूर लिखा जाये। इसी निश्चय के अनुसार मैंने सेनापति, मिश्रबंधु, लाला भगवानदीन, शिवसिंह सेंगर आदि पर ये पुस्तकें लिखी हैं। इधर मैं भूले बिसरे रचनाकारों के परिचय कोश के निर्माण में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ, हिन्दी का अपना व्यावहारिक काव्यशास्त्र अर्थात् घोषित अघोषित काव्य सिद्धांतों के साथ अनुप्रयोगात्मक पद्धति के सहारे एक नितांत निजी काव्यशास्त्र बने, जो संस्कृत और पाश्चात्य सिद्धांतों की नकल मात्र न हो और जो हिन्दी की भाषिक प्रकृति एवं सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित हो। इस पर कई सेमिनार करवाकर जब मैं निराश हो गया तो स्वयं तिनका तिनका जोड़कर मैंने एक काव्यांग बोध तैयार कर लिया है। इसके अतिरिक्त मैंने साहित्यिक पत्रकारिता, तुलनात्मक भारतीय साहित्य, विश्व हिन्दी, साहित्य का अध्यात्मशास्त्र आदि दिशाओं में पहल की है। साहित्याध्यात्म ग्रन्थ संप्रति यंत्रस्थ है। इसमें साहित्य के सत्य शिव सुन्दर रूप की चर्चा ‘मैटाफिजिक्स‘ के सहारे की गयी है। इधर, साहित्य पार्टीजन के अपप्रचार के कारण प्रदूषित हो गया है।
सत्साहित्य के लिए अपेक्षित है सही सर्जनात्मक प्रशिक्षण से परिपूर्ण यह हिन्दी प्रयोगशाला की। आज जरूरत है वैश्विक चेतना से युक्त हिन्दी की, वाद मुक्त समीक्षा की, नुक्कड़ नाट्य आंदोलन की स्तरीय शोध हेतु व्यावहारिक कार्यशालाओं की, सहकारी प्रकाशन संस्था की, व्यावहारिक पत्रकारिता तथा संचार संप्रेषण प्रविधि के संज्ञान की। मैंने कैरियर या रोजगार हेतु उपयोगी हिन्दी ज्ञान विज्ञान परक लेखन की दिशा में भरसक न्यूनाधिक प्रयास किए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 4 दशक पूर्व हिन्दी प्रयोगशाला बनाकर मैंने लगभग दो दर्जन श्रव्य दृश्य वृत्तचित्रों का निर्माण कराया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का सृजन यूजीसी के माध्यम से मैंने किया कराया है। हिन्दी पत्रकारिता, प्रयोजनी हिन्दी तथा शोध का स्तरोन्नय मेरा मिशन रहा है। मैंने न्यूनतम व्यय से राष्ट्रीय गोष्ठियों के आयोजन का एक फार्मूला बनाया है। विभाग के सुसंचालन की दिशा में मेरे कुछ प्रयास अवलोकनीय हैं। मैंने सरकारी अनुदान और विज्ञापन के बिना स्वायत शासी संस्था के सुसंचालन के क्षेत्र में कुछ साहसिक प्रयास किए हैं। इनके अतिरिक्त मुझे यह कहते हुए सुख-संतोष का अनुभव होता है कि देश-विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और प्रकाशकों ने मेरी इन सेवाओं को बढ़ावा दिया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, अयोध्या शोध संस्थान, वृंदावन शोध संस्थान, श्री मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति इन्दौर, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, उ0प्र0 भाषा संस्थान, सूर साहित्य मण्डल आगरा, अवधी परिषद् लखनऊ, अनुवाद परिषद् दिल्ली जैसी छोटी बड़ी अनेक संस्थाओं ने मेरे प्रति आत्मीयता (आस्था) व्यक्त की है। कई संस्थाओं ने अयाचित रूप में पुरस्कार सम्मान भी प्रदान किए हैं। देश विदेश में होने वाली हजारों विचार गोष्ठियों में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला है। लखनऊ, जोधपुर के अलावा चैदह विश्वविद्यालयों ने समय≤ पर अपने यहाँ अतिथि शिक्षक के रूप में मुझे आमंत्रित किया है। इससे मुझे देश के अनेक हिन्दी विभागों को देखने समझने का मौका मिला है। रिटायरमेंट के आठ वर्ष बाद (सतरवर्ष की अवस्था) तक मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा हूँ। कुल लगभग पचास वर्षों तक मैं शिक्षण एवं शोध निर्देशन करता रहा हूँ। शोध निर्देशक तो आज भी हूँ। मैंने दो विषयों (हिन्दी ़पत्रकारिता) और छह विश्वविद्यालयों में कुल 108 डी.लिट् एवं पीएच.डी. शोध प्रबंध अपने निर्देशन में लिखवाये हैं, नए से नए विषयों पर, भरसक उन्हें सर्वथा स्तरीय रूप देकर।
आप सम्प्रति किस कार्य में संलग्न हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं?
मेरी दिनचर्या में प्रमुख कार्य हैं- आधे अधूरे विषयों को पूरा करना। एतदर्थ काफी समय चाहिए। इधर कोरोना काल में यात्रायें बंद रही। घर में पढ़ने लिखने का अवसर तथा परम एकांत सुलभ हो गया। इस बीच मैंने अपने प्रकाशित निबंधों का वर्गीकरण करके ‘‘निबंध हजारा‘ तैयार किया है। इसी अवधि में ‘‘हिन्दी का अपना काव्यशास्त्र‘‘ और ‘‘हिन्दी गौरव‘ (सौ प्रमुख हिन्दी सेवी) ग्रंथ तैयार हुए। कई वर्षों से जिस “खोज‘‘ त्रैमासिक शोध पत्रिका का संपादन कर रहा था, उसमें यथेष्ट पाठक लेखक तथा सहयोगी नहीं मिले, फलतः उसे इस बीच स्थगित करना पड़ा। “स्वाध्याय‘ प्रकाशन‘ नाम से मैंने अच्छी और सस्ती किताबों के प्रकाशन की शुरूआत की थी। इन पुस्तकों का विपणन सुव्यवस्थित हो जाए, तो सबसे सस्ती पुस्तकें छात्रों को सुलभ हो जाएं। विगत 45 वर्षों से ‘साहित्यिकी‘ नाम से मैं एक पुस्तकालय- वाचनालय एवं शोध केन्द्र चला रहा हूँ। उसमें लगभग 250 दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ एवं 25 हजार पुस्तकें पत्र पत्रिकाएँ हैं। यह पब्लिक लाइब्रेरी किसी शुल्क व सिक्योरिटी के बिना हर एक को सुलभ है। निजी संसाधनों से एक भवन, स्टेशनरी, बिजली, पानी तथा जन सुविधाओं के साथ एक पुस्तकालयाध्यक्ष, शोध सहायक कार्यरत है।
कुछ मिलाकर मैं अपनी सेवाओं और उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ। छोटा परिवार है। आवश्यकतानुरूप अल्प आवास, असन, वसन, वाहन तथा आवश्यक देखरेख की सुविधा प्राप्त है। लख चैरासी योनियों की जगह चैरासिवें वर्ष में प्रवेश करते हुए अब तक की यहीं मेरी राम कहानी है।
___________________________________________________________________________________
संस्मरण
आवाज जिनकी है पत्थर में शोला
डॉ. सादिक़
“जब भी पीछे मुड़कर देखता
हूँ..”-सरदार जाफरी कहते हैं- “तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी कामयाब गुज़री लेकिन मैं वह सब कुछ न कर सका जो मैं चाहता था। काश मैंने इससे भी अच्छी शायरी की होती। इससे भी ज़्यादा किताबें लिखीं होतीं। लेकिन कैसे? मेरा तो बेशतर वक़्त फ़िक्रे-मआश (जीविका की चिंता) में ही गुज़र गया। फिर भी मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद आने वाले अदीब और शायर मेरी फ़िक्र (चिंतन) को आगे बढ़ायेंगे और उसे तक़मील (पूर्णता) तक पहुंचायेंगे। जिंदगी के जिन हसीन पहलुओं तक मेरी निगाह न जा सकी, वे उन पहलुओं को ज़रूर देखेंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे और समझायेंगे।”
सरदार जाफरी अपने बाद आने वाली पीढ़ी के साहित्यकारों से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। वे उनके कला और चिंतन में ख़ुद को शामिल महसूस करते हैं। अपनी एक नज़्म ‘नई नस्ल के नाम’ में वे नई पीढ़ी के कलाकारों को आने वाले ज़माने की रौशन किताबें कहकर संबोधित कर करते हुए कहते हैं।
अली सरदार जाफरी का जन्म 29 नवंबर 1913 को हिमालय के दामन में बसे बलरामपुर के एक संपन्न परिवार में हुआ था, जहाँ उनके दादा सैयद मेहदी हसन रियासत के मैनेजर थे। सरदार जाफरी के पिता सैयद जाफर तैयार महाराजा के शस्त्रागार के आला अफसर थे। सरदार कहते हैं कि “मैं जिस घराने में पैदा हुआ वो इंतिहाई मज़हबी मगर साथ ही उदारवादी था। इसलिए हम लोग ईद-मुहर्रम के साथ दशहरा-दिवाली भी मनाते थें।”
सरदार जाफरी की शुरुआती शिक्षा परंपरानुसार घर में ही हुई, फिर छः-सात साल की उम्र में उन्हें लखनऊ के एक धार्मिक मदरसे में दाख़ि़ल करा दिया गया ताकि वे वहाँ अरबी-फारसी पढ़-लिखकर मौलाना बन सकें लेकिन सरदार के मिज़ाज ने उस मदरसे के माहौल, परिवेश और तालीम को क़बूल नहीं किया और वे वहाँ से भागकर वापिस बलरामपुर आ गए। जब दो-तीन बार ऐसा होता रहा तो वालिद ने इसकी वजह पूछी। सरदार ने साफ-साफ कह दिया कि वहाँ मेरा मन नहीं लगता है और मैं अंग्रेज़ी पढ़ना चाहता हूँ। आख़री उनकी बात मान ली गयी।
सरदार जाफरी ने बलरामपुर में ही हाई-स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान वे शायरी करने और कहानियाँ लिखने लगे। 1933 में मैट्रिक पास कर लेने के बाद उन्हें अलीगढ़ भेज दिया गया। पिता की ख़््वाहिश थी कि वे वहाँ पढ़-लिखकर डॉक्टर या बैरिस्टर बने। अलीगढ़ में सरदार का जी ख़ूब लगा। पढ़ाई के साथ-साथ शायरी का सिलसिला भी जारी रहा साथ ही अदबी विषयों पर समीक्षाएं भी लिखने लगे। ‘नौजवानों के अदबी रुझानात’ नाम से चर्चित लेख उसी जमाने की यादगार है।
यह वह जमाना था जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन काफी ज़ोर पकड़ चुका था। प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद पड़ चुकी थी, जिसने साहित्यकारों को बाक़ायदा एक नज़रिए के साथ जोड़ दिया था। सरदार जाफरी अपने युग के तक़ाजों को समझने लगे थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्हें इंक़लाबी ख़्यालात वाले कई शिक्षक और साथी मिल गए, जिनके साथ वे देश की आज़ादी के जेहाद में पूरे जोश-ख़रोश के साथ शामिल हो गए और अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण कॉलेज से निकाल दिए गए।
इसके बाद वे दिल्ली के एंग्लो-अरबिक कॉलेज में दाख़िल करा दिए गए। यहाँ भी उनकी साहित्यिक और राजनैतिक गतिविधियाँ ख़ूब जारी रहीं। बी.ए. के बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अलीगढ़ की तरह यहां भी उन्हें कई इंक़लाबी साथी मिल गए जिनके साथ मिलकर वे जलसों और जुलूसों में नज़्में सुनाने और तक़रीर करने लगे। अंग्रेज़ी लिबास को छोड़कर खादी अपना ली। इस बीच पत्र-पत्रिकाओं में वे ख़ूब छपने लगे थे।
‘आजादी की नज़्में’ नाम से देश भक्ति की जोशीली नज़्मों पर आधारित एक संकलन प्रकाशित किया गया तो उसमें जोश मलीहाबादी की ऐतिहासिक नज़्म ‘ईस्ट इंडिया के फरजंदों के नाम’ के साथ-साथ सरदार जाफरी की एक नज़्म ‘फौजी भर्ती’ भी शामिल थी जिसमें युद्ध का विरोध करते हुए विदेशी सरकार पर तीखा प्रहार किया गया था। इसी साल सरदार जाफरी की कहानियों का एक संकलन ‘मंजिल’ नाम से प्रकाशित हुआ।
पिता की इच्छा थी कि सरदार अब क़ानून पढ़कर प्रैक्टिस शुरु कर दें लेकिन सरदार ने एक साल बाद यह कहकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि क़ानून पढ़ने में उनका दिल नहीं लग रहा है। लिहाज़ा अगले साल उन्हें एम. ए. (अंग्रेजी) में प्रवेश दिलाया गया। आगे की कहानी उनके साथ यह गुज़री कि विदेशी चीफ जस्टिस के सामने विरोध प्रदर्शन करने और विद्यार्थियों को उकसाने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लखनऊ और बनारस की जेलों में रखा गया। साथ ही इम्तहान में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गयी।
आखि़रकार सरदार जाफरी बम्बई आ गए। यहाँ उन्होंने समय≤ पर पत्रकारिता, छद्म लेखन, वृत्त चित्र, धारावाहिक और फिल्म निर्माण जैसे कार्य किए। वे यहां पर कई सियासी आंदोलनों से भी जुड़े रहे। तरक़्क़ी पसंद तहरीक़ का नेतृत्व भी किया और इन सबके साथ-साथ शायरी भी करते रहे। उनकी कई कविताएं हाई-स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के कोर्स में शामिल हो चुकी हैं। कई नज्मों का भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
सरदार जाफरी की शायरी उर्दू साहित्य के इतिहास में एक ख़ास जगह रखती है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बाद उन्हें एक नुमाइंदा शायर की हैसियत हासिल है। उनकी शायरी में मुहब्बत और दर्दमंदी का सशक्त जज़्बा साफ नज़र आता है जो अपने इर्द-गिर्द के ग़रीब और मेहनतकश इंसानों के दर्द को समझने और उसका समाधान तलाश करने में इबारत है।
सरदार जाफरी की शायरी में एक ऐसी नई नज़र मिलती है जो उनसे पहले किसी और शायर में नहीं मिलती। इस सिलसिले में ‘पत्थर की दीवार’ नाम से प्रकाशित उनकी नज़्मों का संकलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
सरदार जाफरी ने आलोचक होने का दावा कभी नहीं किया बल्कि ज़बानी और लिखित तौर पर वे इस बात को नकारते रहे हैं। फिर भी हक़ीक़त यह है कि उर्दू साहित्य में उन्हें रोशन ख़्याल आलोचक के रूप में देखा जाता है। ‘तरक्क़ी पसंद अदब, पैगम्बराने सुखन और इक़बाल शिनासी के अलावा गालिब, मीर, कबीर और मीराबाई की शायरी पर उनकी भूमिकाएं और अनेक आलोचनात्मक लेख उनकी साहित्यिक समझ के आईनादार हैं, जो उन्हें उर्दू के एक प्रतिष्ठित आलोचक की हैसियत देने को काफी है। फिल्मों और धारावाहिकों की बात करें तो अदीबों पर बनाया गया उनका एक धारावाहिक ‘कहकशाँ’ काफी प्रसिद्ध हुआ।
इसमें उन्होंने मजाज़, फिराक़ गोरखपुरी जैसे शायरों और अदीबों की ज़िंदगी और अदब पर अपनी साहित्यिक नज़र का कमाल दिखाया था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा पर जाफरी साहब कहते हैं, “सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे पाने वाला शायर एक ज़बान से निकलकर सारी ज़बानों में पहुंच जाता है। अपने एक ख़ास हल्क़े से निकलकर पूरे मुल्क़ का बन जाता है।” यह अलग बात है कि उनकी शायरी के ज़रिए सारे मुल्क़ ने उन्हें पहले ही अपना रखा है।
साभार: नमस्कार, मई-जून 1998, नई दिल्ली, मो. 8384036071
किसे-किसे, कहाँ-कहाँ, हवा उड़ाके ले गई
यहाँ वहाँ, वहाँ यहाँ, हवा उड़ाके ले गई
बढ़ी थी जो पगार वो नया बजट हड़प गया
न पूछो अब उसे मियाँ, हवा उड़ाके ले गई
वे आस में दहेज की वृद्ध हो गए, उधर
सभी हसीन ‘लड़कियाँ’ हवा उड़ाके ले गई
बढ़ें न दाम, हम यही दुआएँ माँगते रहे
पुरानी मूल्य-सूचियाँ हवा उड़ाके ले गई
वो सीढ़ियाँ जो लेके आए ऊँचा बनने वास्ते,
तो जितनी थीं बुलंदियाँ हवा उड़ाके ले गई
सभी दलों के रहनुमा हैं एक ही हमाम में
सभी की धोती-चड्डियाँ हवा उड़ाके ले गई
वो साम दाम दंड भेद आज़मा के दाँव सब
सदन जो पहुँचे, नेकियाँ हवा उड़ाके ले गई
साभार: ज़िन्दगी का ज़ायक़ा, सादिक़
___________________________________________________________________________________
आलेख, पत्रकारिता स्तंभ
गणतंत्र मीडिया की लक्ष्मण रेखा
डॉ. कुमार कौस्तुभ
भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होनेवाले हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जल्द ही देश 75वां गणतंत्र दिवस भी मनाएगा। हालांकि, यह भी माना जाता है कि विश्व में पहला गणतंत्र भारत के ही वैशाली में कायम किया गया था। इस मायने में भारत विश्व के सभी देशों से आगे है। गणतंत्र के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारत की बात करें तो भारतभूमि पर मीडिया का इतिहास भी काफी पुराना है। भारत में प्रिंट मीडिया की शुरूआत के करीब 250 साल होने जा रहे हैं। हालांकि, देश में समाचारों के प्राइवेट टेलीविजन चैनल महज 26-27 साल से चल रहे हैं और इंटरनेट आधारित वेब मीडिया और समाचारों के बड़े सूत्र के रूप में उभरा सोशल मीडिया भी बहुत पुराना नहीं है। लेकिन, गणतंत्र और मीडिया के अंतर्संबंधों को लेकर हाल के समय में कई अहम सवाल उठे हैं। ये सवाल मूलतः मीडिया की ज़िम्मेदारियों और उसकी भाव-भंगिमा, मंशा और तेवरों से जुड़े हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया को खबरों के प्रकाशन-प्रसारण के लिए पूरी छूट हासिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ने समय≤ पर जन-सरोकारों के प्रति अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभाया है। शायद यही वजह है कि इसे लोकतंत्र का ‘चैथा खंभा‘ भी कहा जाता है। हालांकि मीडिया के लिए इस पद का उपयोग पहल-पहल ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, किंतु भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चैथा खंभा‘ माना गया। वैसे, यह बात सिर्फ आम समझदारी की है और कहीसुनी ही जाती है। लेकिन, मीडिया को लोकतंत्र का चैथा खंबा कहने का अर्थ उसे देश और समाज के प्रति अपने उस उत्तरदायित्व का एहसास कराना भी है जो बिना किसी पूर्व-निर्धारित या विनियमित व्यवस्था के ही उसे सौंप दिया गया। जाहिर है, इससे जन-मानस में मीडिया की विश्वसनीयता और उसकी साख भी जुड़ी हुई है, जिसे बीते दिनों काफी हद तक आघात भी पहुंचा। और चैथे-खंबे के उस तमगे को चोट भी पहुंची जिसका कोई वैधानिक अस्तित्व ही नहीं है। देश के प्रख्यात पत्रकार अखिलेश शर्मा मानते हैं कि “चाहे मीडिया को चैथा खंभा कहा जाता हो, लेकिन संविधान में इसका कोई ज़िक्र नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी जैसे दूसरों को है वैसे ही मीडिया को है। पत्रकार कानून से ऊपर भी नहीं। उसका कोई विशेषाधिकार भी नहीं। मीडिया आत्मनियमन भी नहीं कर सका। अब दो खेमों में बंटा है और उसकी साख रसातल में है ( शर्मा, टविटर, जनवरी 31, 2021)1, कहना न होगा कि अब तक बहुत-से ऐसे सामाजिक-राजनीतिक प्रकरण सामने आ चुके हैं जिनमें मीडिया कवरेज या रिपोर्टिंग पर सवालिया निशान लगे हैं। कभी सरकार, तो कभी आम लोग मीडिया पर पक्षपात या समाचारों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते रहे हैं। इसको लेकर कार्रवाइयां भी होती रही हैं। पत्रकारों पर राजद्रोह या आपराधिक मामले मुकदमे भी हो चुके हैं जिससे व्यवस्था पर भी उंगुली उठी है। सुप्रीम कोर्ट के वक़ील और सायबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता के अनुसार, “संविधान के अनुच्छेद 19 में सीमित प्रतिबंधों के साथ आम जनता और मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा अधिकार दिया गया है। इसीलिए वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में आईटी एक्ट की धारा 66-ए को असंवैधानिक करार दिया था। हाल ही में आई रिसर्च के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के रद्द होने के बावजूद धारा 66-ए के तहत विभिन्न अदालतों में 900 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। कानूनी स्पष्टता नहीं होने से विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा आईपीसी के तहत कठोर धाराओं में मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, जिनमें जल्दी जमानत भी नहीं मिलती। देश के अलग-अलग राज्यों में सोशल मीडिया पोस्ट पर हो रहे बवाल के दौर में शासन और पुलिस की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं होने से संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन हो रहा है। भारतीय गणतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ सुशासन का संतुलन बनना चाहिए। इसके लिए राज्यों में पुलिस और सरकारी अफसरों को संवैधानिक मूल्यों की बेहतर समझ होनी जरूरी है (गुप्ता, जनवरी 26, 2021)।‘‘ दरअसल मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि मीडिया या सोशल मीडिया में किसी तरह की कथित मानहानि से किसी राजनेता या अफसर को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट जाने का अधिकार है, मुद्दा यह है कि क्या हकीकत में मीडिया उस लक्ष्मण-रेखा को लांघ रहा है, जो संविधान के तहत बने कानूनों में समाहित हैं? गहराई से पड़ताल करें तो देखेंगे कि शायद कोई दिन ऐसा नहीं जब मीडिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी की व्यक्तिगत गरिमा पर आक्षेप न होता हो।
प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती है? सरकार और मीडिया के बीच तलवारें क्यों खिंचती हैं? आम लोगों की नजर में मीडिया की विश्वसनीयता क्यों गिर रही है? इसके कई कारण हो सकते हैं। अखिलेश शर्मा कहते हैं कि “मीडिया के बुरे हाल के लिए कुछ पत्रकारों/संपादकों को ही दोष देना ठीक नहीं समस्या राजस्व का ठीक मॉडल न होना है। विज्ञापन पर निर्भरता ने विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है और इसे आम लोगों के हितों से दूर कर दिया। जबकि पत्रकारिता का उद्देश्य आम लोगों की आवाज बनना और सच सामने रखना है‘‘ (शर्मा, ट्विटर, जनवरी 31, 2021)। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि भारत में मीडिया अब मिशन नहीं, कारोबार बन चुका है। बीते बीस-पच्चीस वर्षों में बदले परिदृश्य में मीडिया ने देश की युवा पीढ़ी को रोजगार के शानदार अवसर मुहैया कराये हैं। देश में मीडिया संगठनों (अखबारों, टीवी चैनल, वेब और डिजिटल माध्यम) की तादाद बढ़ी तो कहीं न कहीं प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ी। मर्ज सिर्फ यही नहीं है कि एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कई मीडिया और समाचार संगठनों ने पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता किया, बल्कि यह भी है कि समुचित रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित ऐसे पत्रकारों की भी बड़ी कमी है, जो खबरों और उनसे जुड़े मुद्दों को सही तरीके समझें और फिर उन्हें अपने मंच पर पेश करें। यही वजह है कि आज के दौर में पत्रकारिता कर रहे बहुतेरे पत्रकारों में न तो भाषा के उपयोग की समझदारी है और न ही बर्ताव की शिष्टता। खबरों को पकड़ने और सबसे पहले अपने दर्शकोंपाठकों-श्रोताओं तक पहुंचाने की तेजी में वो ये भूल जाते हैं कि हर खबर से जुड़े कई ऐसे संवेदनशील पहलू होते हैं जिनका ख्याल रखना आवश्यक है। भारतीय गणतंत्र में संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेजा या नासमझी से इस्तेमाल अक्सर पत्रकारों को ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जिससे उनकी अपनी साख तो गिरती ही है, उनके संस्थान का भी नाम खराब होता है और पत्रकारिता की गरिमा तो गिरती ही है।
डिजिटल मीडिया के व्यवहार में आने से खबरों तक लोगों की और लोगों तक खबरों की पहुंच बेहद आसान हो गई है। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन पर इंटरनेट, एप और यूट्यूब जैसे माध्यमों के जरिए अब खबरों का त्वरित प्रकाशन-प्रसारण हो रहा है, आम लोग उन्हें आसानी से हासिल भी कर रहे हैं। इससे सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ खबरों के उत्पादन‘ के प्रति कहीं न कहीं पत्रकारीय गंभीरता भी घटी है। जल्दी से जल्दी खबरों को पब्लिक‘ के लिए पब्लिश करने की कोशिशें कई बार खतरनाक स्थितियां पैदा कर देती हैं। प्रख्यात मीडियाविद प्रो. संजय द्विवेदी कहते हैं, “हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है और यहीं डिजिटल मीडिया करता आ रहा है (द्विवेदी, अक्टूबर 26, 2021)।‘‘ इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य डिजिटल मीडिया का ही है जिसे अब अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपना रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि माध्यम कोई भी हो, पत्रकारीय सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न हो।
सोशल मीडिया के व्यवहार में आने से खबरों को लेकर मीडिया की लक्ष्मण-रेखा अक्सर टूटती दिखाई देती है। सच तो यह है कि सोशल मीडिया पर बहुपक्षीय संवाद के दौरान कोई पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं रह जाता, बल्कि वह आम आदमी की तरह प्रतिक्रिया करता है, जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाते भले ही सही माना जाय, लेकिन पत्रकारिता के लिहाज से कतई उचित नहीं है। वहीं, दूसरा पहलू यह है कि आजकल सोशल मीडिया भी समाचारों का बड़ा स्रोत बन गया है। समस्या यह है कि सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता के माध्यम से कोई जानकारी आती है, तो उसे पुख्ता मानकर खबर चला दी जाती है, जो ठीक नहीं है।
पत्रकारों के लिए आवश्यक है कि खबर किसी भी माध्यम से आये, पहले वे अपनी तरफ से उसकी पूरी पड़ताल करें, तभी आम पाठकों-दर्शकों के लिए पेश करें। किसी के हवाले से आई खबर यदि खबर न हो तो वह पत्रकार की अपनी विश्वसनीयता पर तो आघात करती ही है, उसे संकट में भी डाल सकती है। पत्रकारों के लिए भले ही कोई सरकारी आचार संहिता न हो, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल तो रखना ही चाहिए कि गणतंत्र जिन कानूनों के आधार पर चलता है, उसके दायरे में वे भी आते हैं और यदि किसी भी तरीके से उस कानूनी ‘लक्ष्मणरेखा का उल्लंघन होता है, तो वे कठिनाई में फंस सकते हैं। गणतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी तो देता है, लेकिन पत्रकारों से उच्छंखलता नहीं, गंभीरता की उम्मीद करता है।
संदर्भ:https://twitter.com/akhileshsharma1/status/1355773208952094720?lang=bg
https://hindi.news18.com/blogs/virag-gupta/terrorist-forces-are-active-behind-socialmedia-but-the-law-of-the-country-is-not-clear-3431857.html
https://www.prabhasakshi.com/national/iimc-director-general-sanjay-dwivedi-said-sun-ofdigital-media-can-never-set
संपर्क सूत्र: इंदिरापुरम, गाजियाबाद, मो. 9953630062
ईमेल- kumarkaustubha@gmail.com
___________________________________________________________________________________
यात्रा वृत्तांत
ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क और चिरुकी
श्री राजेन्द्र नागदेव
खूब घना वन... वृक्षों से आच्छादित पहाड़... सामने कुछ नीचे चट्टानों और छोटे पत्थरों के बीच से कल कल कर बहती पहाड़ी नदी...किनारे पर लोहे की चार-पाँच बेन्चें और टेबलें... हर टेबल पर एक छोटी तख्ती जिस पर इस आशय की सूचना कि आप भालुओं के क्षेत्र में हैं। वे यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं। कोई खाद्य पदार्थ टेबल पर या कार में भी न छोड़ें। भालू कार तक भी जा सकते हैं। उन पदार्थों की तालिका भी है जो भालुओं के लिए घातक हैं और उनकी भी जो उन्हें प्रिय हैं... अमेरिका के घने वन में एक टेबल पर मैं, पत्नी, पुत्री, दामाद और छः व तीन वर्षीय नातिनें।
सुबह के दस बज रहे हैं। हम नाश्ते के डिब्बे खोलते हैं। दोनों बच्चियाँ उत्साह से खाद्य पदार्थ निकाल कर टेबल पर बिछाए गए कागजों पर रखती हैं। नजर हर दिशा में जा रही है। भालू नदी की दिशा से आ सकते हैं, विपरीत दिशा से भी अकस्मात आ सकते हैं जिधर पहाड़ और घना जंगल है। सुबह का नाश्ता रोमांचक हो रहा है। सड़क की दूसरी ओर बड़े-बड़े कूड़ेदान रखे हैं। वहाँ भी भालुओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। उन पर लिखा है वे इस तरह बनाए गए हैं कि भालू उन्हें खोल नहीं सकते। पर्यटक इस स्थान पर धीरे-धीरे आने लगे हैं। वाहनों के लिए जहाँ-जहाँ स्थान मिल रहे हैं वहाँ खड़े कर बेन्चों पर बैठ रहे हैं। एक बहुत वृद्ध दम्पती अपने साथ लाई आरामकुर्सियाँ खोल कर बैठते हैं। कुछ पर्यटक नीचे नदी किनारे जा रहे हैं। भालुओं के खतरे के बीच उन्हीं के क्षेत्र में ये सारी गतिविधियाँ चल रहीं हैं। हम आसपास के नैसर्गिक सौन्दर्य का रसपान कर रहे हैं। किंतु, मन में बार-बार यह आशंका उठती है कि यदि भालू आ ही गए तो क्या होगा? हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उन्हें देखने का रोमांच और उत्सुकता भी है तो मन कह रहा है कि वे दूर ही कहीं दिखें पर दिखें जरूर।
खाद्य पदार्थों की गंध हवा में फैलने लगी है साथ ही भालुओं के आ जाने का भय भी। हममे से कोई बता रहा है कि किसी भी वन्य पशु का सामना होने पर दोनों हाथ सीधे ऊपर उठा दो तो पशु को भ्रम हो जाता है कि यह उससे बड़ा कोई प्राणी है और वह डर कर चला जाता है। यहाँ जो तख्ती लगी है उस पर लिखा है कि भालू के आने पर सब लोग एक साथ शोर मचाएँ और उसकी ओर कंकड़-पत्थर फेंकें। पता नहीं वास्तविक स्थिति में किसी को यह सब करने का होश भी रहता होगा या नहीं और उससे भालू भाग जाएगा या और आक्रामक हो जाएगा। किंतु इस समय तो ये ही उपाय सूझ रहे हैं।
हम अमेरिका के ‘ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क’ में हैं। यह पहाड़ों, जंगलों से भरा क्षेत्र दो राज्यों टेनेसी और नार्थ केरोलाइना में फैला हुआ है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ प्रतिवर्ष एक करोड़ पर्यटक आते हैं। यहाँ हर समय धुंध सी छाई रहती है। इसी कारण इसके नाम के साथ ‘स्मोकी’ जुड़ा हुआ है। हम इन्डियाना राज्य से चले थे। केन्टुकी को पार कर टेनेसी राज्य में आए हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में आने का हमारा उद्देश्य नैसर्गिक सौन्दर्य के दर्शन करना है ही, हमारे लिए एक और आकर्षण यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन्स की एक प्रजाति ‘चिरुकी’ की जीवन शैली देखना भी है। इन मूलनिवासियों को यूरोप से आए लोगों द्वारा दास बना कर हर सुविधा से वंचित रखा गया था। आज भी उनकी स्थिति अमेरिका में दोयम दर्जे के नागरिकों सी ही है। उन लोगों की व्यथा से परिचित होना भी हमारा उद्देश्य है।
इस पार्क के पहाड़ों के विहंगम दृष्य का आनंद ‘न्यू फाउंड गेप’ नामक स्थान से पर्यटक लेते हैं । इन पहाड़ों से गुजरते हुए मुझे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ याद आ रहे हैं। विशेष रूप से बोमडिला और तवांग के बीच के। वहाँ के पहाड़ अधिक नैसर्गिक रूप में बहुत गहरी घाटियों और ऊँची चोंटियों के कारण अधिक भयावह लगते हैं। यहाँ पहाड़ों, नदियों, झरनों के अलावा अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और वन्य प्राणी हैं। भालू, सामान्य हिरण, एल्क-एक प्रकार का बहुत बड़े आकार का हिरण, भेड़िये और सर्पों की कई प्रजातियाँ हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए भालू तो नहीं किंतु एल्क, हिरण और भेड़िये दिखाई दिये। एक स्थान पर 3-4 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में बड़ी-बड़ी तितलियाँ दिखीं। लगा जैसे वह उनका ही साम्राज्य हो।
हम ‘न्यू फाउंड लैंड’ में लगभग दो घंटे रुके। सामने खूब विशाल घाटी है और उसके पार पहाड़ दिखाई देते हैं जो नार्थ केरोलाइना के हैं। पूरी दुनिया से आए हुए पर्यटक यहाँ प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहे हैं। नार्थ केरोलाइना के उन पहाड़ों में ही चिरूकी आदिवासियों का वास है। मार्ग में गेट्लिनबर्ग आता है जो पर्यटकों की पसंद के मान से विश्व के बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। जिस होटल में हमने पहले से आरक्षण करवा रखा है वह गेट्लिनबर्ग से लगभग सात मील पहले पिजनफोर्ज नामक स्थान में है। चिरुकी लोगों की बस्ती पिजनफोर्ज से 32 मील दूर राष्ट्रीय उद्यान के दूसरे छोर पर है। रास्ते में गेट्लिनबर्ग की भीड़भाड़ से बचने के लिए हमने बायपास लिया। चिरुकी आदिवासियों के क्षेत्र की ओर जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। न्यूफाउंड लैंड से पहले चिमनीज पिकनिक क्षेत्र है। आरंभ में भालुओं के क्षेत्र में नाश्ते का जो उल्लेख आया है वह यहीं का है।
हम चिरुकियों की बस्ती की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। घना वन समाप्त हो गया है। हम किसी छोटे कस्बे में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते में भालुओं की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं जैसे शहरों में महापुरुषों की लगी होती हैं। इससे यहाँ के आदिवासियों के जीवन में भालुओं के सम्मानपूर्ण स्थान का आभास होता है।
दोपहर हो चुकी है। ढाई बज रहे हैं। भूख लग रही है। एक नदी किनारे विश्राम स्थल है खुला हुआ। घास के बड़े मैदान में टेबल-कुर्सियाँ लगी हैं। नदी के जल में और बाहर घास पर बहुत सारी बत्तखें हैं। लोग उन्हें पास बुला रहे हैं। दाना खिला रहे हैं। हम यहाँ साथ लाया हुआ खाना खाते है। हमने प्रवास के लिए दो दिनों का खाना और पानी रख लिया था पर वह कम पड़ गया। इस क्षेत्र में अमेरिका की चमक दमक वाली छबि से नितांत भिन्न उसका सीधा सादा रूप दिखाई दे रहा है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ सामने ही छोटा-सा हाट लगा है जैसा हमारे यहाँ गाँवों-कस्बों में साप्ताहिक हाट लगता है। 20-25 छोटी-छोटी दुकानें हैं। इन्हें दुकानें भी नहीं कहा जा सकता। कहीं टेबलों पर बेचने के लिए वस्तुएँ रखीं हैं कहीं भूमि पर ही कपड़ा या पोलिथिन बिछा कर वस्तुएँ रखी गईं हैं। वस्तुएँ भी क्या हैं, घरों में दैनिक उपयोग में आने वाली छोटी- मोटी वस्तुएँ। वे भी नई नहीं अनुपयोगी हो चुकीं पुरानी जैसे कप-प्लेटें, मणियों की मालाएँ, कंघियाँ, आइने आदि। यह वास्तव में कबाड़ी बाजार है यहाँ के मूल निवासी चिरुकियों का। चिरुकी संस्कृति का आभास यहाँ मिलना आरंभ हो गया है। कुछ देर विश्राम करके और बत्तखों के साथ कुछ समय बिताने के बाद आगे के लिए निकलते हैं। आगे ओकोनालुफ्ती विजिटर सेन्टर है। यह केन्द्र चिरुकी आदिवासी संस्कृति को बचाने और उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया गया है। यहाँ से पर्यटकों को चिरुकी प्रजाति के रहन सहन और उनसे संबंधित संस्थानों जैसे चिरुकी हेरिटेज सेन्टर आदि की जानकारी मिल जाती है। चिरुकी इंडियन्स के जीवन और उनके संघर्षमय इतिहास को जानने समझने की उत्सुकता के साथ हम सबकुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ गोलाकार बड़ा सा हाल है। अन्दर दीवारों के साथ- साथ लकड़ी की ही गोलाकार बेन्चें बनी हैं किसी स्टेडियम की सीटों की तरह नीचे से ऊपर की ओर। हाल पूरा भरा हुआ है। हाल के मध्य में खड़ी एक चिरूकी महिला चिरुकी लोगों पर यूरोप से आए लोगों द्वारा किये गए अत्याचारों, चिरूकी लोगों की व्यथा और उनके संघर्ष की कहानियाँ सुना रही है। महिला के उच्चारण हम ठीक तरह समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ समय वहाँ बैठ कर बाहर निकल आते हैं।
एक सपाट मैदान के बीच काष्ठ का अनगढ सा स्तंभ है जिसके शीर्ष पर काष्ठ का ही त्रिकोणीय छत्र सा बना है। यह स्तंभ मिट्टी के लगभग एक फुट ऊँचे वर्गाकार चबूतरे पर है। चबूतरे के आसपास नृत्य तथा अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए खाली स्थान है। मैदान के किनारे दर्शकों के लिए लकड़ी की बेन्चें हैं। यह चिरुकी बस्ती का समारोह स्थल है। पर्यटक सीटों पर बैठ रहे हैं। नृत्य की तैयारी हो रही है। यह नृत्य किसी देवता की अर्चना से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान है जैसा सामान्यतः विश्व भर की आदिम जातियों में होता है। चिरुकी स्त्री- पुरुष स्तंभ के आसपास गोल घेरा बना कर खड़े हो जाते हैं। पर्यटकों से भी भाग लेने का अनुरोध करते हैं। वे भी आकर शामिल होने लगते हैं। ऐसे दुर्लभ अवसरों को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। घेरे में एक स्त्री फिर एक पुरुष फिर स्त्री इस तरह सब लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ कर। सभी आदिवासियों के नृत्यों में सामान्यतः इसी तरह का संयोजन देखा जाता है। भारत के कई प्रागैतिहासिक गुहा शैलचित्रों में भी इसी तरह के नृत्य चित्रित पाए गए हैं। हम भी नृत्य में सम्मिलित हो जाते हैं। आयु का कोई बंधन नहीं है। बहुत छोटे बच्चों से लेकर 80-85 वर्ष तक की उम्र के हर आयु वर्ग के लोग हैं। दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों के लोग हैं चिरुकियों के साथ एकाकार होते हुए। वाद्य बजने लगते हैं। उनकी ताल पर लोग थिरकते हुए गोल घेरे में चबूतरे के चारों ओर घूमने लगते हैं। मुझे लग रहा है कि संसार के सभी आदिवासी समूहों के गायन-वादन-नर्तन में लगभग एक ही तरह की लय होती है और वह देर तक चलती रहती है। अमेरिका के मूल निवासियों के साथ उनके नृत्य में भाग लेने का यह अनुभव अविस्मरणीय है। मुझे यहाँ फिर अरुणाचलप्रदेश याद आ रहा है। वहाँ के आदिवासी उत्सव याद आ रहे हैं। मैंने चैथाई सदी पूर्व कुछ अवसरों पर वहाँ आदिवासियों के साथ नृत्य किये थे। कोई भी यात्रा कभी अकेली नहीं होती। हम एक साथ एक ही समय में अनेक समानांतर यात्राएँ करते हैं।
काष्ठ स्तंभ के पास खड़ा एक चिरुकी युवक गा रहा है। सब लोग गोल घेरे में वाद्यों के ताल पर थिरकते हुए घूम रहे हैं। बहुत देर तक एक ही तरह घूमने के बाद लोग एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं और उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाहर घूम कर पुनः अंदर आ जाते हैं और पूर्ववत नृत्य करने लगते हैं। लगातार घूमते रहने और चलने से मैं थक गया हूँ । पाँव जबाब दे रहे हैं। घेरे से बाहर निकल कर बैठ जाता हूँ। नृत्य की समाप्ति पर उस दल के मुखिया के साथ जो अपने पारंपरिक परिधान में है हम कुछ देर बातें करते हैं। मुखिया प्रौढ़ है उसके साथ दो युवक भी हैं। उनके रीति-रिवाजों के संबंध में और अमेरिकी समाज में उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में उनसे बात करते हैं और उनके साथ कुछ फोटो लेकर वहाँ से चल देते हैं।
यह सारा क्षेत्र पहाड़ी है। हम जंगल में हैं। यहाँ निकट ही चिरुकी जीवन को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए एक चिरुकी गाँव की रचना की गई है। लगभग पच्चीस झोपड़ियाँ सी हैं। इनमें कुछ उनके घर हैं जिनसे उनके रहन सहन की झलक मिलती है। कुछ प्रदर्शनी के स्टालों जैसी हैं और उसी उद्देश्य से बनाई भी गई हैं। इन बाँस और लकड़ी से निर्मित स्टालों में हस्तशिल्प की वस्तुएँ रखी गईं हैं। हर स्टाल में वस्तुओं को बनाए जाने की विधियाँ प्रत्यक्ष बताई जा रही हैं। पर्यटकों के समूह में लगभग तीस लोग हैं। हमारे साथ एक चिरूकी युवती गाइड है। वह हर स्टाल पर विस्तार से जानकारी देती जा रही है और कहीं-कहीं स्वयं भी वस्तुओं को निर्मित करने के प्रात्यक्षिक देती है।
चिरूकी अमेरिका के मूलनिवासी हैं। उनकी संख्या अब मात्र एक प्रतिशत रह गई है। अमेरिका की 98 प्रतिशत भूमि पर यूरोप से आए लोगों का आधिपत्य है। हम जिस क्षेत्र में हैं वह चिरुकियों द्वारा विशेष रूप से अपने लिए विकसित किया गया है। विडंबना यह है कि यह भूमि उन्हें अमेरिकी सरकार से खरीदनी पड़ी है। इसका मूल्य उन्होंने किश्तों में चुकाया है। इन मूल निवासियों को यहाँ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह रहना पड़ रहा है। इनकी संस्कृति धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। चिरुकी प्रकृति का सम्मान करने वाली शिकार पर निर्भर प्रजाति है।
इस बस्ती में पूरा चिरुकी जीवन झलकता है। यहाँ एक स्थान पर बोर्ड है -“ओकोनालुफ्ती इंडियन विलेज, चिरुकी इंडियन रिजर्वेशन, चिरुकी, नार्थ केरोलाइना” हम यहाँ लगे हुए स्टालों पर जा रहे हैं। एक स्थान पर आठ फुट लंबे बाँस में से फूँक मार कर लगभग बीस फुट दूरी पर निशाने पर तीर छोड़ा जा रहा है। कुछ पर्यटक यह कोशिश करते हैं पर सफल नहीं हो पाते । चिरुकी गाइड भी यह करती है और वह निशाना सहजता से साध लेती है। हस्तशिल्प की जो वस्तुएँ यहाँ रखी गईं हैं वे कला की दृष्टि से मुझे स्तरीय प्रतीत नहीं हुईं। इनकी तुलना में भारत में आदिवासियों द्वारा निर्मित वस्तुएँ अधिक सुन्दर लगती हैं। शाम घिरने लगी है बरसात भी होने लगी है। हम अत्याधुनिक अमेरिका में उसके नितांत भिन्न मूल स्वरूप को आत्मसात कर वहाँ से प्रस्थान करते हैं।
...सामने जलपोत है बहुत बड़ा। हम उसमे प्रवेश कर रहे हैं। जलपोत का कप्तान सभी आगंतुकों का अभिवादन करता है और सबको अंदर ले जाता है। अंदर जलपोत के अन्य कर्मचारी हैं। वे वहाँ की एक-एक वस्तु के विषय में जानकारी दे रहे हैं। हम धीरे-धीरे इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं। हम 1912 में चले जाते हैं। यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध और सबसे अभागे जलपोत ‘टाइटेनिक’ की विशाल हूबहू प्रतिकृति है। पिजनफोर्ज में स्थित यह इस जलपोत के विषय में जानकारी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसे इस तरह बनाया गया है कि पर्यटक को प्रतीत हो वह स्वयं उसमे यात्रा कर रहा है। म्यूजियम के सभी कर्मचारी पिछली शताब्दी के दूसरे दशक की ही पोशाक में हैं। म्यूज़ियम के परिसर में जलपोत के समुद्र की तलहटी में मिले अवशेषों से निकाला गया लोहे का लंगर रखा है। वर्षों पूर्व देखी गई अंग्रेजी फिल्म ‘टाइटेनिक’ मेरी आँखों के सामने सजीव हो रही है... चीखते-चिल्लाते स्त्री-पुरुष और बच्चे... जलपोत में आ रहा भूकंप... अंधकार... चारों ओर हाहाकार और
असहायता...सबके बीच पनपती और समाप्त होती प्रेम कहानी.... धीरे-धीरे अपने जन्म के साथ ही मृत्यु की तरफ जा रहा एक अभागा जलपोत... म्यूज़ियम में जलपोत में रखे उस समय के वास्तविक सामानों को भी रखा गया है। हमें जो टिकिट दिये गए हैं वे हूबहू वैसे ही हैं जैसे जहाज में यात्रा कर रहे यात्रियों के पास थे। प्रदर्शित वस्तुओं में यात्रियों के फोटो, उनके कोट, हैट, लकड़ी के भारी बक्से जिनमे यात्री अपने सामान रख कर ले जा रहे थे, पीले पड़ चुके दाग-धब्बों वाले लिखे-अधलिखे पोस्ट्कार्ड, डेक पर रखी जाने वाली कुर्सियाँ आदि हैं। लोग उन पत्रों को पढ रहे हैं और दुर्घटना से पूर्व के उस जलपोत के वातावरण में जा रहे हैं। एक लड़की ने लिखा है कि इस यात्रा के बाद वह भारत में समाजसेवा करने के लिए जाना चाहती है। भारत आने की उसकी इच्छा अधूरी रह गई।
जहाज के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर उसके डूबने तक का पूरा इतिहास यहाँ प्रदर्शित है। निर्माण करते समय के छायाचित्र हैं। जहाज के प्रस्थान के समय के तथा उसके संक्षिप्त जीवन काल संबंधी अन्य कई छायाचित्र हैं। जहाज के बाहर समुद्र बनाया गया है। उसका पानी उसी तापक्रम पर एकदम शीतल रखा गया है जैसा उस समय रहा होगा। बर्फ की वह चट्टान भी बनाई गई है जिससे जलपोत टकरा कर ध्वस्त हुआ था। पर्यटक जल को स्पर्श करके देख रहे हैं। ‘टाइटेनिक’ में लगभग सवा दो हजार यात्री और कर्मचारी थे। उनमे से पन्द्रह सौ समुद्र में समा गए। वह इंग्लैंड के साउथएम्प्टन से10 अप्रेल 1912 को निकला था और न्यूयार्क जा रहा था। 14 अप्रेल 1912 की रात 11-40 पर बर्फ की विशाल चट्टान से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट तक धीरे-धीरे पानी में डूबते हुए 15 अप्रेल की सुबह पूरी तरह महासागर की तलहटी में उतर गया। यह उस समय का विश्व का विशालतम जलपोत था और अपनी पहली ही यात्रा पर निकला था। इसका निर्माण ‘हार्ट्लैंड एण्ड वुल्फ’ शिपयार्ड में किया गया था। जलपोत में उस समय के यूरोप के विभिन्न देशों के सबसे रईस लोग यात्रा कर रहे थे। जलपोत में उसका वास्तुकार थामस एन्ड्रूज भी था जो मारा गया। पता नहीं क्यों इतने महत्वपूर्ण जलपोत में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जीवन रक्षक जैकेट मात्र आधे यात्रियों के लिए ही थे। हम उस परिसर से बाहर निकलते हैं। इतिहास से बाहर निकल कर वर्तमान में आते हैं और अपने होटल के लिए प्रस्थान करते हैं।
दानिशकुंज, कोलार रोड, भोपाल, मो. 8989569036
ईमेलः raj&nagdeve@hotmail.com